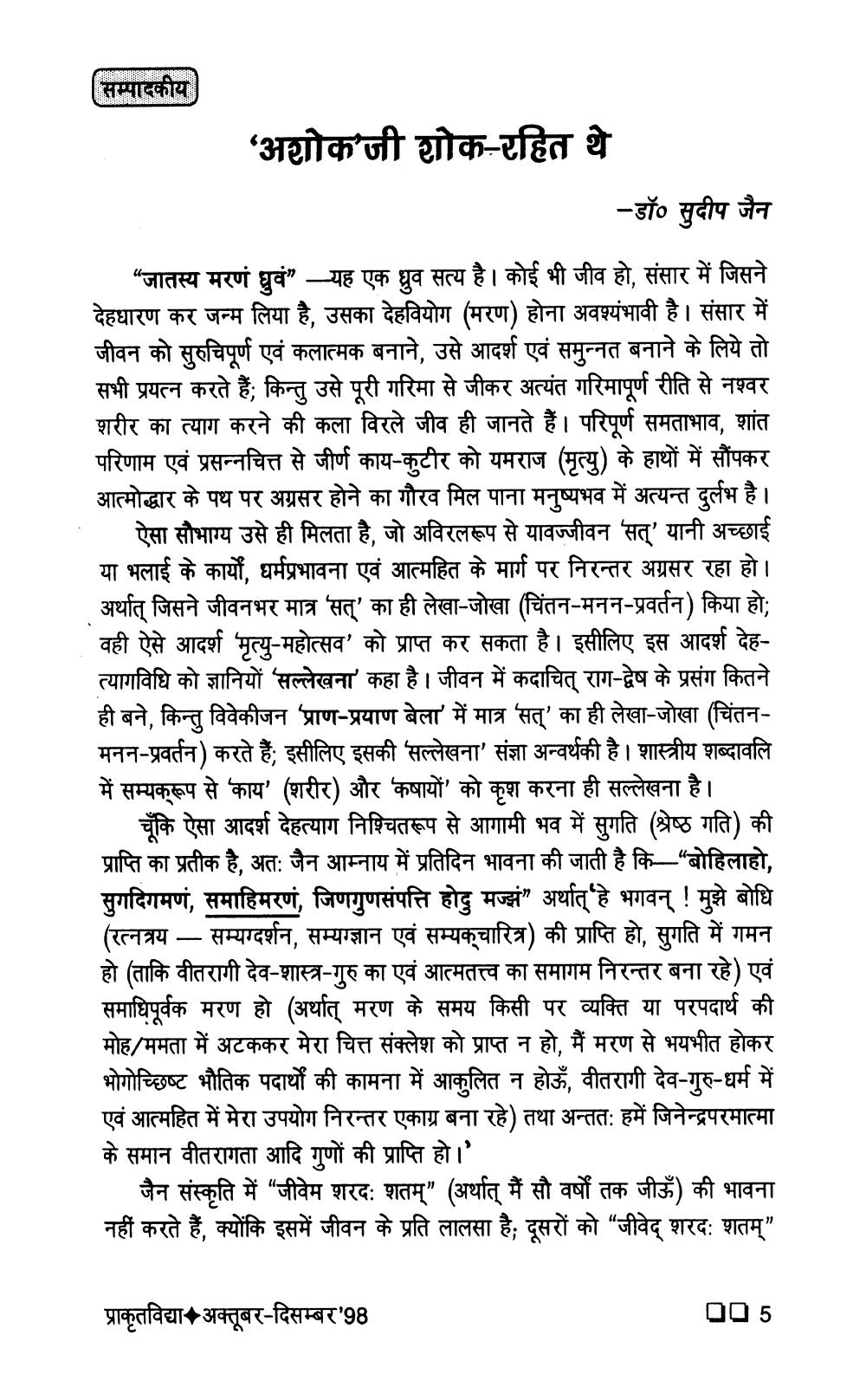________________
(सम्पादकीय
'अशोक जी शोक-रहित थे
-डॉ० सुदीप जैन “जातस्य मरणं धुवं” —यह एक ध्रुव सत्य है। कोई भी जीव हो, संसार में जिसने देहधारण कर जन्म लिया है, उसका देहवियोग (मरण) होना अवश्यंभावी है। संसार में जीवन को सुरुचिपूर्ण एवं कलात्मक बनाने, उसे आदर्श एवं समुन्नत बनाने के लिये तो सभी प्रयत्न करते हैं; किन्तु उसे पूरी गरिमा से जीकर अत्यंत गरिमापूर्ण रीति से नश्वर शरीर का त्याग करने की कला विरले जीव ही जानते हैं। परिपूर्ण समताभाव, शांत परिणाम एवं प्रसन्नचित्त से जीर्ण काय-कुटीर को यमराज (मृत्यु) के हाथों में सौंपकर आत्मोद्धार के पथ पर अग्रसर होने का गौरव मिल पाना मनुष्यभव में अत्यन्त दुर्लभ है।
ऐसा सौभाग्य उसे ही मिलता है, जो अविरलरूप से यावज्जीवन 'सत्' यानी अच्छाई या भलाई के कार्यों, धर्मप्रभावना एवं आत्महित के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर रहा हो। अर्थात् जिसने जीवनभर मात्र 'सत्' का ही लेखा-जोखा (चिंतन-मनन-प्रवर्तन) किया हो; वही ऐसे आदर्श 'मृत्यु-महोत्सव' को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस आदर्श देहत्यागविधि को ज्ञानियों ‘सल्लेखना' कहा है। जीवन में कदाचित् राग-द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किन्तु विवेकीजन 'प्राण-प्रयाण बेला' में मात्र 'सत्' का ही लेखा-जोखा (चिंतनमनन-प्रवर्तन) करते हैं; इसीलिए इसकी 'सल्लेखना' संज्ञा अन्वर्थकी है। शास्त्रीय शब्दावलि में सम्यक्रूप से 'काय' (शरीर) और 'कषायों' को कृश करना ही सल्लेखना है।
चूँकि ऐसा आदर्श देहत्याग निश्चितरूप से आगामी भव में सुगति (श्रेष्ठ गति) की प्राप्ति का प्रतीक है, अत: जैन आम्नाय में प्रतिदिन भावना की जाती है कि-"बोहिलाहो, सुगदिगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होदु मज्झं” अर्थात् 'हे भगवन् ! मुझे बोधि (रत्नत्रय – सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र) की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो (ताकि वीतरागी देव-शास्त्र-गुरु का एवं आत्मतत्त्व का समागम निरन्तर बना रहे) एवं समाधिपूर्वक मरण हो (अर्थात् मरण के समय किसी पर व्यक्ति या परपदार्थ की मोह/ममता में अटककर मेरा चित्त संक्लेश को प्राप्त न हो, मैं मरण से भयभीत होकर भोगोच्छिष्ट भौतिक पदार्थों की कामना में आकुलित न होऊँ, वीतरागी देव-गुरु-धर्म में एवं आत्महित में मेरा उपयोग निरन्तर एकाग्र बना रहे) तथा अन्तत: हमें जिनेन्द्रपरमात्मा के समान वीतरागता आदि गुणों की प्राप्ति हो।' ।
जैन संस्कृति में “जीवेम शरदः शतम्” (अर्थात् मैं सौ वर्षों तक जीऊँ) की भावना नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जीवन के प्रति लालसा है; दूसरों को “जीवेद् शरदः शतम्"
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर'98
005