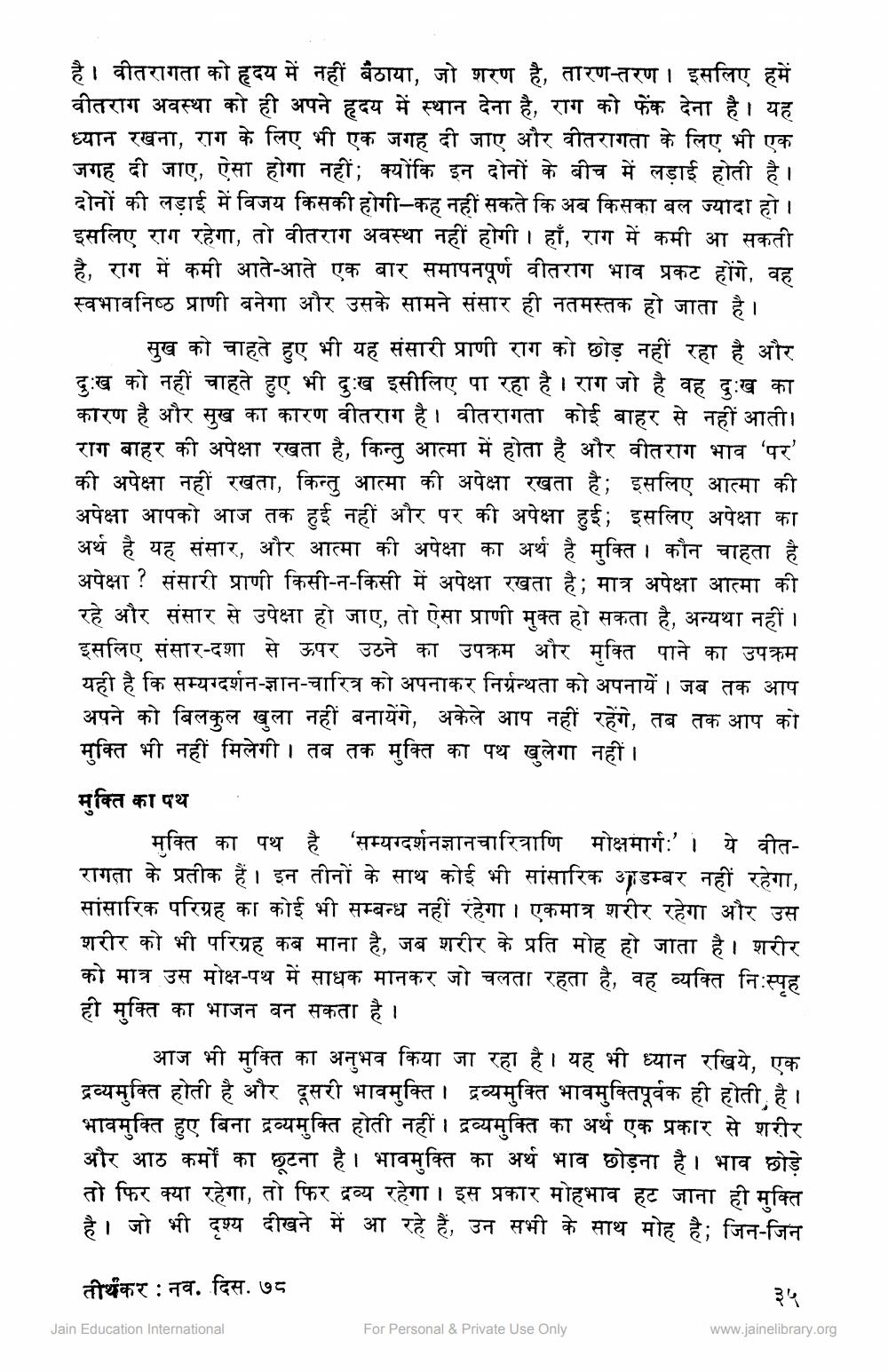________________
है। वीतरागता को हृदय में नहीं बैठाया, जो शरण है, तारण-तरण। इसलिए हमें वीतराग अवस्था को ही अपने हृदय में स्थान देना है, राग को फेंक देना है। यह ध्यान रखना, राग के लिए भी एक जगह दी जाए और वीतरागता के लिए भी एक जगह दी जाए, ऐसा होगा नहीं; क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दोनों की लड़ाई में विजय किसकी होगी-कह नहीं सकते कि अब किसका बल ज्यादा हो। इसलिए राग रहेगा, तो वीतराग अवस्था नहीं होगी। हाँ, राग में कमी आ सकती है, राग में कमी आते-आते एक बार समापनपूर्ण वीतराग भाव प्रकट होंगे, वह स्वभावनिष्ठ प्राणी बनेगा और उसके सामने संसार ही नतमस्तक हो जाता है।
सुख को चाहते हुए भी यह संसारी प्राणी राग को छोड़ नहीं रहा है और दुःख को नहीं चाहते हुए भी दुःख इसीलिए पा रहा है। राग जो है वह दुःख का कारण है और सुख का कारण वीतराग है। वीतरागता कोई बाहर से नहीं आती। राग बाहर की अपेक्षा रखता है, किन्तु आत्मा में होता है और वीतराग भाव 'पर' की अपेक्षा नहीं रखता, किन्तु आत्मा की अपेक्षा रखता है; इसलिए आत्मा की अपेक्षा आपको आज तक हुई नहीं और पर की अपेक्षा हुई; इसलिए अपेक्षा का अर्थ है यह संसार, और आत्मा की अपेक्षा का अर्थ है मुक्ति। कौन चाहता है अपेक्षा ? संसारी प्राणी किसी-न-किसी में अपेक्षा रखता है; मात्र अपेक्षा आत्मा की रहे और संसार से उपेक्षा हो जाए, तो ऐसा प्राणी मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए संसार-दशा से ऊपर उठने का उपक्रम और मुक्ति पाने का उपक्रम यही है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को अपनाकर निर्ग्रन्थता को अपनायें। जब तक आप अपने को बिलकुल खुला नहीं बनायेंगे, अकेले आप नहीं रहेंगे, तब तक आप को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तब तक मुक्ति का पथ खुलेगा नहीं। मुक्ति का पथ
__मक्ति का पथ है 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः'। ये वीतरागता के प्रतीक हैं। इन तीनों के साथ कोई भी सांसारिक आडम्बर नहीं रहेगा, सांसारिक परिग्रह का कोई भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। एकमात्र शरीर रहेगा और उस शरीर को भी परिग्रह कब माना है, जब शरीर के प्रति मोह हो जाता है। शरीर को मात्र उस मोक्ष-पथ में साधक मानकर जो चलता रहता है, वह व्यक्ति निःस्पृह ही मुक्ति का भाजन बन सकता है।
आज भी मुक्ति का अनुभव किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखिये, एक द्रव्यमुक्ति होती है और दूसरी भावमुक्ति। द्रव्यमुक्ति भावमुक्तिपूर्वक ही होती है। भावमुक्ति हुए बिना द्रव्यमुक्ति होती नहीं। द्रव्यमुक्ति का अर्थ एक प्रकार से शरीर और आठ कर्मों का छूटना है। भावमुक्ति का अर्थ भाव छोड़ना है। भाव छोडे तो फिर क्या रहेगा, तो फिर द्रव्य रहेगा। इस प्रकार मोहभाव हट जाना ही मुक्ति है। जो भी दृश्य दीखने में आ रहे हैं, उन सभी के साथ मोह है; जिन-जिन
तीर्थकर : नव. दिस. ७८
३५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org