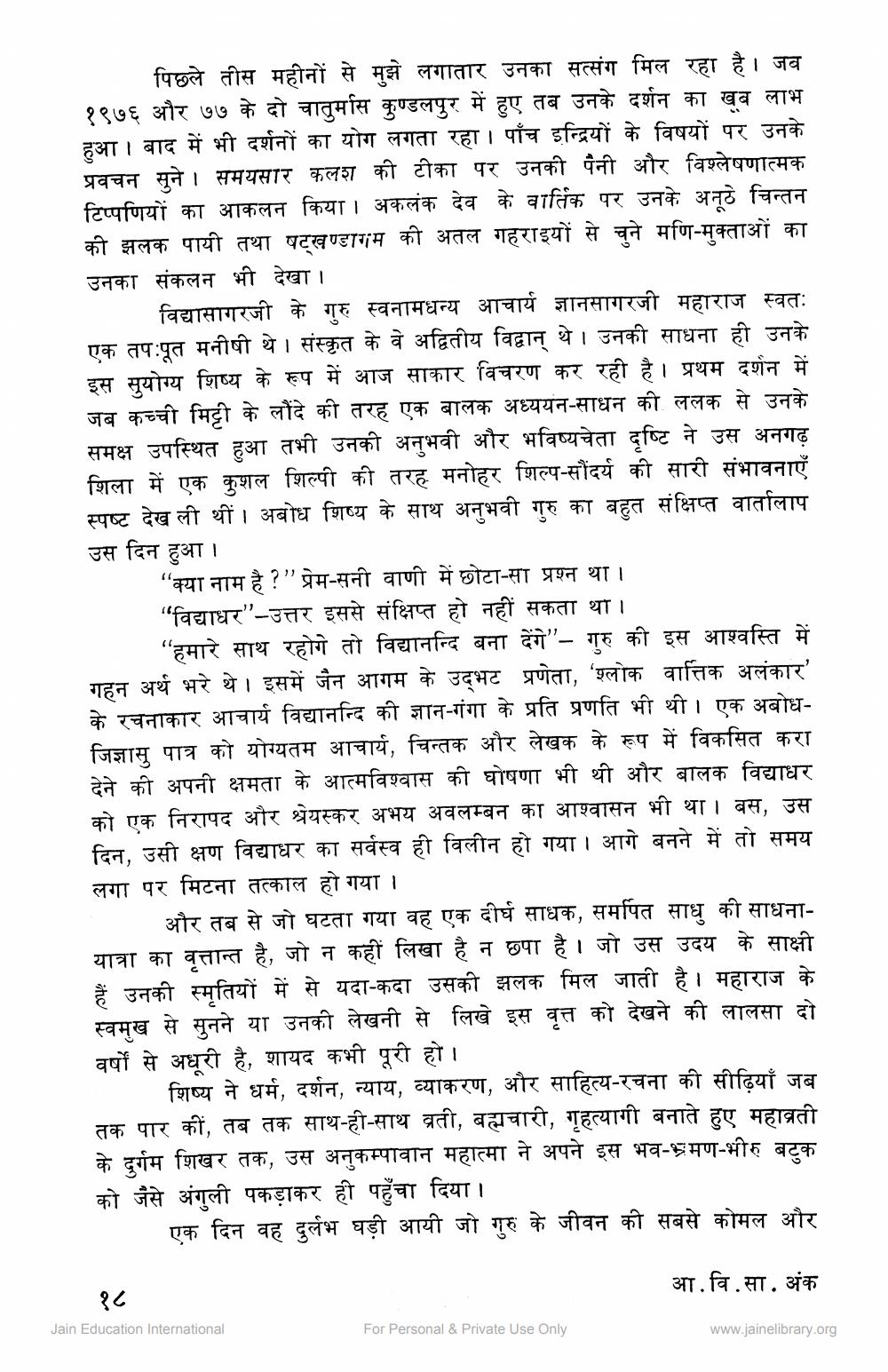________________
पिछले तीस महीनों से मुझे लगातार उनका सत्संग मिल रहा है। जब १९७६ और ७७ के दो चातुर्मास कुण्डलपुर में हुए तब उनके दर्शन का खब लाभ हुआ। बाद में भी दर्शनों का योग लगता रहा। पाँच इन्द्रियों के विषयों पर उनके प्रवचन सुने। समयसार कलश की टीका पर उनकी पैनी और विश्लेषणात्मक टिप्पणियों का आकलन किया। अकलंक देव के वार्तिक पर उनके अनुठे चिन्तन की झलक पायी तथा षट्खण्डागम की अतल गहराइयों से चुने मणि-मुक्ताओं का उनका संकलन भी देखा।
विद्यासागरजी के गुरु स्वनामधन्य आचार्य ज्ञानसागरजी महाराज स्वतः एक तपःपूत मनीषी थे। संस्कृत के वे अद्वितीय विद्वान् थे। उनकी साधना ही उनके इस सुयोग्य शिष्य के रूप में आज साकार विचरण कर रही है। प्रथम दर्शन में जब कच्ची मिट्टी के लौंदे की तरह एक बालक अध्ययन-साधन की ललक से उनके समक्ष उपस्थित हुआ तभी उनकी अनुभवी और भविष्यचेता दृष्टि ने उस अनगढ़ शिला में एक कुशल शिल्पी की तरह मनोहर शिल्प-सौंदर्य की सारी संभावनाएँ स्पष्ट देख ली थीं। अबोध शिष्य के साथ अनुभवी गुरु का बहुत संक्षिप्त वार्तालाप उस दिन हुआ।
"क्या नाम है ?' प्रेम-सनी वाणी में छोटा-सा प्रश्न था। "विद्याधर"-उत्तर इससे संक्षिप्त हो नहीं सकता था।
"हमारे साथ रहोगे तो विद्यानन्दि बना देंगे"- गुरु की इस आश्वस्ति में गहन अर्थ भरे थे। इसमें जैन आगम के उद्भट प्रणेता, ‘श्लोक वात्तिक अलंकार' के रचनाकार आचार्य विद्यानन्दि की ज्ञान-गंगा के प्रति प्रणति भी थी। एक अबोधजिज्ञासु पात्र को योग्यतम आचार्य, चिन्तक और लेखक के रूप में विकसित करा देने की अपनी क्षमता के आत्मविश्वास की घोषणा भी थी और बालक विद्याधर को एक निरापद और श्रेयस्कर अभय अवलम्बन का आश्वासन भी था। बस, उस दिन, उसी क्षण विद्याधर का सर्वस्व ही विलीन हो गया। आगे बनने में तो समय लगा पर मिटना तत्काल हो गया ।
_ और तब से जो घटता गया वह एक दीर्घ साधक, समर्पित साधु की साधनायात्रा का वृत्तान्त है, जो न कहीं लिखा है न छपा है। जो उस उदय के साक्षी हैं उनकी स्मृतियों में से यदा-कदा उसकी झलक मिल जाती है। महाराज के स्वमुख से सुनने या उनकी लेखनी से लिखे इस वृत्त को देखने की लालसा दो वर्षों से अधूरी है, शायद कभी पूरी हो।
शिष्य ने धर्म, दर्शन, न्याय, व्याकरण, और साहित्य-रचना की सीढ़ियाँ जब तक पार की, तब तक साथ-ही-साथ व्रती, बह्मचारी, गृहत्यागी बनाते हुए महाव्रती के दुर्गम शिखर तक, उस अनुकम्पावान महात्मा ने अपने इस भव-भ्रमण-भीरु बटुक को जैसे अंगुली पकड़ाकर ही पहुँचा दिया।
एक दिन वह दुर्लभ घड़ी आयी जो गुरु के जीवन की सबसे कोमल और
१८
आ.वि.सा. अंक
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org