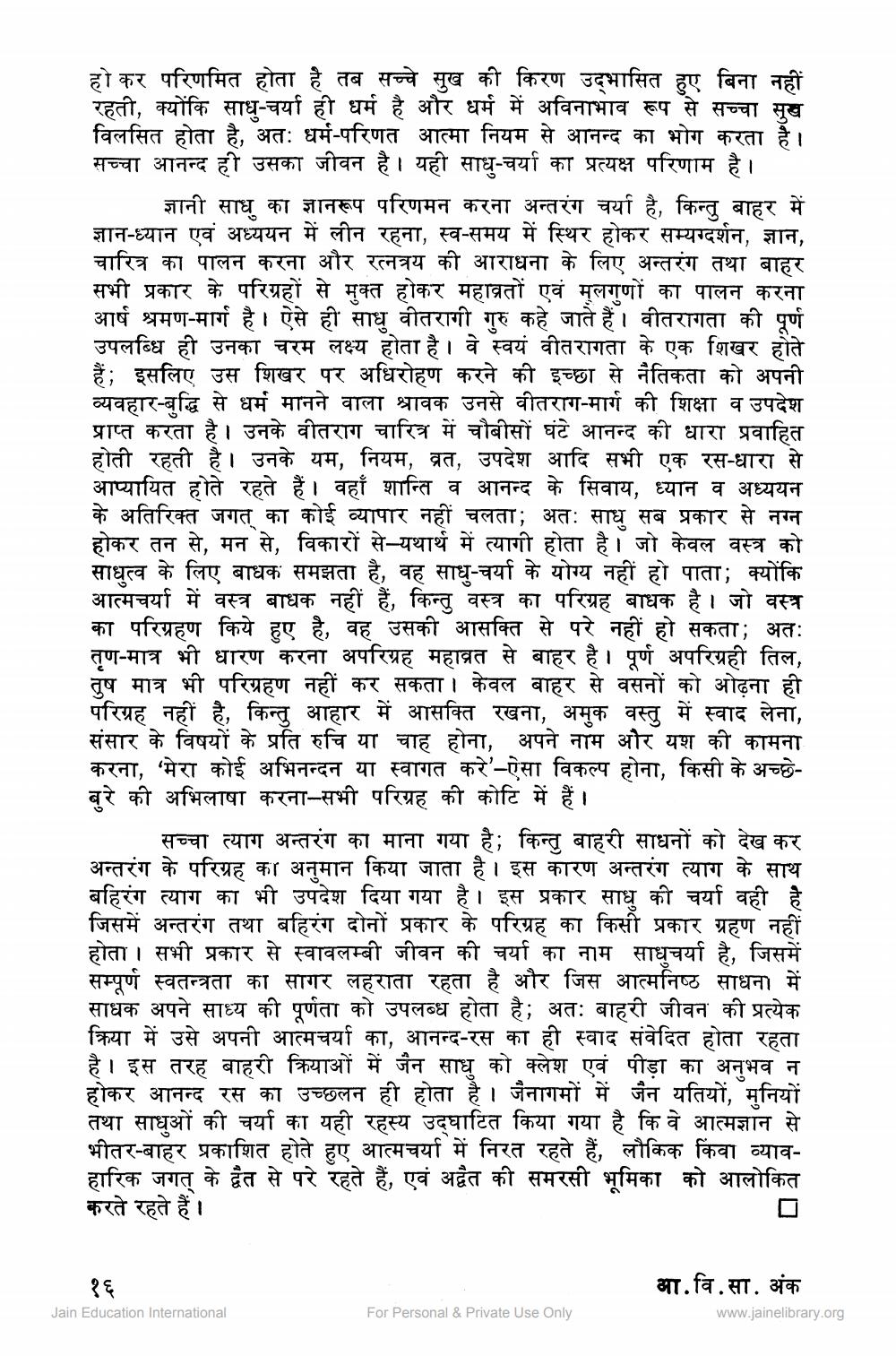________________
हो कर परिणमित होता है तब सच्चे सुख की किरण उद्भासित हए बिना नहीं रहती. क्योंकि साध-चर्या ही धर्म है और धर्म में अविनाभाव रूप से सच्चा सख विलसित होता है, अत: धर्म-परिणत आत्मा नियम से आनन्द का भोग करता है। सच्चा आनन्द ही उसका जीवन है। यही साधु-चर्या का प्रत्यक्ष परिणाम है।
ज्ञानी साधु का ज्ञानरूप परिणमन करना अन्तरंग चर्या है, किन्तु बाहर में ज्ञान-ध्यान एवं अध्ययन में लीन रहना, स्व-समय में स्थिर होकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन करना और रत्नत्रय की आराधना के लिए अन्तरंग तथा बाहर सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होकर महाव्रतों एवं मुलगुणों का पालन करना आर्ष श्रमण-मार्ग है। ऐसे ही साधु वीतरागी गुरु कहे जाते हैं। वीतरागता की पूर्ण उपलब्धि ही उनका चरम लक्ष्य होता है। वे स्वयं वीतरागता के एक शिखर होते हैं; इसलिए उस शिखर पर अधिरोहण करने की इच्छा से नैतिकता को अपनी व्यवहार-बुद्धि से धर्म मानने वाला श्रावक उनसे वीतराग-मार्ग की शिक्षा व उपदेश प्राप्त करता है। उनके वीतराग चारित्र में चौबीसों घंटे आनन्द की धारा प्रवाहित होती रहती है। उनके यम, नियम, व्रत, उपदेश आदि सभी एक रस-धारा से आप्यायित होते रहते हैं। वहाँ शान्ति व आनन्द के सिवाय, ध्यान व अध्ययन के अतिरिक्त जगत् का कोई व्यापार नहीं चलता; अत: साधु सब प्रकार से नग्न होकर तन से, मन से, विकारों से-यथार्थ में त्यागी होता है। जो केवल वस्त्र को साधुत्व के लिए बाधक समझता है, वह साधु-चर्या के योग्य नहीं हो पाता; क्योंकि आत्मचर्या में वस्त्र बाधक नहीं हैं, किन्तु वस्त्र का परिग्रह बाधक है। जो वस्त्र का परिग्रहण किये हुए है, वह उसकी आसक्ति से परे नहीं हो सकता; अतः तृण-मात्र भी धारण करना अपरिग्रह महाव्रत से बाहर है। पूर्ण अपरिग्रही तिल, तुष मात्र भी परिग्रहण नहीं कर सकता। केवल बाहर से वसनों को ओढ़ना ही परिग्रह नहीं है, किन्तु आहार में आसक्ति रखना, अमुक वस्तु में स्वाद लेना, संसार के विषयों के प्रति रुचि या चाह होना, अपने नाम और यश की कामना करना, 'मेरा कोई अभिनन्दन या स्वागत करे'-ऐसा विकल्प होना, किसी के अच्छेबुरे की अभिलाषा करना-सभी परिग्रह की कोटि में हैं।
____ सच्चा त्याग अन्तरंग का माना गया है; किन्तु बाहरी साधनों को देख कर अन्तरंग के परिग्रह का अनुमान किया जाता है। इस कारण अन्तरंग त्याग के साथ बहिरंग त्याग का भी उपदेश दिया गया है। इस प्रकार साध की चर्या वही है जिसमें अन्तरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का किसी प्रकार ग्रहण नहीं होता। सभी प्रकार से स्वावलम्बी जीवन की चर्या का नाम साधुचर्या है, जिसमें सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का सागर लहराता रहता है और जिस आत्मनिष्ठ साधना में साधक अपने साध्य की पूर्णता को उपलब्ध होता है; अत: बाहरी जीवन की प्रत्येक क्रिया में उसे अपनी आत्मचर्या का, आनन्द-रस का ही स्वाद संवेदित होता रहता है। इस तरह बाहरी क्रियाओं में जैन साधु को क्लेश एवं पीड़ा का अनुभव न होकर आनन्द रस का उच्छलन ही होता है। जैनागमों में जैन यतियों, मुनियों तथा साधुओं की चर्या का यही रहस्य उदघाटित किया गया है कि वे आत्मज्ञान से भीतर-बाहर प्रकाशित होते हुए आत्मचर्या में निरत रहते हैं, लौकिक किंवा व्यावहारिक जगत् के द्वैत से परे रहते हैं, एवं अद्वैत की समरसी भूमिका को आलोकित करते रहते हैं।
आ.वि.सा. अंक
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org