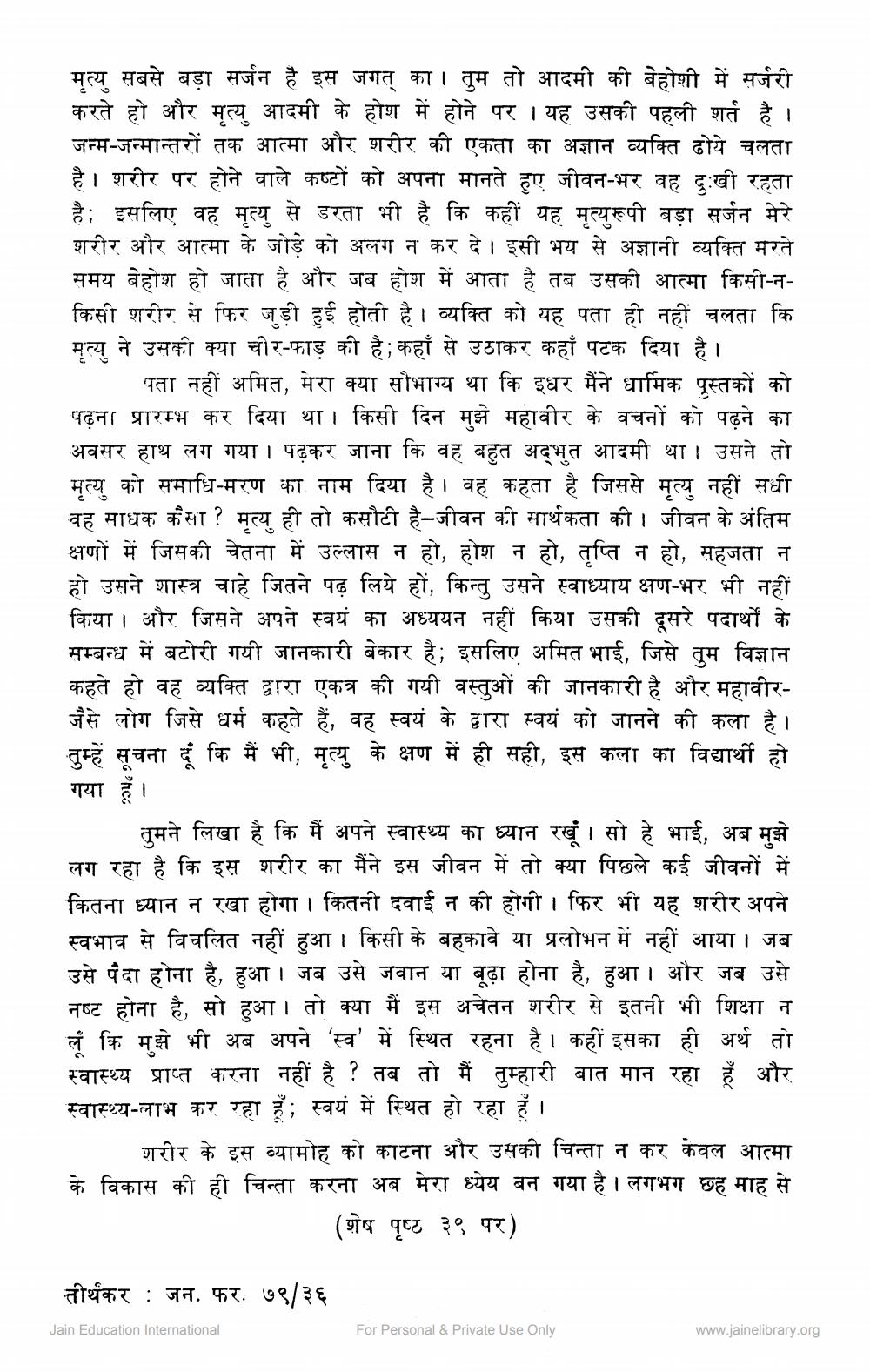________________
मृत्यु सबसे बड़ा सर्जन है इस जगत् का। तुम तो आदमी की बेहोशी में सर्जरी करते हो और मृत्यु आदमी के होश में होने पर । यह उसकी पहली शर्त है । जन्म-जन्मान्तरों तक आत्मा और शरीर की एकता का अज्ञान व्यक्ति ढोये चलता है। शरीर पर होने वाले कष्टों को अपना मानते हुए जीवन-भर वह दुःखी रहता है; इसलिए वह मृत्यु से डरता भी है कि कहीं यह मृत्युरूपी बड़ा सर्जन मेरे शरीर और आत्मा के जोड़े को अलग न कर दे। इसी भय से अज्ञानी व्यक्ति मरते समय बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तब उसकी आत्मा किसी-नकिसी शरीर से फिर जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि मृत्यु ने उसकी क्या चीर-फाड़ की है; कहाँ से उठाकर कहाँ पटक दिया है।
पता नहीं अमित, मेरा क्या सौभाग्य था कि इधर मैंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। किसी दिन मुझे महावीर के वचनों को पढ़ने का अवसर हाथ लग गया। पढ़कर जाना कि वह बहुत अद्भुत आदमी था। उसने तो मृत्यु को समाधि-मरण का नाम दिया है। वह कहता है जिससे मृत्यु नहीं सधी वह साधक कैसा? मृत्यु ही तो कसौटी है-जीवन की सार्थकता की। जीवन के अंतिम क्षणों में जिसकी चेतना में उल्लास न हो, होश न हो, तृप्ति न हो, सहजता न हो उसने शास्त्र चाहे जितने पढ़ लिये हों, किन्तु उसने स्वाध्याय क्षण-भर भी नहीं किया। और जिसने अपने स्वयं का अध्ययन नहीं किया उसकी दूसरे पदार्थों के सम्बन्ध में बटोरी गयी जानकारी बेकार है; इसलिए अमित भाई, जिसे तुम विज्ञान कहते हो वह व्यक्ति द्वारा एकत्र की गयी वस्तुओं की जानकारी है और महावीरजैसे लोग जिसे धर्म कहते हैं, वह स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने की कला है। तुम्हें सूचना दूं कि मैं भी, मृत्यु के क्षण में ही सही, इस कला का विद्यार्थी हो गया हूँ।
तुमने लिखा है कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखू । सो हे भाई, अब मुझे लग रहा है कि इस शरीर का मैंने इस जीवन में तो क्या पिछले कई जीवनों में कितना ध्यान न रखा होगा। कितनी दवाई न की होगी। फिर भी यह शरीर अपने स्वभाव से विचलित नहीं हुआ। किसी के बहकावे या प्रलोभन में नहीं आया। जब उसे पैदा होना है, हुआ। जब उसे जवान या बूढ़ा होना है, हुआ। और जब उसे नष्ट होना है, सो हुआ। तो क्या मैं इस अचेतन शरीर से इतनी भी शिक्षा न लूँ कि मुझे भी अब अपने 'स्व' में स्थित रहना है। कहीं इसका ही अर्थ तो स्वास्थ्य प्राप्त करना नहीं है ? तब तो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ और स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूँ; स्वयं में स्थित हो रहा है।
शरीर के इस व्यामोह को काटना और उसकी चिन्ता न कर केवल आत्मा के विकास की ही चिन्ता करना अब मेरा ध्येय बन गया है। लगभग छह माह से
(शेष पृष्ट ३९ पर)
तीर्थंकर : जन. फर. ७९/३६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org