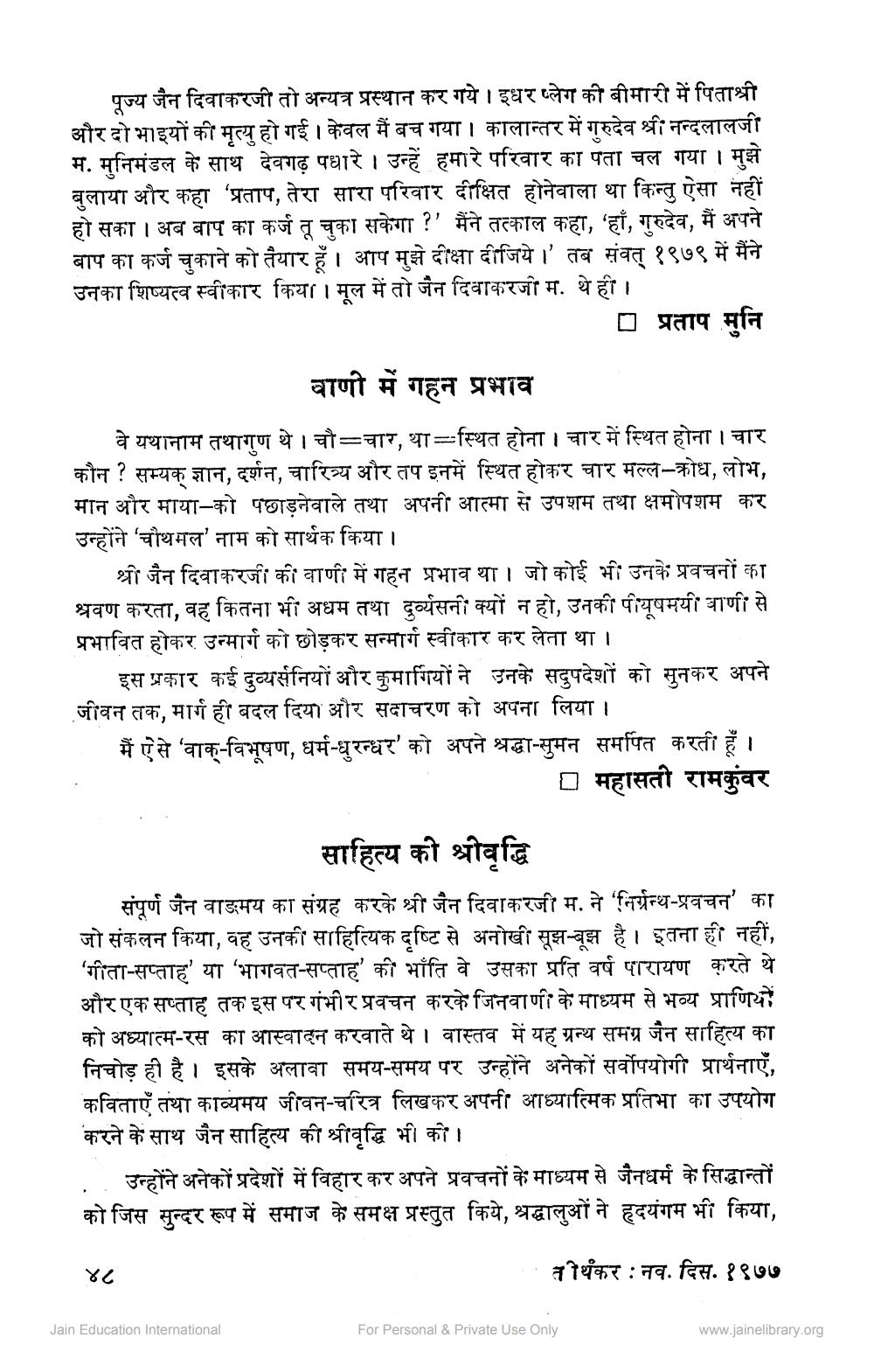________________
पूज्य जैन दिवाकरजी तो अन्यत्र प्रस्थान कर गये। इधर प्लेग की बीमारी में पिताश्री और दो भाइयों की मृत्यु हो गई। केवल मैं बच गया। कालान्तर में गुरुदेव श्री नन्दलालजी म. मुनिमंडल के साथ देवगढ़ पधारे । उन्हें हमारे परिवार का पता चल गया । मुझे बुलाया और कहा 'प्रताप, तेरा सारा परिवार दीक्षित होनेवाला था किन्तु ऐसा नहीं हो सका। अब बाप का कर्ज तू चुका सकेगा ?' मैंने तत्काल कहा, 'हाँ, गुरुदेव, मैं अपने बाप का कर्ज चुकाने को तैयार हूँ। आप मुझे दीक्षा दीजिये।' तब संवत् १९७९ में मैंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। मूल में तो जैन दिवाकरजी म. थे ही।
- प्रताप मुनि वाणी में गहन प्रभाव वे यथानाम तथागुण थे । चौ-चार, था=स्थित होना। चार में स्थित होना । चार कौन ? सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इनमें स्थित होकर चार मल्ल-क्रोध, लोभ, मान और माया को पछाड़नेवाले तथा अपनी आत्मा से उपशम तथा क्षमोपशम कर उन्होंने 'चौथमल' नाम को सार्थक किया।
श्री जैन दिवाकरजी की वाणी में गहन प्रभाव था। जो कोई भी उनके प्रवचनों का श्रवण करता, वह कितना भी अधम तथा दुर्व्यसनी क्यों न हो, उनकी पीयूषमयी वाणी से प्रभावित होकर उन्मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग स्वीकार कर लेता था।
__ इस प्रकार कई दुव्यर्सनियों और कुमागियों ने उनके सदुपदेशों को सुनकर अपने जीवन तक, मार्ग ही बदल दिया और सदाचरण को अपना लिया। मैं ऐसे 'वाक्-विभूषण, धर्म-धुरन्धर' को अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करती हूँ।
- महासती रामकुंवर
साहित्य को श्रीवृद्धि संपूर्ण जैन वाङमय का संग्रह करके श्री जैन दिवाकरजी म. ने 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' का जो संकलन किया, वह उनकी साहित्यिक दृष्टि से अनोखी सूझ-बूझ है। इतना ही नहीं, 'गीता-सप्ताह' या 'भागवत-सप्ताह' की भाँति वे उसका प्रति वर्ष पारायण करते थे
और एक सप्ताह तक इस पर गंभीर प्रवचन करके जिनवाणी के माध्यम से भव्य प्राणियों को अध्यात्म-रस का आस्वादन करवाते थे। वास्तव में यह ग्रन्थ समग्र जैन साहित्य का निचोड़ ही है। इसके अलावा समय-समय पर उन्होंने अनेकों सर्वोपयोगी प्रार्थनाएँ, कविताएँ तथा काव्यमय जीवन-चरित्र लिखकर अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा का उपयोग करने के साथ जैन साहित्य की श्रीवृद्धि भी को। . उन्होंने अनेकों प्रदेशों में विहार कर अपने प्रवचनों के माध्यम से जैनधर्म के सिद्धान्तों को जिस सुन्दर रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किये, श्रद्धालुओं ने हृदयंगम भी किया,
४८
तीर्थंकर : नव. दिस. १९७७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org