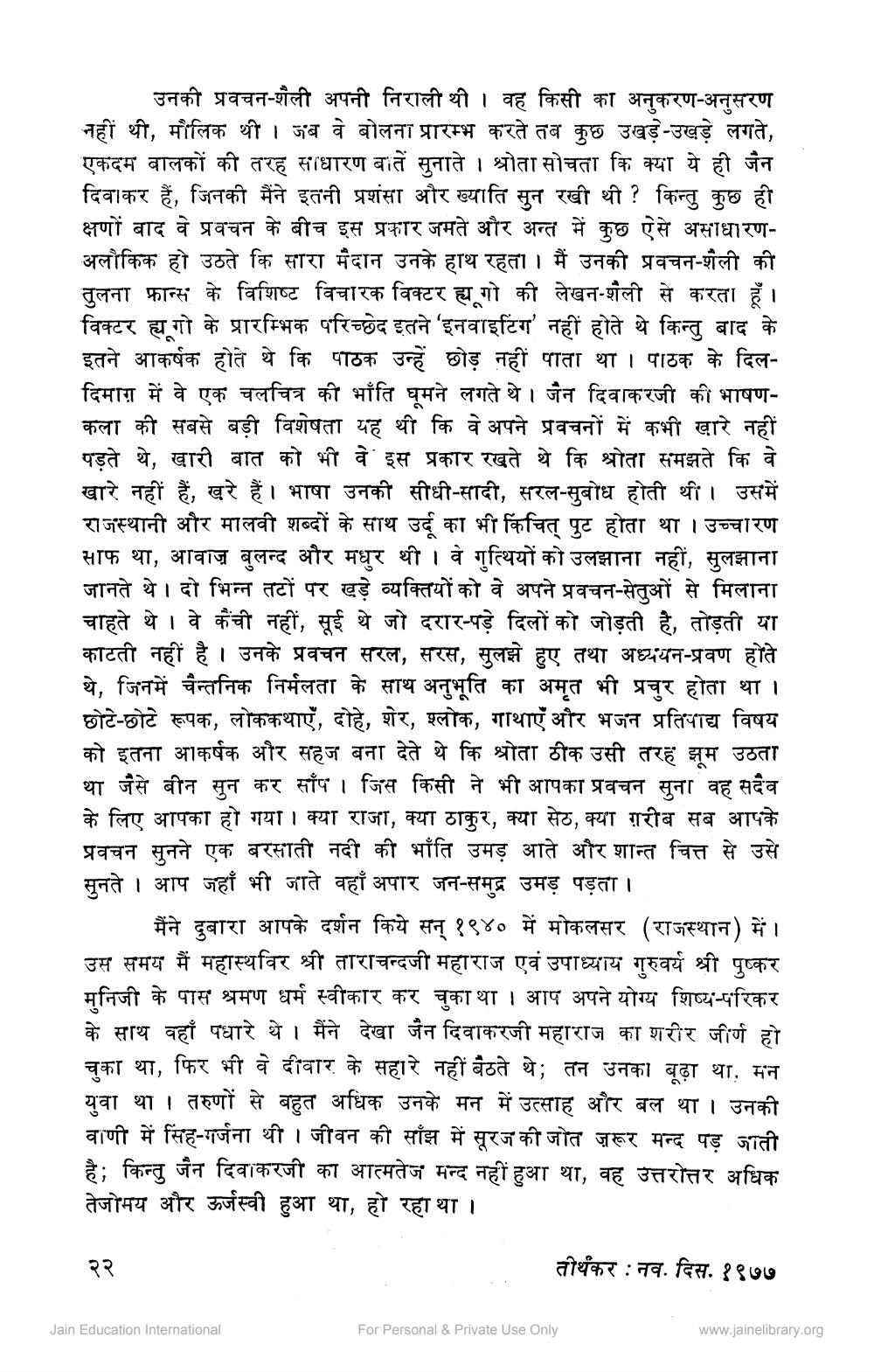________________
उनकी प्रवचन-शैली अपनी निराली थी । वह किसी का अनुकरण-अनुसरण नहीं थी, मौलिक थी। जब वे बोलना प्रारम्भ करते तब कुछ उखड़े-उखड़े लगते, एकदम बालकों की तरह साधारण बातें सुनाते । श्रोता सोचता कि क्या ये ही जैन दिवाकर हैं, जिनकी मैंने इतनी प्रशंसा और ख्याति सुन रखी थी ? किन्तु कुछ ही क्षणों बाद वे प्रवचन के बीच इस प्रकार जमते और अन्त में कुछ ऐसे असाधारणअलौकिक हो उठते कि सारा मैदान उनके हाथ रहता। मैं उनकी प्रवचन-शैली की तुलना फ्रान्स के विशिष्ट विचारक विक्टर ह्य गो की लेखन-शैली से करता हूँ। विक्टर ह्य गो के प्रारम्भिक परिच्छेद इतने 'इनवाइटिंग नहीं होते थे किन्तु बाद के इतने आकर्षक होते थे कि पाठक उन्हें छोड़ नहीं पाता था । पाठक के दिलदिमाग़ में वे एक चलचित्र की भाँति घूमने लगते थे। जैन दिवाकरजी की भाषणकला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने प्रवचनों में कभी खारे नहीं पड़ते थे, खारी बात को भी वे इस प्रकार रखते थे कि श्रोता समझते कि वे खारे नहीं हैं, खरे हैं। भाषा उनकी सीधी-सादी, सरल-सुबोध होती थी। उसमें राजस्थानी और मालवी शब्दों के साथ उर्दू का भी किंचित् पुट होता था । उच्चारण साफ था, आवाज बुलन्द और मधुर थी। वे गुत्थियों को उलझाना नहीं, सुलझाना जानते थे। दो भिन्न तटों पर खड़े व्यक्तियों को वे अपने प्रवचन-सेतुओं से मिलाना चाहते थे। वे कैंची नहीं, सूई थे जो दरार-पड़े दिलों को जोड़ती है, तोड़ती या काटती नहीं है । उनके प्रवचन सरल, सरस, सुलझे हुए तथा अध्ययन-प्रवण होते थे, जिनमें चैन्तनिक निर्मलता के साथ अनुभूति का अमृत भी प्रचुर होता था। छोटे-छोटे रूपक, लोककथाएँ, दोहे, शेर, श्लोक, गाथाएँ और भजन प्रतिपाद्य विषय को इतना आकर्षक और सहज बना देते थे कि श्रोता ठीक उसी तरह झूम उठता था जैसे बीन सुन कर साँप । जिस किसी ने भी आपका प्रवचन सुना वह सदैव के लिए आपका हो गया। क्या राजा, क्या ठाकुर, क्या सेठ, क्या ग़रीब सब आपके प्रवचन सुनने एक बरसाती नदी की भाँति उमड़ आते और शान्त चित्त से उसे सुनते । आप जहाँ भी जाते वहाँ अपार जन-समुद्र उमड़ पड़ता।
___मैंने दुबारा आपके दर्शन किये सन् १९४० में मोकलसर (राजस्थान) में। उस समय मैं महास्थविर श्री ताराचन्दजी महाराज एवं उपाध्याय गुरुवर्य श्री पुष्कर मनिजी के पास श्रमण धर्म स्वीकार कर चुका था । आप अपने योग्य शिष्य-परिकर के साथ वहाँ पधारे थे। मैंने देखा जैन दिवाकरजी महाराज का शरीर जीर्ण हो चुका था, फिर भी वे दीवार के सहारे नहीं बैठते थे; तन उनका बूढ़ा था. मन युवा था । तरुणों से बहुत अधिक उनके मन में उत्साह और बल था। उनकी वाणी में सिंह-गर्जना थी । जीवन की साँझ में सूरज की जोत ज़रूर मन्द पड़ जाती है; किन्तु जैन दिवाकरजी का आत्मतेज मन्द नहीं हुआ था, वह उत्तरोत्तर अधिक तेजोमय और ऊर्जस्वी हुआ था, हो रहा था।
२२
तीर्थंकर : नव. दिस. १९७७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org