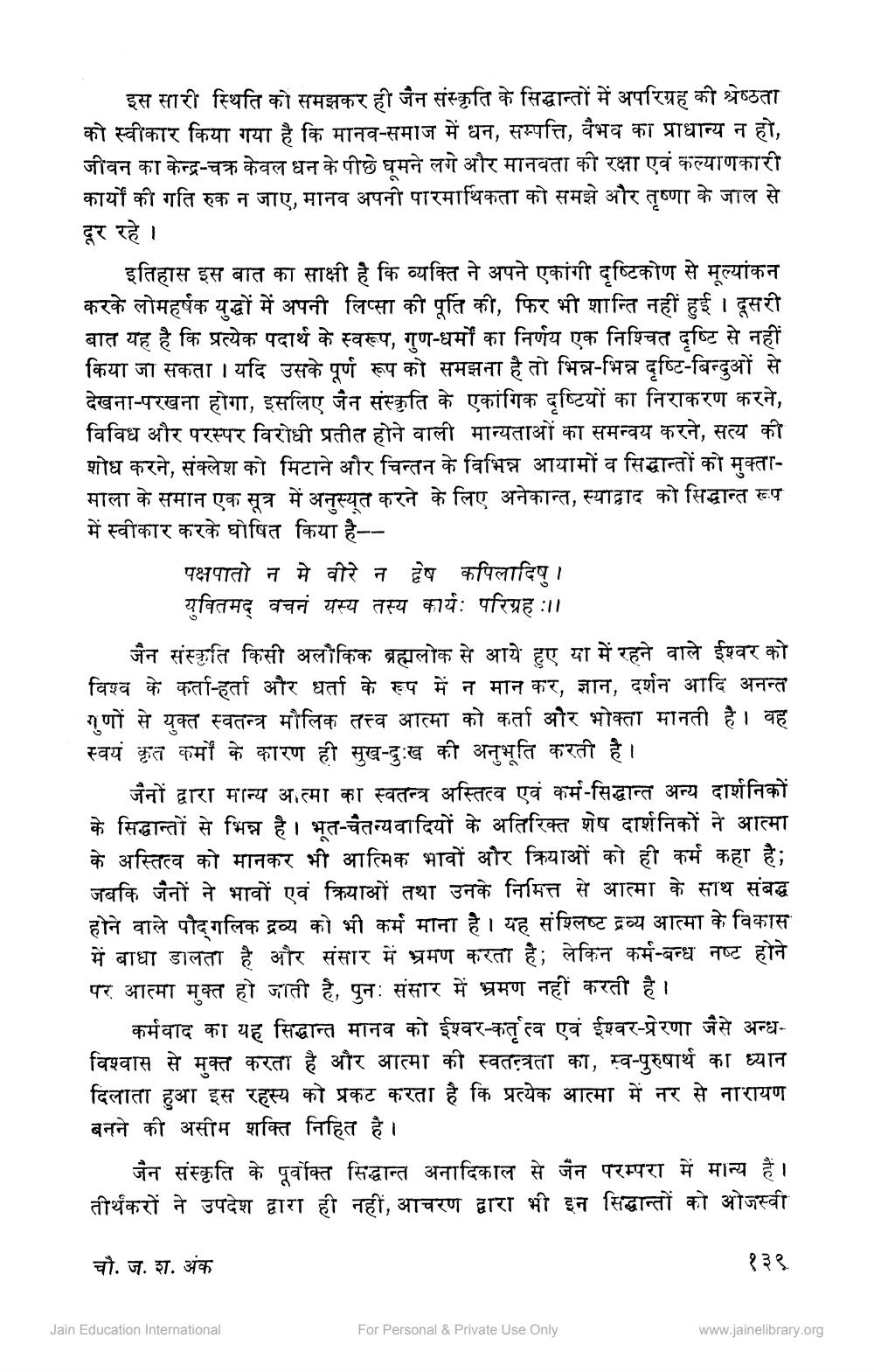________________
इस सारी स्थिति को समझकर ही जैन संस्कृति के सिद्धान्तों में अपरिग्रह की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है कि मानव-समाज में धन, सम्पत्ति, वैभव का प्राधान्य न हो, जीवन का केन्द्र-चक्र केवल धन के पीछे घूमने लगे और मानवता की रक्षा एवं कल्याणकारी कार्यों की गति रुक न जाए, मानव अपनी पारमार्थिकता को समझे और तृष्णा के जाल से दूर रहे। ___इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति ने अपने एकांगी दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके लोमहर्षक युद्धों में अपनी लिप्सा की पूर्ति की, फिर भी शान्ति नहीं हुई । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप, गुण-धर्मों का निर्णय एक निश्चित दृष्टि से नहीं किया जा सकता । यदि उसके पूर्ण रूप को समझना है तो भिन्न-भिन्न दृष्टि-बिन्दुओं से देखना-परखना होगा, इसलिए जैन संस्कृति के एकांगिक दृष्टियों का निराकरण करने, विविध और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली मान्यताओं का समन्वय करने, सत्य की शोध करने, संक्लेश को मिटाने और चिन्तन के विभिन्न आयामों व सिद्धान्तों को मुक्तामाला के समान एक सूत्र में अनुस्यूत करने के लिए अनेकान्त, स्याद्वाद को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करके घोषित किया है--
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु ।
युवितमद् वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह :।। जैन संस्कृति किसी अलौकिक ब्रह्मलोक से आये हुए या में रहने वाले ईश्वर को विश्व के कर्ता-हर्ता और धर्ता के रूप में न मान कर, ज्ञान, दर्शन' आदि अनन्त गुणों से युक्त स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानती है। वह स्वयं कृत कर्मों के कारण ही सुख-दुःख की अनुभूति करती है।
जैनों द्वारा मान्य आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व एवं कर्म-सिद्धान्त अन्य दार्शनिकों के सिद्धान्तों से भिन्न है। भूत-चैतन्यवादियों के अतिरिक्त शेष दार्शनिकों ने आत्मा के अस्तित्व को मानकर भी आत्मिक भावों और क्रियाओं को ही कर्म कहा है; जबकि जैनों ने भावों एवं क्रियाओं तथा उनके निमित्त से आत्मा के साथ संबद्ध होने वाले पौद्गलिक द्रव्य को भी कर्म माना है। यह संश्लिष्ट द्रव्य आत्मा के विकास में बाधा डालता है और संसार में भ्रमण करता है; लेकिन कर्म-बन्ध नष्ट होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है, पुनः संसार में भ्रमण नहीं करती है।
कर्मवाद का यह सिद्धान्त मानव को ईश्वर-कर्तृत्व एवं ईश्वर-प्रेरणा जैसे अन्धविश्वास से मुक्त करता है और आत्मा की स्वतन्त्रता का, स्व-पुरुषार्थ का ध्यान दिलाता हुआ इस रहस्य को प्रकट करता है कि प्रत्येक आत्मा में नर से नारायण बनने की असीम शक्ति निहित है।
जैन संस्कृति के पूर्वोक्त सिद्धान्त अनादिकाल से जैन परम्परा में मान्य हैं। तीर्थंकरों ने उपदेश द्वारा ही नहीं, आचरण द्वारा भी इन सिद्धान्तों को ओजस्वी
चौ. ज. श. अंक
१३९
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org