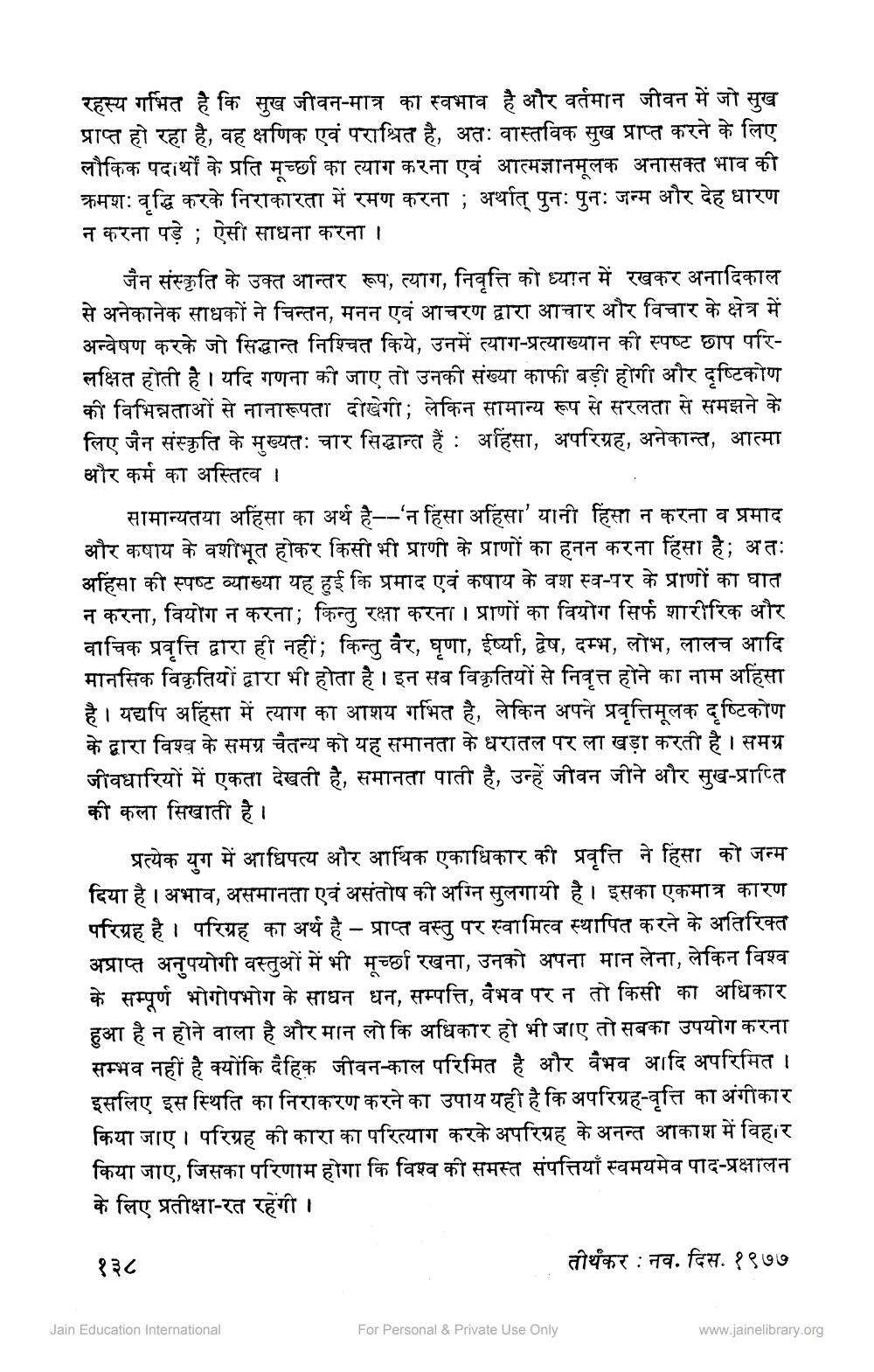________________
रहस्य गभित है कि सुख जीवन-मात्र का स्वभाव है और वर्तमान जीवन में जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह क्षणिक एवं पराश्रित है, अतः वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए लौकिक पदार्थों के प्रति मूर्छा का त्याग करना एवं आत्मज्ञानमूलक अनासक्त भाव की क्रमशः वृद्धि करके निराकारता में रमण करना ; अर्थात् पुनः पुनः जन्म और देह धारण न करना पड़े ; ऐसी साधना करना ।
जैन संस्कृति के उक्त आन्तर रूप', त्याग, निवृत्ति को ध्यान में रखकर अनादिकाल से अनेकानेक साधकों ने चिन्तन, मनन एवं आचरण द्वारा आचार और विचार के क्षेत्र में अन्वेषण करके जो सिद्धान्त निश्चित किये, उनमें त्याग-प्रत्याख्यान की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। यदि गणना की जाए तो उनकी संख्या काफी बड़ी होगी और दृष्टिकोण की विभिन्नताओं से नानारूपता दोखेगी; लेकिन सामान्य रूप से सरलता से समझने के लिए जैन संस्कृति के मुख्यतः चार सिद्धान्त हैं : अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्त, आत्मा और कर्म का अस्तित्व ।
सामान्यतया अहिंसा का अर्थ है--'न हिंसा अहिंसा' यानी हिंसा न करना व प्रमाद और कषाय के वशीभूत होकर किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन करना हिंसा है; अतः
की स्पष्ट व्याख्या यह हई कि प्रमाद एवं कषाय के वश स्व-पर के प्राणों का घात न करना, वियोग न करना; किन्तु रक्षा करना । प्राणों का वियोग सिर्फ शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति द्वारा ही नहीं; किन्तु वैर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, लोभ, लालच आदि मानसिक विकृतियों द्वारा भी होता है । इन सब विकृतियों से निवृत्त होने का नाम अहिंसा है। यद्यपि अहिंसा में त्याग का आशय गभित है, लेकिन अपने प्रवृत्तिमूलक दृष्टिकोण के द्वारा विश्व के समग्र चैतन्य को यह समानता के धरातल पर ला खड़ा करती है । समग्र जीवधारियों में एकता देखती है, समानता पाती है, उन्हें जीवन जीने और सुख-प्राप्ति की कला सिखाती है।
प्रत्येक युग में आधिपत्य और आर्थिक एकाधिकार की प्रवृत्ति ने हिंसा को जन्म दिया है । अभाव, असमानता एवं असंतोष की अग्नि सुलगायी है। इसका एकमात्र कारण परिग्रह है। परिग्रह का अर्थ है - प्राप्त वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करने के अतिरिक्त अप्राप्त अनुपयोगी वस्तुओं में भी मूर्छा रखना, उनको अपना मान लेना, लेकिन विश्व के सम्पूर्ण भोगोपभोग के साधन धन, सम्पत्ति, वैभव पर न तो किसी का अधिकार हुआ है न होने वाला है और मान लो कि अधिकार हो भी जाए तो सबका उपयोग करना सम्भव नहीं है क्योंकि दैहिक जीवन-काल परिमित है और वैभव आदि अपरिमित । इसलिए इस स्थिति का निराकरण करने का उपाय यही है कि अपरिग्रह-वृत्ति का अंगीकार किया जाए। परिग्रह की कारा का परित्याग करके अपरिग्रह के अनन्त आकाश में विहार किया जाए, जिसका परिणाम होगा कि विश्व की समस्त संपत्तियाँ स्वमयमेव पाद-प्रक्षालन के लिए प्रतीक्षा-रत रहेंगी।
१३८
तीर्थंकर : नव. दिस. १९७७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org