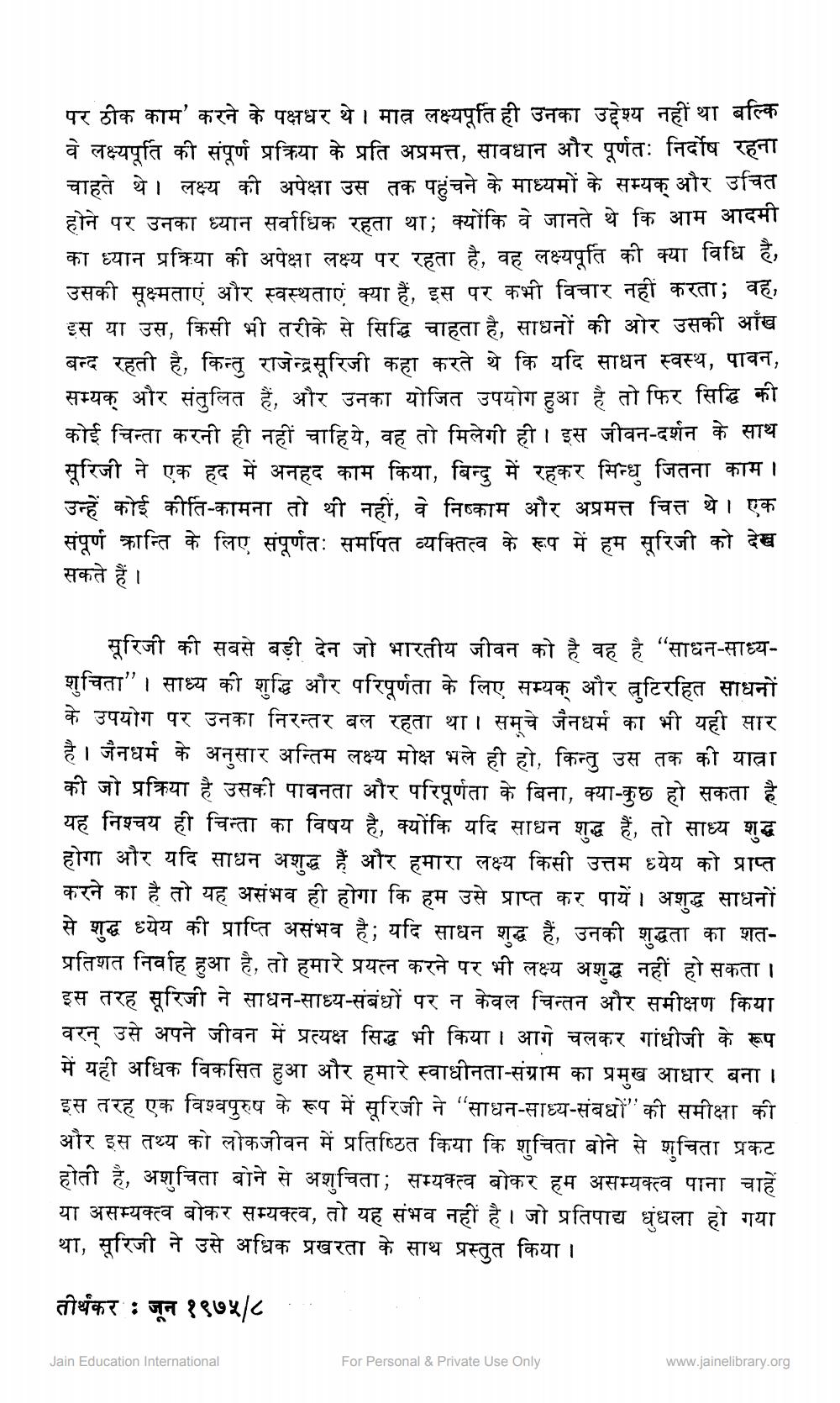________________
पर ठीक काम' करने के पक्षधर थे। मात्र लक्ष्यपूर्ति ही उनका उद्देश्य नहीं था बल्कि वे लक्ष्यपूर्ति की संपूर्ण प्रक्रिया के प्रति अप्रमत्त, सावधान और पूर्णतः निर्दोष रहना चाहते थे। लक्ष्य की अपेक्षा उस तक पहुंचने के माध्यमों के सम्यक् और उचित होने पर उनका ध्यान सर्वाधिक रहता था; क्योंकि वे जानते थे कि आम आदमी का ध्यान प्रक्रिया की अपेक्षा लक्ष्य पर रहता है, वह लक्ष्यपूर्ति की क्या विधि हैं, उसकी सूक्ष्मताएं और स्वस्थताएं क्या हैं, इस पर कभी विचार नहीं करता; वह, इस या उस, किसी भी तरीके से सिद्धि चाहता है, साधनों की ओर उसकी आँख बन्द रहती है, किन्तु राजेन्द्रसूरिजी कहा करते थे कि यदि साधन स्वस्थ, पावन, सम्यक् और संतुलित हैं, और उनका योजित उपयोग हआ है तो फिर सिद्धि की कोई चिन्ता करनी ही नहीं चाहिये, वह तो मिलेगी ही। इस जीवन-दर्शन के साथ सूरिजी ने एक हद में अनहद काम किया, बिन्दु में रहकर सिन्धु जितना काम। उन्हें कोई कीति-कामना तो थी नहीं, वे निष्काम और अप्रमत्त चित्त थे। एक संपूर्ण क्रान्ति के लिए संपूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व के रूप में हम सूरिजी को देख सकते हैं।
सूरिजी की सबसे बड़ी देन जो भारतीय जीवन को है वह है “साधन-साध्यशुचिता"। साध्य की शुद्धि और परिपूर्णता के लिए सम्यक् और त्रुटिरहित साधनों के उपयोग पर उनका निरन्तर बल रहता था। सम्चे जैनधर्म का भी यही सार है। जैनधर्म के अनुसार अन्तिम लक्ष्य मोक्ष भले ही हो, किन्तु उस तक की यात्रा की जो प्रक्रिया है उसकी पावनता और परिपूर्णता के बिना, क्या-कुछ हो सकता है यह निश्चय ही चिन्ता का विषय है, क्योंकि यदि साधन शुद्ध हैं, तो साध्य शुद्ध होगा और यदि साधन अशुद्ध हैं और हमारा लक्ष्य किसी उत्तम ध्येय को प्राप्त करने का है तो यह असंभव ही होगा कि हम उसे प्राप्त कर पायें। अशुद्ध साधनों से शुद्ध ध्येय की प्राप्ति असंभव है; यदि साधन शुद्ध हैं, उनकी शुद्धता का शतप्रतिशत निर्वाह हुआ है, तो हमारे प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य अशुद्ध नहीं हो सकता। इस तरह सूरिजी ने साधन-साध्य-संबंधों पर न केवल चिन्तन और समीक्षण किया वरन् उसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष सिद्ध भी किया। आगे चलकर गांधीजी के रूप में यही अधिक विकसित हुआ और हमारे स्वाधीनता-संग्राम का प्रमुख आधार बना। इस तरह एक विश्वपुरुष के रूप में सूरिजी ने “साधन-साध्य-संबधों" की समीक्षा की
और इस तथ्य को लोकजीवन में प्रतिष्ठित किया कि शुचिता बोने से शुचिता प्रकट होती है, अशुचिता बोने से अशुचिता; सम्यक्त्व बोकर हम असम्यक्त्व पाना चाहें या असम्यक्त्व बोकर सम्यक्त्व, तो यह संभव नहीं है। जो प्रतिपाद्य धुंधला हो गया था, सूरिजी ने उसे अधिक प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया।
तीर्थकर : जून १९७५/८
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org