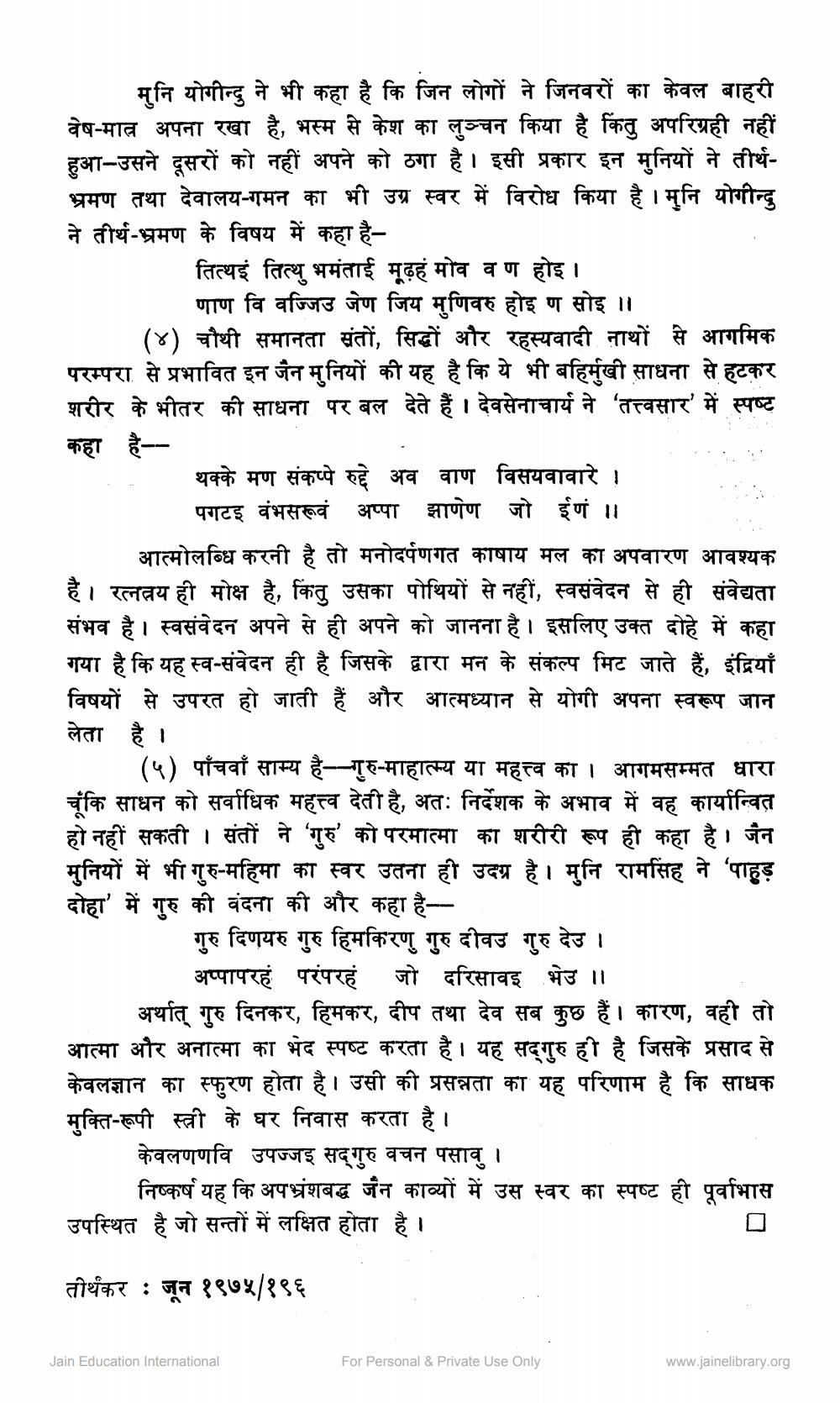________________
मुनि योगीन्दु ने भी कहा है कि जिन लोगों ने जिनवरों का केवल बाहरी वेष-मात्र अपना रखा है, भस्म से केश का लुञ्चन किया है किंतु अपरिग्रही नहीं हुआ-उसने दूसरों को नहीं अपने को ठगा है। इसी प्रकार इन मुनियों ने तीर्थभ्रमण तथा देवालय-गमन का भी उग्र स्वर में विरोध किया है । मुनि योगीन्दु ने तीर्थ-भ्रमण के विषय में कहा है
तित्थई तित्थु भमंताई मूढ़हं मोव व ण होइ।
णाण वि वज्जिउ जेण जिय मुणिवरु होइ ण सोइ ॥ (४) चौथी समानता संतों, सिद्धों और रहस्यवादी नाथों से आगमिक परम्परा से प्रभावित इन जैन मुनियों की यह है कि ये भी बहिर्मुखी साधना से हटकर शरीर के भीतर की साधना पर बल देते हैं । देवसेनाचार्य ने 'तत्त्वसार' में स्पष्ट कहा है--
थक्के मण संकप्पे रुद्दे अव वाण विसयवावारे ।
पगटइ वंभसरूवं अप्पा झाणेण जो ईणं ॥
आत्मोलब्धि करनी है तो मनोदर्पणगत काषाय मल का अपवारण आवश्यक है। रत्नत्रय ही मोक्ष है, किंतु उसका पोथियों से नहीं, स्वसंवेदन से ही संवेद्यता संभव है। स्वसंवेदन अपने से ही अपने को जानना है। इसलिए उक्त दोहे में कहा गया है कि यह स्व-संवेदन ही है जिसके द्वारा मन के संकल्प मिट जाते हैं, इंद्रियाँ विषयों से उपरत हो जाती हैं और आत्मध्यान से योगी अपना स्वरूप जान लेता है।
(५) पाँचवाँ साम्य है-गुरु-माहात्म्य या महत्त्व का। आगमसम्मत धारा चूंकि साधन को सर्वाधिक महत्त्व देती है, अतः निर्देशक के अभाव में वह कार्यान्वित हो नहीं सकती । संतों ने 'गुरु' को परमात्मा का शरीरी रूप ही कहा है। जैन मुनियों में भी गुरु-महिमा का स्वर उतना ही उदग्र है। मुनि रामसिंह ने 'पाहुड़ दोहा' में गुरु की वंदना की और कहा है
गुरु दिणयरु गुरु हिमकिरणु गुरु दीवउ गुरु देउ ।
अप्पापरहं परंपरहं जो दरिसावइ भेउ ।। अर्थात् गुरु दिनकर, हिमकर, दीप तथा देव सब कुछ हैं। कारण, वही तो आत्मा और अनात्मा का भेद स्पष्ट करता है। यह सद्गुरु ही है जिसके प्रसाद से केवलज्ञान का स्फुरण होता है। उसी की प्रसन्नता का यह परिणाम है कि साधक मुक्ति-रूपी स्त्री के घर निवास करता है।
केवलणणवि उपज्जइ सद्गुरु वचन पसावु ।
निष्कर्ष यह कि अपभ्रंशबद्ध जैन काव्यों में उस स्वर का स्पष्ट ही पूर्वाभास उपस्थित है जो सन्तों में लक्षित होता है।
तीर्थंकर : जून १९७५/१९६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org