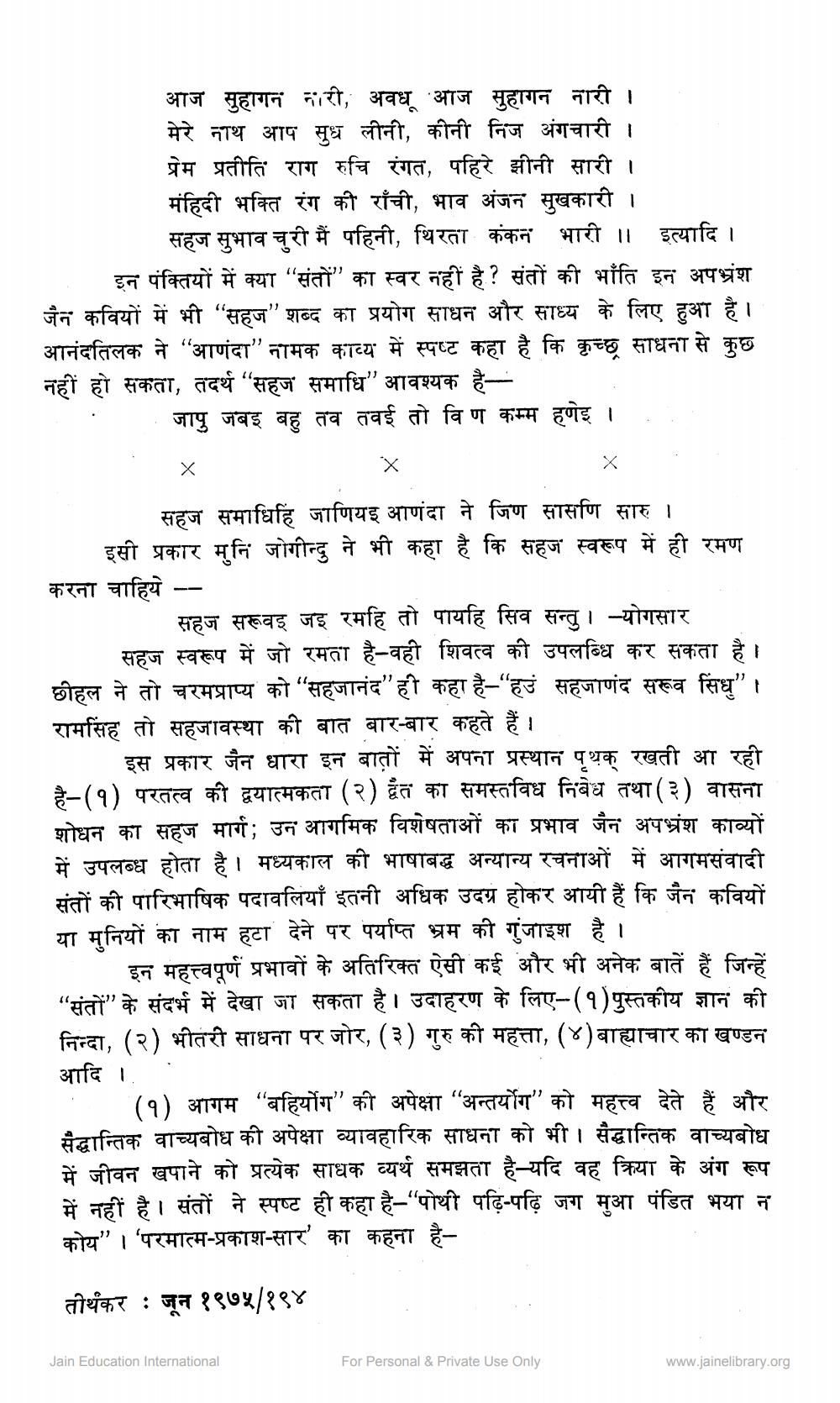________________
आज सुहागन नारी, अवधू आज सुहागन नारी । मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी निज अंगचारी । प्रेम प्रतीति राग रुचि रंगत, पहिरे झीनी सारी । मंहिदी भक्ति रंग की राँची, भाव अंजन सुखकारी ।
सहज सुभाव चुरी मैं पहिनी, थिरता कंकन भारी ।। इत्यादि । इन पंक्तियों में क्या “संतों” का स्वर नहीं है ? संतों की भाँति इन अपभ्रंश जैन कवियों में भी “सहज' शब्द का प्रयोग साधन और साध्य के लिए हुआ है। आनंदतिलक ने “आणंदा" नामक काव्य में स्पष्ट कहा है कि कृच्छ्र साधना से कुछ नहीं हो सकता, तदर्थ “सहज समाधि" आवश्यक है
जापु जबइ बहु तव तवई तो वि ण कम्म हणेइ ।
सहज समाधिहिं जाणियइ आणंदा ने जिण सासणि सारु । इसी प्रकार मुनि जोगीन्दु ने भी कहा है कि सहज स्वरूप में ही रमण करना चाहिये --
सहज सरूवइ जइ रमहि तो पायहि सिव सन्तु। -योगसार सहज स्वरूप में जो रमता है-वही शिवत्व की उपलब्धि कर सकता है। छीहल ने तो चरमप्राप्य को “सहजानंद" ही कहा है-“हउं सहजाणंद सरूव सिंधु" । रामसिंह तो सहजावस्था की बात बार-बार कहते हैं ।
इस प्रकार जैन धारा इन बातों में अपना प्रस्थान पथक रखती आ रही है-(१) परतत्व की द्वयात्मकता (२) द्वैत का समस्तविध निबेध तथा (३) वासना शोधन का सहज मार्ग; उन आगमिक विशेषताओं का प्रभाव जैन अपभ्रंश काव्यों में उपलब्ध होता है। मध्यकाल की भाषाबद्ध अन्यान्य रचनाओं में आगमसंवादी संतों की पारिभाषिक पदावलियाँ इतनी अधिक उदग्र होकर आयी हैं कि जैन कवियों या मुनियों का नाम हटा देने पर पर्याप्त भ्रम की गुंजाइश है ।
इन महत्त्वपूर्ण प्रभावों के अतिरिक्त ऐसी कई और भी अनेक बातें हैं जिन्हें "संतों" के संदर्भ में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए-(१)पुस्तकीय ज्ञान की निन्दा, (२) भीतरी साधना पर जोर, (३) गुरु की महत्ता, (४) बाह्याचार का खण्डन आदि ।
(१) आगम “बहिर्योग' की अपेक्षा "अन्तर्योग” को महत्त्व देते हैं और सैद्धान्तिक वाच्यबोध की अपेक्षा व्यावहारिक साधना को भी। सैद्धान्तिक वाच्यबोध में जीवन खपाने को प्रत्येक साधक व्यर्थ समझता है यदि वह क्रिया के अंग रूप में नहीं है। संतों ने स्पष्ट ही कहा है-“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोय" । 'परमात्म-प्रकाश-सार' का कहना है
तीर्थंकर : जून १९७५/१९४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org