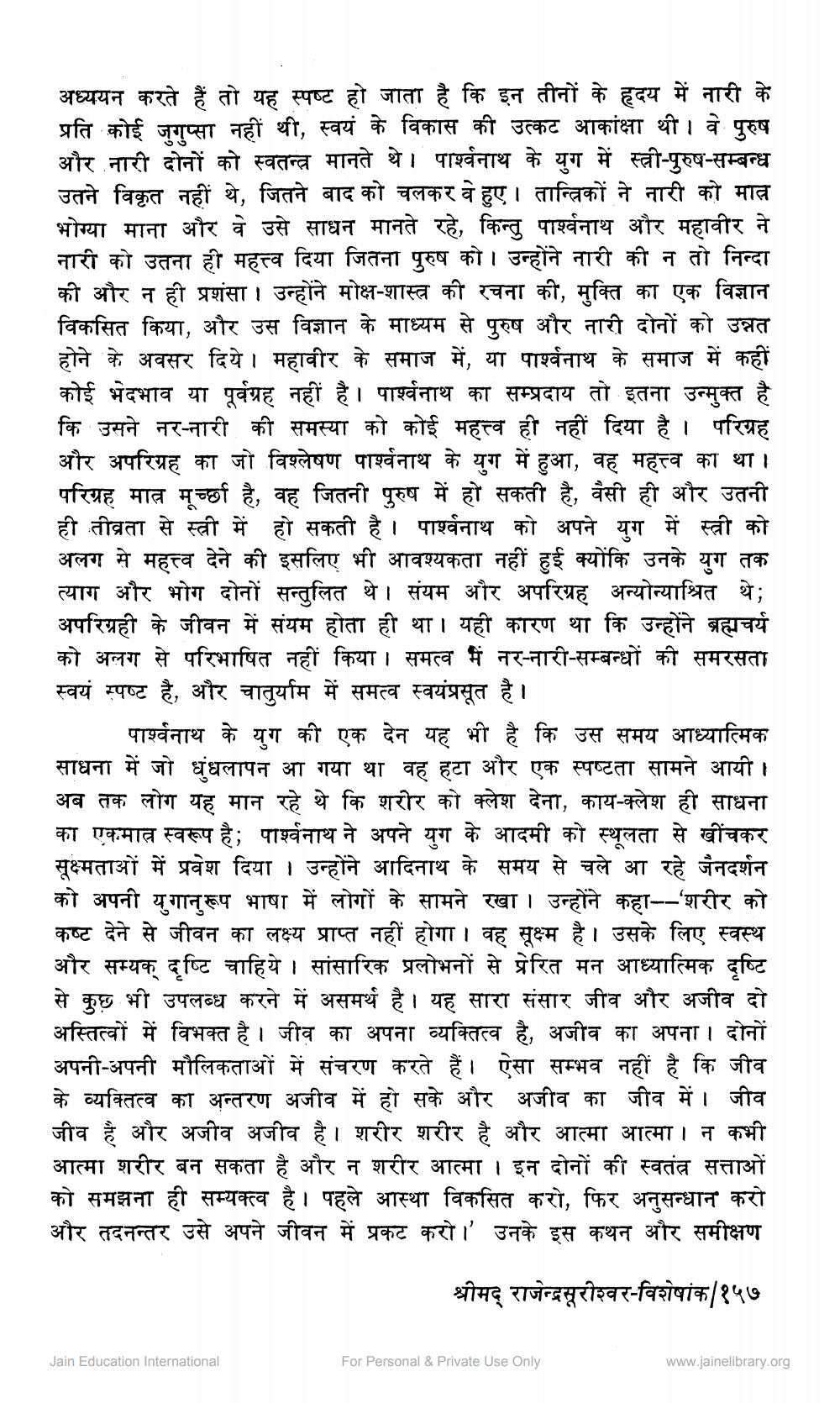________________
अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों के हृदय में नारी के प्रति कोई जगप्सा नहीं थी, स्वयं के विकास की उत्कट आकांक्षा थी। वे पुरुष और नारी दोनों को स्वतन्त्र मानते थे। पार्श्वनाथ के युग में स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध उतने विकृत नहीं थे, जितने बाद को चलकर वे हुए। तान्त्रिकों ने नारी को मात्र भोग्या माना और वे उसे साधन मानते रहे, किन्तु पार्श्वनाथ और महावीर ने नारी को उतना ही महत्त्व दिया जितना पुरुष को। उन्होंने नारी की न तो निन्दा की और न ही प्रशंसा। उन्होंने मोक्ष-शास्त्र की रचना की, मुक्ति का एक विज्ञान विकसित किया, और उस विज्ञान के माध्यम से पुरुष और नारी दोनों को उन्नत होने के अवसर दिये। महावीर के समाज में, या पार्श्वनाथ के समाज में कहीं कोई भेदभाव या पूर्वग्रह नहीं है। पार्श्वनाथ का सम्प्रदाय तो इतना उन्मुक्त है कि उसने नर-नारी की समस्या को कोई महत्त्व ही नहीं दिया है। परिग्रह
और अपरिग्रह का जो विश्लेषण पार्श्वनाथ के युग में हुआ, वह महत्त्व का था। परिग्रह मात्र मूर्छा है, वह जितनी पुरुष में हो सकती है, वैसी ही और उतनी ही तीव्रता से स्त्री में हो सकती है। पार्श्वनाथ को अपने युग में स्त्री को अलग से महत्त्व देने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि उनके युग तक त्याग और भोग दोनों सन्तुलित थे। संयम और अपरिग्रह अन्योन्याश्रित थे; अपरिग्रही के जीवन में संयम होता ही था। यही कारण था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को अलग से परिभाषित नहीं किया। समत्व मैं नर-नारी-सम्बन्धों की समरसता स्वयं स्पष्ट है, और चातुर्याम में समत्व स्वयंप्रसूत है।
पार्श्वनाथ के युग की एक देन यह भी है कि उस समय आध्यात्मिक साधना में जो धुंधलापन आ गया था वह हटा और एक स्पष्टता सामने आयी। अब तक लोग यह मान रहे थे कि शरीर को क्लेश देना, काय-क्लेश ही साधना का एकमात्र स्वरूप है; पार्श्वनाथ ने अपने युग के आदमी को स्थूलता से खींचकर सूक्ष्मताओं में प्रवेश दिया। उन्होंने आदिनाथ के समय से चले आ रहे जैनदर्शन को अपनी युगानुरूप भाषा में लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा--'शरीर को कष्ट देने से जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। वह सूक्ष्म है। उसके लिए स्वस्थ और सम्यक दृष्टि चाहिये । सांसारिक प्रलोभनों से प्रेरित मन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी उपलब्ध करने में असमर्थ है। यह सारा संसार जीव और अजीव दो अस्तित्वों में विभक्त है। जीव का अपना व्यक्तित्व है, अजीव का अपना। दोनों अपनी-अपनी मौलिकताओं में संचरण करते हैं। ऐसा सम्भव नहीं है कि जीव के व्यक्तित्व का अन्तरण अजीव में हो सके और अजीव का जीव में। जीव जीव है और अजीव अजीव है। शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा। न कभी आत्मा शरीर बन सकता है और न शरीर आत्मा । इन दोनों की स्वतंत्र सत्ताओं को समझना ही सम्यक्त्व है। पहले आस्था विकसित करो, फिर अनुसन्धान करो और तदनन्तर उसे अपने जीवन में प्रकट करो।' उनके इस कथन और समीक्षण
श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वर-विशेषांक/१५७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org