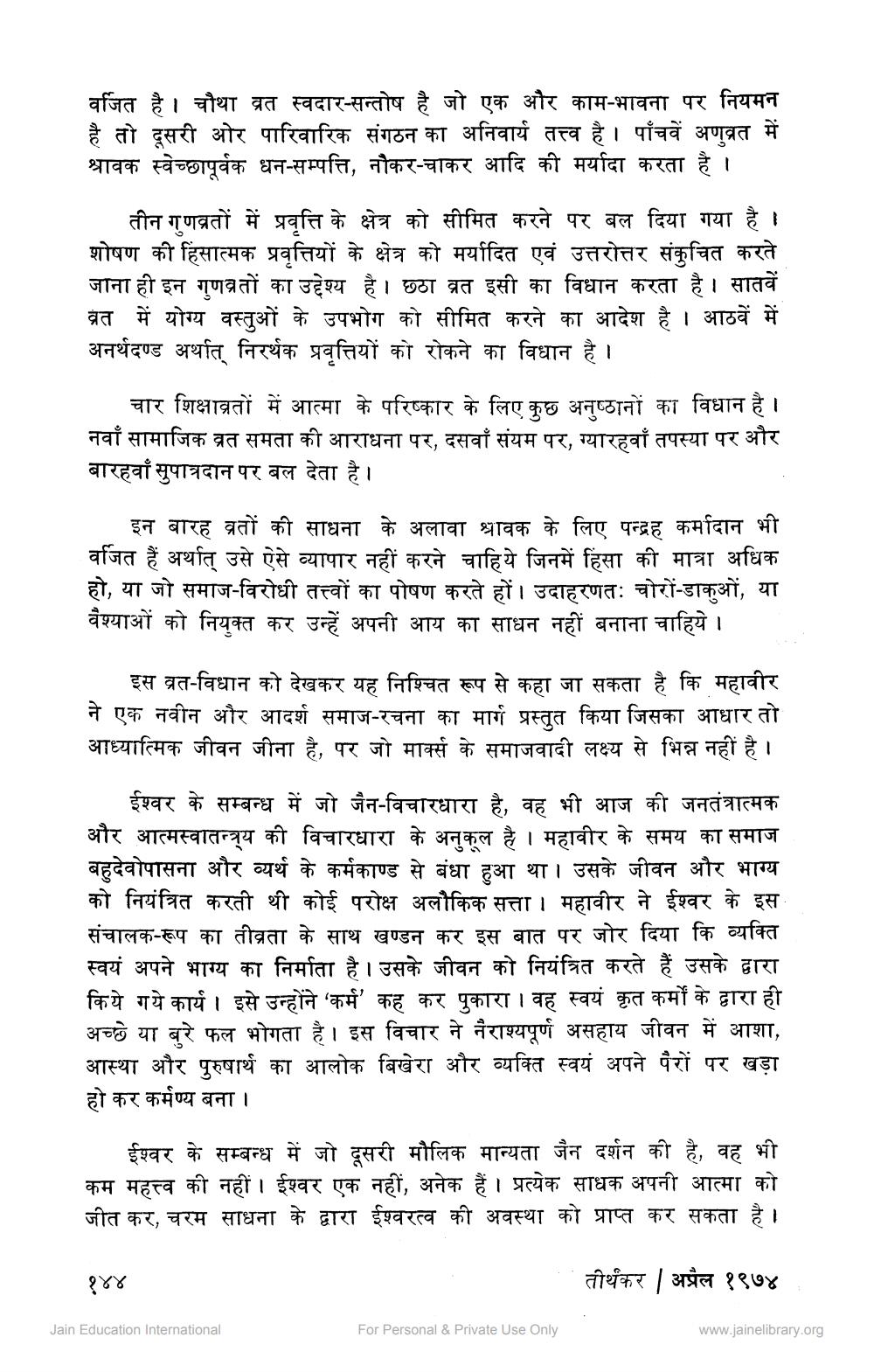________________
वर्जित है। चौथा व्रत स्वदार-सन्तोष है जो एक और काम-भावना पर नियमन है तो दूसरी ओर पारिवारिक संगठन का अनिवार्य तत्त्व है। पाँचवें अणुव्रत में श्रावक स्वेच्छापूर्वक धन-सम्पत्ति, नौकर-चाकर आदि की मर्यादा करता है ।
तीन गुणव्रतों में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया है । शोषण की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मर्यादित एवं उत्तरोत्तर संकुचित करते जाना ही इन गुणवतों का उद्देश्य है। छठा व्रत इसी का विधान करता है। सातवें व्रत में योग्य वस्तुओं के उपभोग को सीमित करने का आदेश है । आठवें में अनर्थदण्ड अर्थात् निरर्थक प्रवृत्तियों को रोकने का विधान है।
चार शिक्षाव्रतों में आत्मा के परिष्कार के लिए कुछ अनुष्ठानों का विधान है। नवाँ सामाजिक व्रत समता की आराधना पर, दसवाँ संयम पर, ग्यारहवाँ तपस्या पर और बारहवाँ सुपात्रदान पर बल देता है।
____ इन बारह व्रतों की साधना के अलावा श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान भी वर्जित हैं अर्थात् उसे ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिये जिनमें हिंसा की मात्रा अधिक हो, या जो समाज-विरोधी तत्त्वों का पोषण करते हों। उदाहरणतः चोरों-डाकुओं, या वैश्याओं को नियुक्त कर उन्हें अपनी आय का साधन नहीं बनाना चाहिये।
___ इस व्रत-विधान को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महावीर ने एक नवीन और आदर्श समाज-रचना का मार्ग प्रस्तुत किया जिसका आधार तो आध्यात्मिक जीवन जीना है, पर जो मार्क्स के समाजवादी लक्ष्य से भिन्न नहीं है ।
ईश्वर के सम्बन्ध में जो जैन-विचारधारा है, वह भी आज की जनतंत्रात्मक और आत्मस्वातन्त्र्य की विचारधारा के अनुकूल है । महावीर के समय का समाज बहुदेवोपासना और व्यर्थ के कर्मकाण्ड से बंधा हुआ था। उसके जीवन और भाग्य को नियंत्रित करती थी कोई परोक्ष अलौकिक सत्ता। महावीर ने ईश्वर के इस संचालक-रूप का तीव्रता के साथ खण्डन कर इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं उसके द्वारा किये गये कार्य । इसे उन्होंने 'कर्म' कह कर पुकारा । वह स्वयं कृत कर्मों के द्वारा ही अच्छे या बुरे फल भोगता है। इस विचार ने नैराश्यपूर्ण असहाय जीवन में आशा, आस्था और पुरुषार्थ का आलोक बिखेरा और व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो कर कर्मण्य बना।
ईश्वर के सम्बन्ध में जो दूसरी मौलिक मान्यता जैन दर्शन की है, वह भी कम महत्त्व की नहीं। ईश्वर एक नहीं, अनेक हैं। प्रत्येक साधक अपनी आत्मा को जीत कर, चरम साधना के द्वारा ईश्वरत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
१४४
तीर्थंकर | अप्रैल १९७४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org