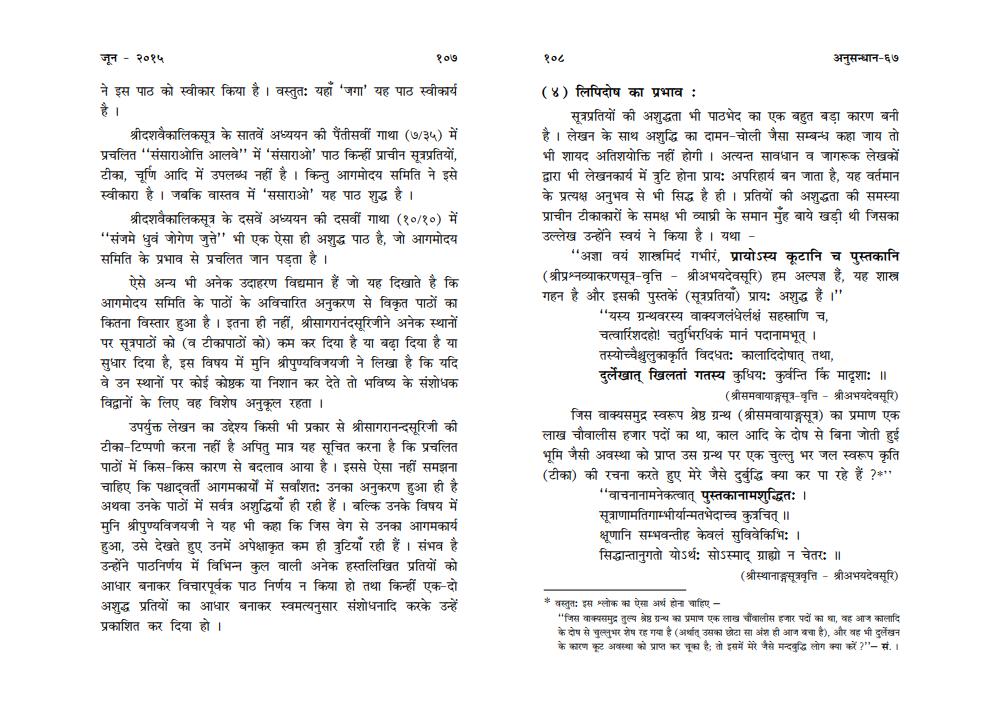________________
जून - २०१५
१०७
१०८
अनुसन्धान-६७
ने इस पाठ को स्वीकार किया है । वस्तुत: यहाँ 'जगा' यह पाठ स्वीकार्य
श्रीदशवैकालिकसूत्र के सातवें अध्ययन की पैंतीसवीं गाथा (७/३५) में प्रचलित "संसाराओत्ति आलवे" में 'संसाराओ' पाठ किन्हीं प्राचीन सूत्रप्रतियों, टीका, चूणि आदि में उपलब्ध नहीं है। किन्तु आगमोदय समिति ने इसे स्वीकारा है । जबकि वास्तव में 'ससाराओ' यह पाठ शुद्ध है।
श्रीदशवकालिकसत्र के दसवें अध्ययन की दसवीं गाथा (१०/१०) में "संजमे धुर्व जोगेण जुत्ते" भी एक ऐसा ही अशुद्ध पाठ है, जो आगमोदय समिति के प्रभाव से प्रचलित जान पड़ता है।
ऐसे अन्य भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जो यह दिखाते है कि आगमोदय समिति के पाठों के अविचारित अनुकरण से विकृत पाठों का कितना विस्तार हुआ है। इतना ही नहीं, श्रीसागरानंदसूरिजीने अनेक स्थानों पर सूत्रपाठों को (व टीकापाठों को) कम कर दिया है या बढ़ा दिया है या सुधार दिया है, इस विषय में मुनि श्रीपुण्यविजयजी ने लिखा है कि यदि वे उन स्थानों पर कोई कोष्ठक या निशान कर देते तो भविष्य के संशोधक विद्वानों के लिए वह विशेष अनुकूल रहता ।
उपर्युक्त लेखन का उद्देश्य किसी भी प्रकार से श्रीसागरानन्दसूरिजी की टीका-टिप्पणी करना नहीं है अपितु मात्र यह सूचित करना है कि प्रचलित पाठों में किस-किस कारण से बदलाव आया है। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पश्चाद्वर्ती आगमकार्यों में सर्वांशतः उनका अनुकरण हुआ ही है अथवा उनके पाठों में सर्वत्र अशुद्धियाँ ही रही हैं। बल्कि उनके विषय में मुनि श्रीपुण्यविजयजी ने यह भी कहा कि जिस वेग से उनका आगमकार्य हुआ, उसे देखते हुए उनमें अपेक्षाकृत कम ही त्रुटिया रही हैं। संभव है उन्होंने पाठनिर्णय में विभिन्न कुल वाली अनेक हस्तलिखित प्रतियों को आधार बनाकर विचारपूर्वक पाठ निर्णय न किया हो तथा किन्हीं एक-दो अशुद्ध प्रतियों का आधार बनाकर स्वमत्यनुसार संशोधनादि करके उन्हें प्रकाशित कर दिया हो ।
(४) लिपिदोष का प्रभाव :
सूत्रप्रतियों की अशद्धता भी पाठभेद का एक बहुत बड़ा कारण बनी है। लेखन के साथ अशुद्धि का दामन-चोली जैसा सम्बन्ध कहा जाय तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी । अत्यन्त सावधान व जागरूक लेखकों द्वारा भी लेखनकार्य में त्रुटि होना प्राय: अपरिहार्य बन जाता है, यह वर्तमान के प्रत्यक्ष अनुभव से भी सिद्ध है ही । प्रतियों की अशुद्धता की समस्या प्राचीन टीकाकारों के समक्ष भी व्याघ्री के समान मुंह बाये खड़ी थी जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं ने किया है । यथा -
"अज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं, प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि (श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र-वृत्ति - श्रीअभयदेवसूरि) हम अल्पज्ञ हैं, यह शास्त्र गहन है और इसकी पुस्तकें (सूत्रप्रतियाँ) प्रायः अशुद्ध हैं।"
"यस्य ग्रन्थवरस्य वाक्यजलंधेर्लक्षं सहस्राणि च, चत्वारिंशदहो! चतुर्भिरधिकं मानं पदानामभूत् । तस्योच्चैश्चलुकाकृति विदधत: कालादिदोषात् तथा, दुर्लेखात् खिलतां गतस्य कुधियः कुर्वन्ति किं मादृशाः ॥
(श्रीसमवायाङ्गसूत्र-वृत्ति - श्रीअभयदेवसूरि) जिस वाक्यसमुद्र स्वरूप श्रेष्ठ ग्रन्थ (श्रीसमवायाङ्गसूत्र) का प्रमाण एक लाख चौवालीस हजार पदों का था, काल आदि के दोष से बिना जोती हुई भूमि जैसी अवस्था को प्राप्त उस ग्रन्थ पर एक चुल्लु भर जल स्वरूप कृति (टीका) की रचना करते हुए मेरे जैसे दुर्बुद्धि क्या कर पा रहे हैं ?"
"वाचनानामनेकत्वात् पुस्तकानामशुद्धितः । सूत्राणामतिगाम्भीर्यान्मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥ झूणानि सम्भवन्तीह केवलं सुविवेकिभिः । सिद्धान्तानुगतो योऽर्थः सोऽस्माद् ग्राह्यो न चेतरः ॥
(श्रीस्थानाङ्गसूत्रवृत्ति - श्रीअभयदेवसूरि)
* वस्तुत: इस श्लोक का ऐसा अर्थ होना चाहिए -
"जिस वाक्यसमुद्र तुल्य श्रेष्ठ ग्रन्थ का प्रमाण एक लाख चौवालीस हजार पदों का था, वह आज कालादि के दोष से चुल्लूभर शेष रह गया है (अर्थात् उसका छोटा सा अंश ही आज बचा है), और वह भी दुलेखन के कारण कूट अवस्था को प्राण कर चूका है तो इसमें मेरे जैसे मन्दबुद्धि लोग क्या करें?"-सं.।