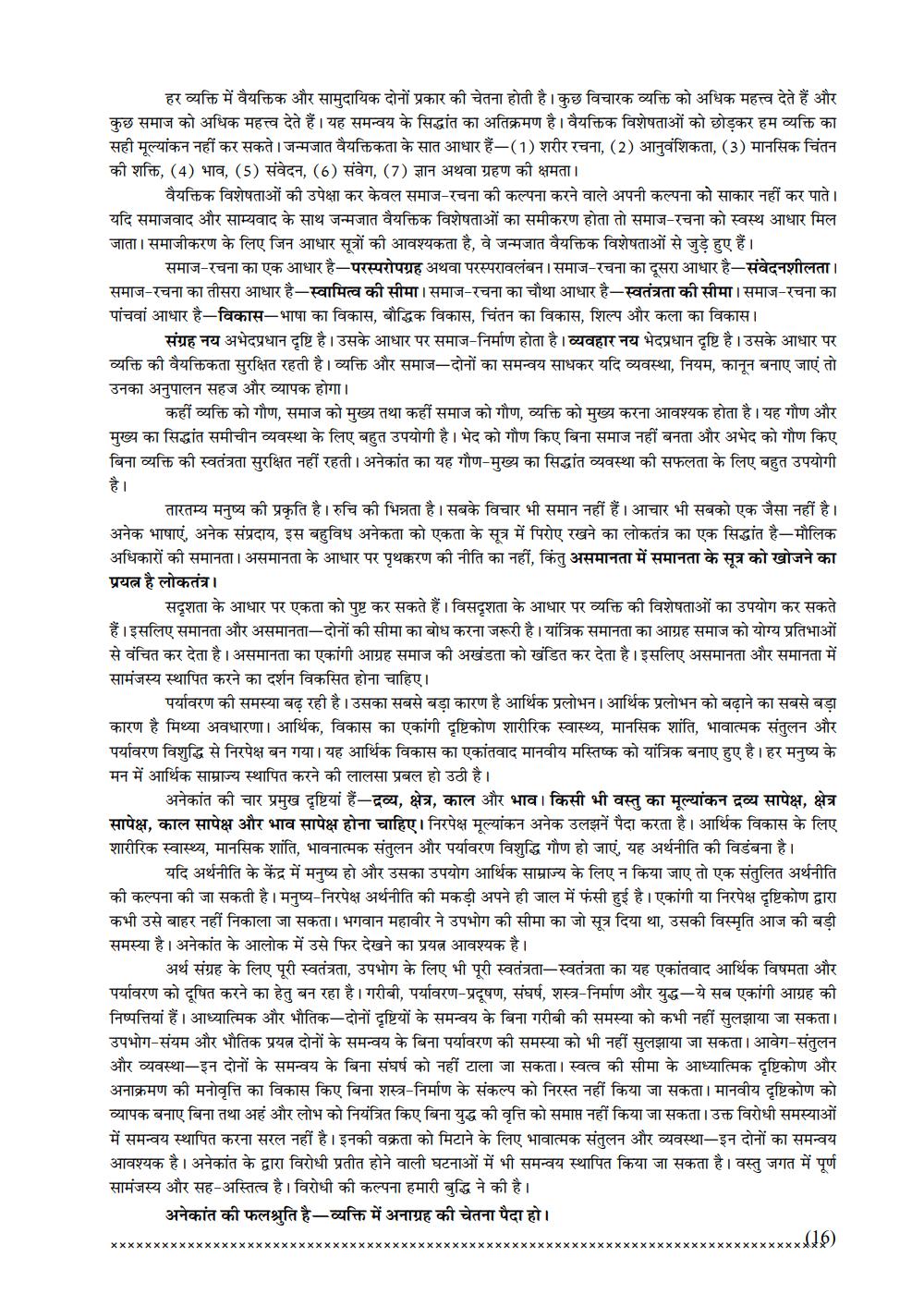________________ हर व्यक्ति में वैयक्तिक और सामुदायिक दोनों प्रकार की चेतना होती है। कुछ विचारक व्यक्ति को अधिक महत्त्व देते हैं और कुछ समाज को अधिक महत्त्व देते हैं। यह समन्वय के सिद्धांत का अतिक्रमण है। वैयक्तिक विशेषताओं को छोड़कर हम व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। जन्मजात वैयक्तिकता के सात आधार हैं-(1) शरीर रचना, (2) आनुवंशिकता, (3) मानसिक चिंतन की शक्ति, (4) भाव, (5) संवेदन, (6) संवेग, (7) ज्ञान अथवा ग्रहण की क्षमता। वैयक्तिक विशेषताओं की उपेक्षा कर केवल समाज-रचना की कल्पना करने वाले अपनी कल्पना को साकार नहीं कर पाते। यदि समाजवाद और साम्यवाद के साथ जन्मजात वैयक्तिक विशेषताओं का समीकरण होता तो समाज-रचना को स्वस्थ आधार मिल जाता। समाजीकरण के लिए जिन आधार सूत्रों की आवश्यकता है, वे जन्मजात वैयक्तिक विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। समाज-रचना का एक आधार है-परस्परोपग्रह अथवा परस्परावलंबन / समाज-रचना का दूसरा आधार है-संवेदनशीलता। समाज-रचना का तीसरा आधार है-स्वामित्व की सीमा। समाज-रचना का चौथा आधार है-स्वतंत्रता की सीमा। समाज-रचना का पांचवां आधार है-विकास-भाषा का विकास, बौद्धिक विकास, चिंतन का विकास, शिल्प और कला का विकास। ___ संग्रह नय अभेदप्रधान दृष्टि है। उसके आधार पर समाज-निर्माण होता है / व्यवहार नय भेदप्रधान दृष्टि है। उसके आधार पर व्यक्ति की वैयक्तिकता सुरक्षित रहती है। व्यक्ति और समाज-दोनों का समन्वय साधकर यदि व्यवस्था, नियम, कानून बनाए जाएं तो उनका अनुपालन सहज और व्यापक होगा। कहीं व्यक्ति को गौण, समाज को मुख्य तथा कहीं समाज को गौण, व्यक्ति को मुख्य करना आवश्यक होता है। यह गौण और मुख्य का सिद्धांत समीचीन व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। भेद को गौण किए बिना समाज नहीं बनता और अभेद को गौण किए बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। अनेकांत का यह गौण-मुख्य का सिद्धांत व्यवस्था की सफलता के लिए बहुत उपयोगी तारतम्य मनुष्य की प्रकृति है। रुचि की भिन्नता है। सबके विचार भी समान नहीं हैं। आचार भी सबको एक जैसा नहीं है। अनेक भाषाएं, अनेक संप्रदाय, इस बहुविध अनेकता को एकता के सूत्र में पिरोए रखने का लोकतंत्र का एक सिद्धांत है-मौलिक अधिकारों की समानता। असमानता के आधार पर पृथक्करण की नीति का नहीं, किंतु असमानता में समानता के सूत्र को खोजने का प्रयत्न है लोकतंत्र। सदृशता के आधार पर एकता को पुष्ट कर सकते हैं। विसदृशता के आधार पर व्यक्ति की विशेषताओं का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए समानता और असमानता–दोनों की सीमा का बोध करना जरूरी है। यांत्रिक समानता का आग्रह समाज को योग्य प्रतिभाओं से वंचित कर देता है। असमानता का एकांगी आग्रह समाज की अखंडता को खंडित कर देता है। इसलिए असमानता और समानता में सामंजस्य स्थापित करने का दर्शन विकसित होना चाहिए। पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक प्रलोभन / आर्थिक प्रलोभन को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है मिथ्या अवधारणा। आर्थिक, विकास का एकांगी दृष्टिकोण शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावात्मक संतुलन और पर्यावरण विशद्धि से निरपेक्ष बन गया। यह आर्थिक विकास का एकांतवाद मानवीय मस्तिष्क को यांत्रिक बनाए हुए है। हर मनुष्य के मन में आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने की लालसा प्रबल हो उठी है। अनेकांत की चार प्रमुख दृष्टियां हैं-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी भी वस्तु का मूल्यांकन द्रव्य सापेक्ष, क्षेत्र सापेक्ष, काल सापेक्ष और भाव सापेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष मूल्यांकन अनेक उलझनें पैदा करता है। आर्थिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और पर्यावरण विशुद्धि गौण हो जाएं, यह अर्थनीति की विडंबना है। यदि अर्थनीति के केंद्र में मनुष्य हो और उसका उपयोग आर्थिक साम्राज्य के लिए न किया जाए तो एक संतुलित अर्थनीति की कल्पना की जा सकती है। मनुष्य-निरपेक्ष अर्थनीति की मकड़ी अपने ही जाल में फंसी हुई है। एकांगी या निरपेक्ष दृष्टिकोण द्वारा कभी उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। भगवान महावीर ने उपभोग की सीमा का जो सूत्र दिया था, उसकी विस्मृति आज की बड़ी समस्या है। अनेकांत के आलोक में उसे फिर देखने का प्रयत्न आवश्यक है। __अर्थ संग्रह के लिए पूरी स्वतंत्रता, उपभोग के लिए भी पूरी स्वतंत्रता-स्वतंत्रता का यह एकांतवाद आर्थिक विषमता और पर्यावरण को दूषित करने का हेतु बन रहा है। गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, संघर्ष, शस्त्र-निर्माण और युद्ध-ये सब एकांगी आग्रह की निष्पत्तियां हैं। आध्यात्मिक और भौतिक-दोनों दृष्टियों के समन्वय के बिना गरीबी की समस्या को कभी नहीं सुलझाया जा सकता। उपभोग-संयम और भौतिक प्रयत्न दोनों के समन्वय के बिना पर्यावरण की समस्या को भी नहीं सुलझाया जा सकता। आवेग-संतुलन और व्यवस्था-इन दोनों के समन्वय के बिना संघर्ष को नहीं टाला जा सकता। स्वत्व की सीमा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनाक्रमण की मनोवृत्ति का विकास किए बिना शस्त्र-निर्माण के संकल्प को निरस्त नहीं किया जा सकता। मानवीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाए बिना तथा अहं और लोभ को नियंत्रित किए बिना युद्ध की वृत्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। उक्त विरोधी समस्याओं में समन्वय स्थापित करना सरल नहीं है। इनकी वक्रता को मिटाने के लिए भावात्मक संतुलन और व्यवस्था-इन दोनों का समन्वय आवश्यक है। अनेकांत के द्वारा विरोधी प्रतीत होने वाली घटनाओं में भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। वस्तु जगत में पूर्ण सामंजस्य और सह-अस्तित्व है। विरोधी की कल्पना हमारी बुद्धि ने की है। अनेकांत की फलश्रुति है-व्यक्ति में अनाग्रह की चेतना पैदा हो। xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> xxxxxx (16)