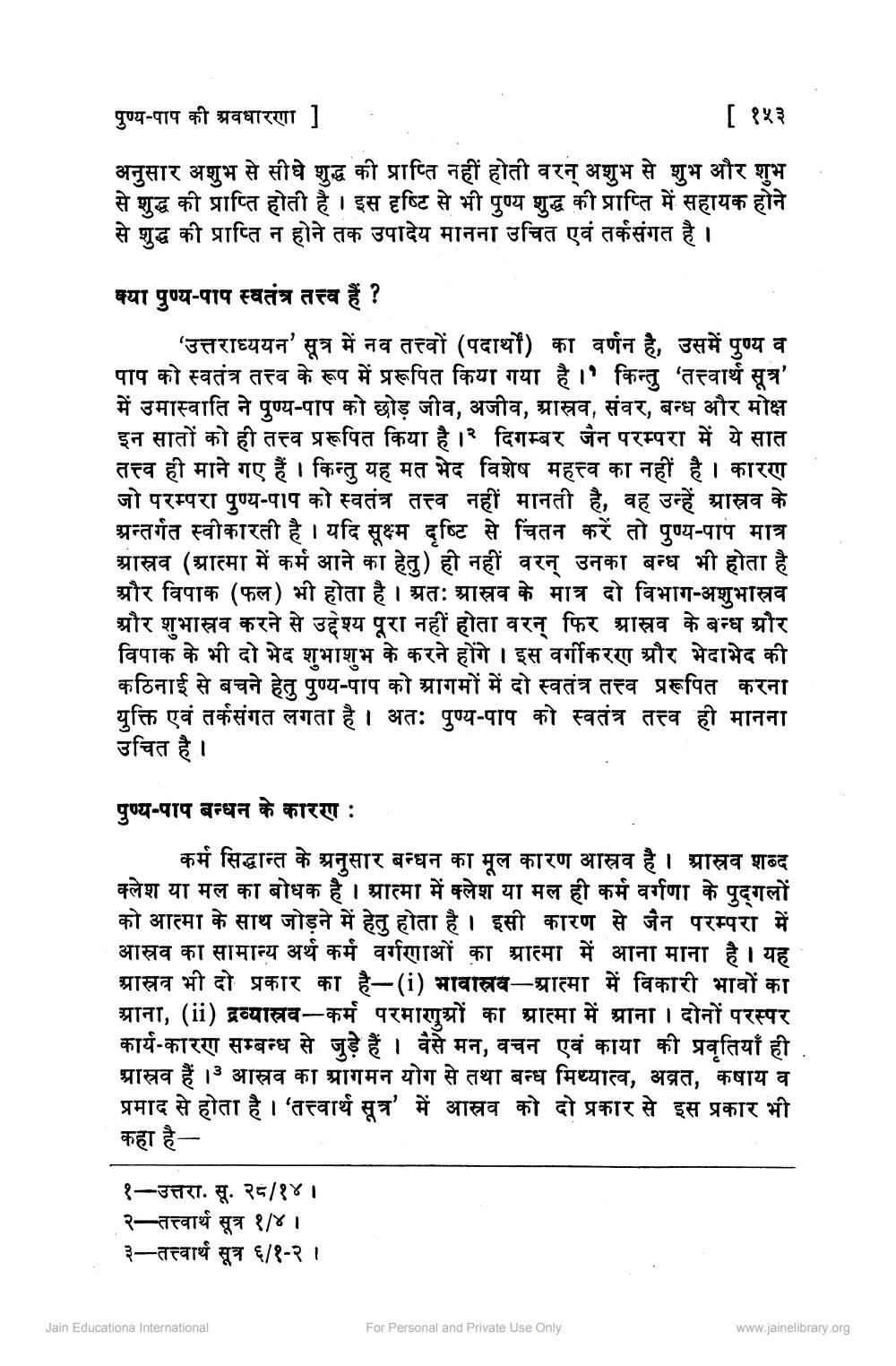________________
पुण्य-पाप की अवधारणा ] .
[ १५३ अनुसार अशुभ से सीधे शुद्ध की प्राप्ति नहीं होती वरन् अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की प्राप्ति होती है । इस दृष्टि से भी पुण्य शुद्ध की प्राप्ति में सहायक होने से शुद्ध की प्राप्ति न होने तक उपादेय मानना उचित एवं तर्कसंगत है।
क्या पुण्य-पाप स्वतंत्र तत्त्व हैं ?
'उत्तराध्ययन' सूत्र में नव तत्त्वों (पदार्थों) का वर्णन है, उसमें पुण्य व पाप को स्वतंत्र तत्त्व के रूप में प्ररूपित किया गया है। किन्तु 'तत्त्वार्थ सूत्र' में उमास्वाति ने पुण्य-पाप को छोड़ जीव, अजीव, आस्रव, संवर, बन्ध और मोक्ष इन सातों को ही तत्त्व प्ररूपित किया है ।२ दिगम्बर जैन परम्परा में ये सात तत्त्व ही माने गए हैं। किन्तु यह मत भेद विशेष महत्त्व का नहीं है। कारण जो परम्परा पुण्य-पाप को स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानती है, वह उन्हें आस्रव के अन्तर्गत स्वीकारती है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करें तो पुण्य-पाप मात्र आस्रव (आत्मा में कर्म आने का हेतु) ही नहीं वरन् उनका बन्ध भी होता है और विपाक (फल) भी होता है । अतः आस्रव के मात्र दो विभाग-अशुभास्रव और शुभास्रव करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता वरन् फिर प्रास्रव के बन्ध और विपाक के भी दो भेद शुभाशुभ के करने होंगे। इस वर्गीकरण और भेदाभेद की कठिनाई से बचने हेतु पुण्य-पाप को आगमों में दो स्वतंत्र तत्त्व प्ररूपित करना युक्ति एवं तर्कसंगत लगता है। अतः पुण्य-पाप को स्वतंत्र तत्त्व ही मानना उचित है।
पुण्य-पाप बन्धन के कारण :
कर्म सिद्धान्त के अनुसार बन्धन का मूल कारण आस्रव है। आस्रव शब्द क्लेश या मल का बोधक है । आत्मा में क्लेश या मल ही कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा के साथ जोड़ने में हेतु होता है। इसी कारण से जैन परम्परा में आस्रव का सामान्य अर्थ कर्म वर्गणाओं का आत्मा में आना माना है। यह आस्रव भी दो प्रकार का है-(i) भावानव-आत्मा में विकारी भावों का आना, (i) द्रव्यानव-कर्म परमाणुओं का प्रात्मा में आना । दोनों परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध से जुड़े हैं । वैसे मन, वचन एवं काया की प्रवृतियाँ ही . प्रास्रव हैं । आस्रव का आगमन योग से तथा बन्ध मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय व प्रमाद से होता है । 'तत्त्वार्थ सूत्र' में आस्रव को दो प्रकार से इस प्रकार भी कहा है
१-उत्तरा. सू. २८/१४ । २-तत्त्वार्थ सूत्र १/४ । ३-तत्त्वार्थ सूत्र ६/१-२ ।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org