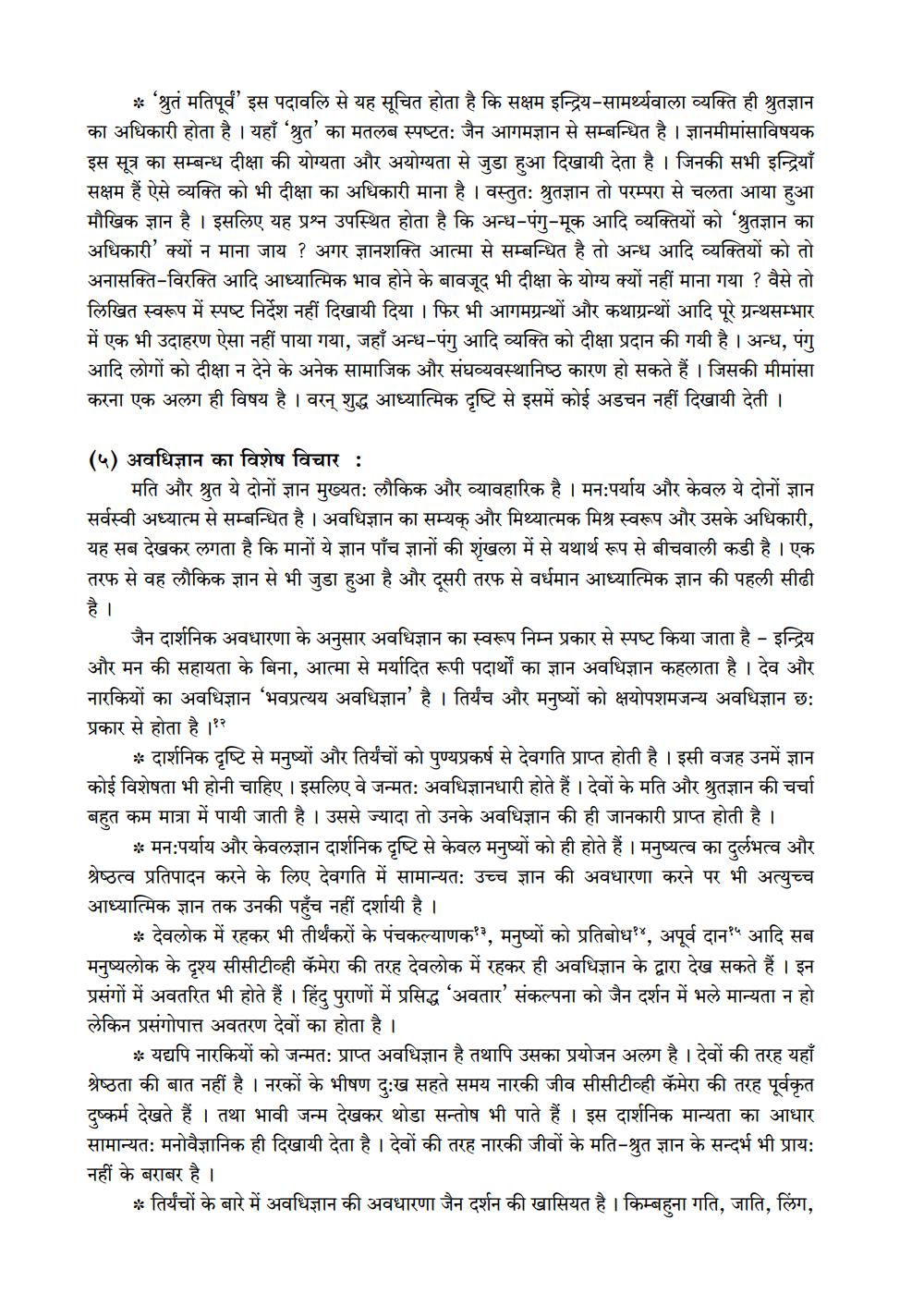________________
* 'श्रुतं मतिपूर्वं' इस पदावलि से यह सूचित होता है कि सक्षम इन्द्रिय-सामर्थ्यवाला व्यक्ति ही श्रुतज्ञान का अधिकारी होता है । यहाँ श्रुत' का मतलब स्पष्टत: जैन आगमज्ञान से सम्बन्धित है । ज्ञानमीमांसाविषयक इस सूत्र का सम्बन्ध दीक्षा की योग्यता और अयोग्यता से जुड़ा हुआ दिखायी देता है । जिनकी सभी इन्द्रियाँ सक्षम हैं ऐसे व्यक्ति को भी दीक्षा का अधिकारी माना है । वस्तुतः श्रुतज्ञान तो परम्परा से चलता आया हुआ मौखिक ज्ञान है । इसलिए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अन्ध-पंगु-मूक आदि व्यक्तियों को 'श्रुतज्ञान का अधिकारी' क्यों न माना जाय ? अगर ज्ञानशक्ति आत्मा से सम्बन्धित है तो अन्ध आदि व्यक्तियों को तो अनासक्ति-विरक्ति आदि आध्यात्मिक भाव होने के बावजूद भी दीक्षा के योग्य क्यों नहीं माना गया ? वैसे तो लिखित स्वरूप में स्पष्ट निर्देश नहीं दिखायी दिया । फिर भी आगमग्रन्थों और कथाग्रन्थों आदि पूरे ग्रन्थसम्भार में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पाया गया, जहाँ अन्ध-पंगु आदि व्यक्ति को दीक्षा प्रदान की गयी है । अन्ध, पंगु आदि लोगों को दीक्षा न देने के अनेक सामाजिक और संघव्यवस्थानिष्ठ कारण हो सकते हैं । जिसकी मीमांसा करना एक अलग ही विषय है । वरन् शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें कोई अडचन नहीं दिखायी देती ।
(५) अवधिज्ञान का विशेष विचार :
मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान मुख्यत: लौकिक और व्यावहारिक है । मन:पर्याय और केवल ये दोनों ज्ञान सर्वस्वी अध्यात्म से सम्बन्धित है । अवधिज्ञान का सम्यक् और मिथ्यात्मक मिश्र स्वरूप और उसके अधिकारी, यह सब देखकर लगता है कि मानों ये ज्ञान पाँच ज्ञानों की शृंखला में से यथार्थ रूप से बीचवाली कडी है । एक तरफ से वह लौकिक ज्ञान से भी जुडा हुआ है और दूसरी तरफ से वर्धमान आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढी
जैन दार्शनिक अवधारणा के अनुसार अवधिज्ञान का स्वरूप निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है - इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, आत्मा से मर्यादित रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है । देव और नारकियों का अवधिज्ञान ‘भवप्रत्यय अवधिज्ञान' है । तिर्यंच और मनुष्यों को क्षयोपशमजन्य अवधिज्ञान छ: प्रकार से होता है ।१२
* दार्शनिक दृष्टि से मनुष्यों और तिर्यंचों को पुण्यप्रकर्ष से देवगति प्राप्त होती है । इसी वजह उनमें ज्ञान कोई विशेषता भी होनी चाहिए । इसलिए वे जन्मतः अवधिज्ञानधारी होते हैं । देवों के मति और श्रुतज्ञान की चर्चा बहुत कम मात्रा में पायी जाती है । उससे ज्यादा तो उनके अवधिज्ञान की ही जानकारी प्राप्त होती है।
* मन:पर्याय और केवलज्ञान दार्शनिक दृष्टि से केवल मनुष्यों को ही होते हैं । मनुष्यत्व का दुर्लभत्व और श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने के लिए देवगति में सामान्यत: उच्च ज्ञान की अवधारणा करने पर भी अत्युच्च आध्यात्मिक ज्ञान तक उनकी पहुँच नहीं दर्शायी है ।
* देवलोक में रहकर भी तीर्थंकरों के पंचकल्याणक ३, मनुष्यों को प्रतिबोध, अपूर्व दान'५ आदि सब मनुष्यलोक के दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरा की तरह देवलोक में रहकर ही अवधिज्ञान के द्वारा देख सकते हैं । इन प्रसंगों में अवतरित भी होते हैं । हिंदु पुराणों में प्रसिद्ध 'अवतार' संकल्पना को जैन दर्शन में भले मान्यता न हो लेकिन प्रसंगोपात्त अवतरण देवों का होता है।
* यद्यपि नारकियों को जन्मत: प्राप्त अवधिज्ञान है तथापि उसका प्रयोजन अलग है। देवों की तरह यहाँ श्रेष्ठता की बात नहीं है । नरकों के भीषण दुःख सहते समय नारकी जीव सीसीटीव्ही कॅमेरा की तरह पूर्वकृत दष्कर्म देखते हैं । तथा भावी जन्म देखकर थोडा सन्तोष भी पाते हैं । इस दार्शनिक मान्यता का आधार सामान्यत: मनोवैज्ञानिक ही दिखायी देता है । देवों की तरह नारकी जीवों के मति-श्रुत ज्ञान के सन्दर्भ भी प्रायः नहीं के बराबर है।
* तिर्यंचों के बारे में अवधिज्ञान की अवधारणा जैन दर्शन की खासियत है । किम्बहुना गति, जाति, लिंग,