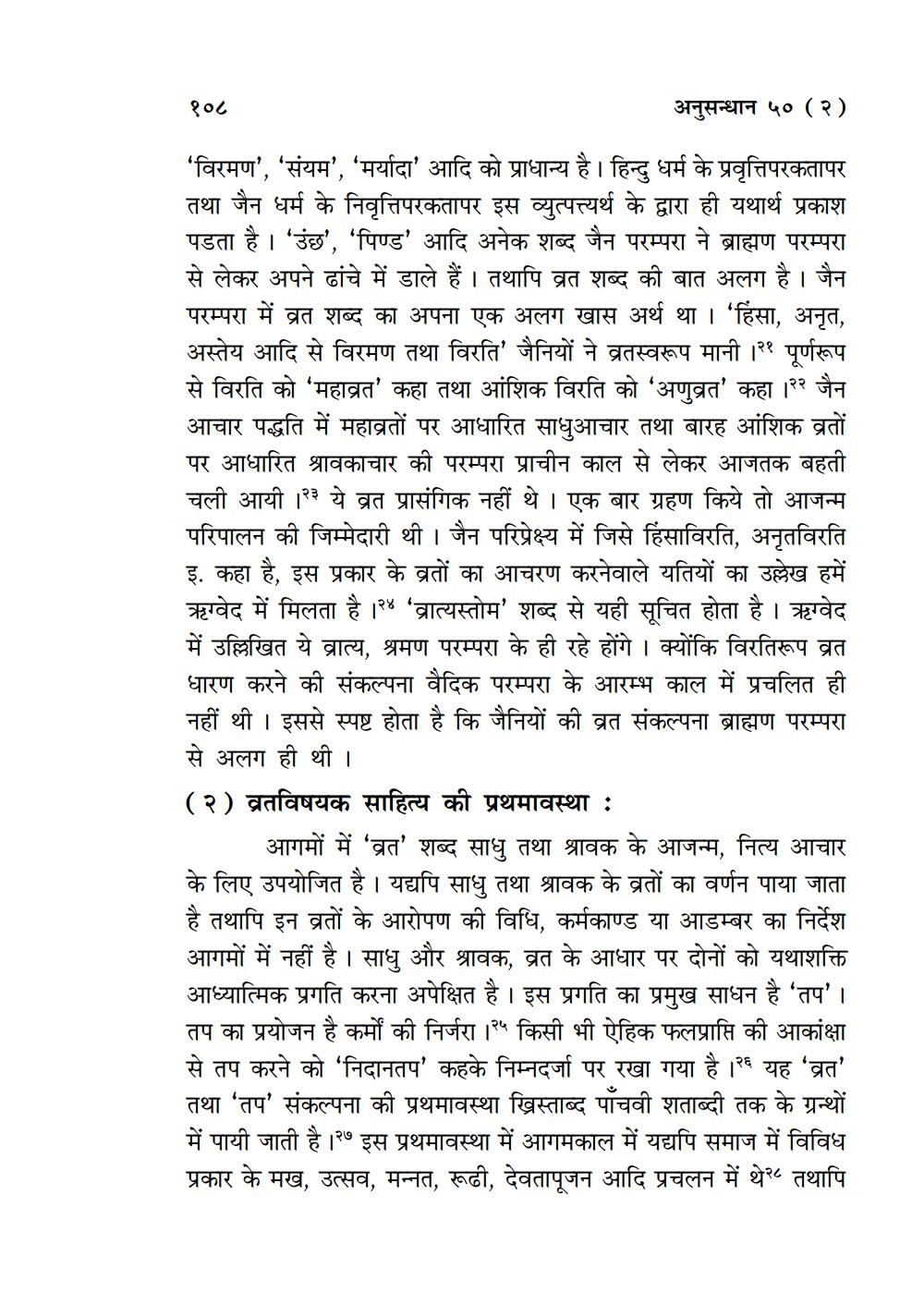________________
१०८
अनुसन्धान ५० (२)
'विरमण', 'संयम', 'मर्यादा' आदि को प्राधान्य है। हिन्दु धर्म के प्रवृत्तिपरकतापर तथा जैन धर्म के निवृत्तिपरकतापर इस व्युत्पत्त्यर्थ के द्वारा ही यथार्थ प्रकाश पडता है । 'उंछ', 'पिण्ड' आदि अनेक शब्द जैन परम्परा ने ब्राह्मण परम्परा से लेकर अपने ढांचे में डाले हैं। तथापि व्रत शब्द की बात अलग है। जैन परम्परा में व्रत शब्द का अपना एक अलग खास अर्थ था । 'हिंसा, अनृत, अस्तेय आदि से विरमण तथा विरति' जैनियों ने व्रतस्वरूप मानी ।२१ पूर्णरूप से विरति को 'महाव्रत' कहा तथा आंशिक विरति को 'अणुव्रत' कहा ।२२ जैन आचार पद्धति में महाव्रतों पर आधारित साधुआचार तथा बारह आंशिक व्रतों पर आधारित श्रावकाचार की परम्परा प्राचीन काल से लेकर आजतक बहती चली आयी ।२३ ये व्रत प्रासंगिक नहीं थे। एक बार ग्रहण किये तो आजन्म परिपालन की जिम्मेदारी थी। जैन परिप्रेक्ष्य में जिसे हिंसाविरति, अनृतविरति इ. कहा है, इस प्रकार के व्रतों का आचरण करनेवाले यतियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है ।२४ 'व्रात्यस्तोम' शब्द से यही सूचित होता है । ऋग्वेद में उल्लिखित ये व्रात्य, श्रमण परम्परा के ही रहे होंगे। क्योंकि विरतिरूप व्रत धारण करने की संकल्पना वैदिक परम्परा के आरम्भ काल में प्रचलित ही नहीं थी । इससे स्पष्ट होता है कि जैनियों की व्रत संकल्पना ब्राह्मण परम्परा से अलग ही थी। (२) व्रतविषयक साहित्य की प्रथमावस्था :
आगमों में 'व्रत' शब्द साधु तथा श्रावक के आजन्म, नित्य आचार के लिए उपयोजित है । यद्यपि साधु तथा श्रावक के व्रतों का वर्णन पाया जाता है तथापि इन व्रतों के आरोपण की विधि, कर्मकाण्ड या आडम्बर का निर्देश आगमों में नहीं है। साधु और श्रावक, व्रत के आधार पर दोनों को यथाशक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना अपेक्षित है । इस प्रगति का प्रमुख साधन है 'तप' । तप का प्रयोजन है कर्मों की निर्जरा ।२५ किसी भी ऐहिक फलप्राप्ति की आकांक्षा से तप करने को 'निदानतप' कहके निम्नदर्जा पर रखा गया है ।२६ यह 'व्रत' तथा 'तप' संकल्पना की प्रथमावस्था ख्रिस्ताब्द पाचवी शताब्दी तक के ग्रन्थों में पायी जाती है । इस प्रथमावस्था में आगमकाल में यद्यपि समाज में विविध प्रकार के मख, उत्सव, मन्नत, रूढी, देवतापूजन आदि प्रचलन में थे२८ तथापि