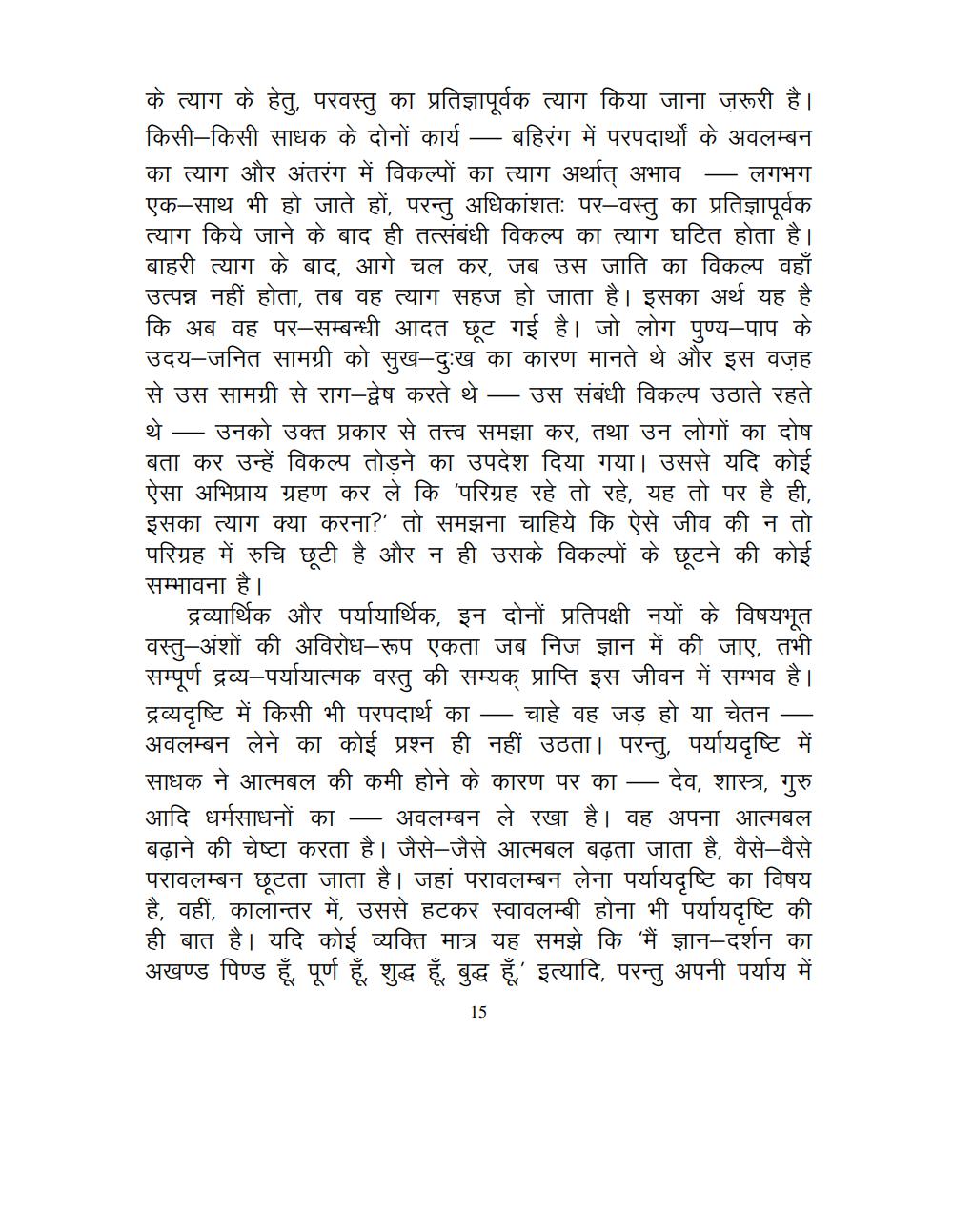________________
के त्याग के हेतु, परवस्तु का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग किया जाना जरूरी है। किसी-किसी साधक के दोनों कार्य — बहिरंग में परपदार्थों के अवलम्बन का त्याग और अंतरंग में विकल्पों का त्याग अर्थात् अभाव – लगभग एक-साथ भी हो जाते हों, परन्तु अधिकांशतः पर-वस्तु का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग किये जाने के बाद ही तत्संबंधी विकल्प का त्याग घटित होता है। बाहरी त्याग के बाद, आगे चल कर, जब उस जाति का विकल्प वहाँ उत्पन्न नहीं होता, तब वह त्याग सहज हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब वह पर-सम्बन्धी आदत छट गई है। जो लोग पण्य-पाप के उदय-जनित सामग्री को सुख-दुःख का कारण मानते थे और इस वजह से उस सामग्री से राग-द्वेष करते थे – उस संबंधी विकल्प उठाते रहते थे – उनको उक्त प्रकार से तत्त्व समझा कर, तथा उन लोगों का दोष बता कर उन्हें विकल्प तोड़ने का उपदेश दिया गया। उससे यदि कोई ऐसा अभिप्राय ग्रहण कर ले कि 'परिग्रह रहे तो रहे, यह तो पर है ही, इसका त्याग क्या करना?' तो समझना चाहिये कि ऐसे जीव की न तो परिग्रह में रुचि छूटी है और न ही उसके विकल्पों के छूटने की कोई सम्भावना है।
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों प्रतिपक्षी नयों के विषयभूत वस्तु-अंशों की अविरोध-रूप एकता जब निज ज्ञान में की जाए, तभी सम्पूर्ण द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु की सम्यक् प्राप्ति इस जीवन में सम्भव है। द्रव्यदृष्टि में किसी भी परपदार्थ का – चाहे वह जड़ हो या चेतन - अवलम्बन लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु, पर्यायदृष्टि में साधक ने आत्मबल की कमी होने के कारण पर का - देव, शास्त्र, गुरु आदि धर्मसाधनों का – अवलम्बन ले रखा है। वह अपना आत्मबल बढ़ाने की चेष्टा करता है। जैसे-जैसे आत्मबल बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे परावलम्बन छूटता जाता है। जहां परावलम्बन लेना पर्यायदृष्टि का विषय है, वहीं, कालान्तर में, उससे हटकर स्वावलम्बी होना भी पर्यायदृष्टि की ही बात है। यदि कोई व्यक्ति मात्र यह समझे कि 'मैं ज्ञान-दर्शन का अखण्ड पिण्ड हूँ, पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, इत्यादि, परन्तु अपनी पर्याय में