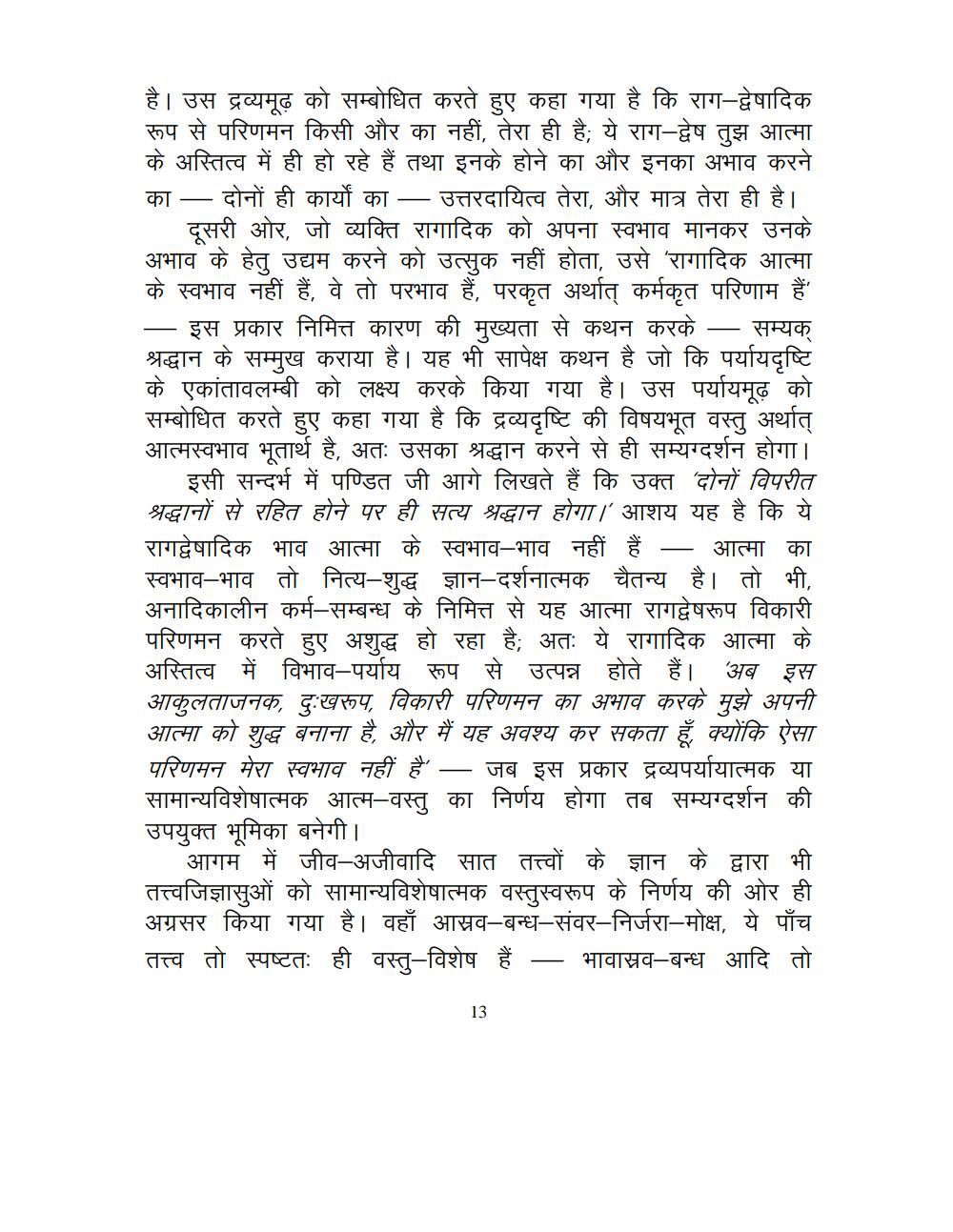________________
है। उस द्रव्यमूढ़ को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि राग-द्वेषादिक रूप से परिणमन किसी और का नहीं, तेरा ही है; ये राग-द्वेष तुझ आत्मा के अस्तित्व में ही हो रहे हैं तथा इनके होने का और इनका अभाव करने का – दोनों ही कार्यों का – उत्तरदायित्व तेरा, और मात्र तेरा ही है।
दूसरी ओर, जो व्यक्ति रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके अभाव के हेतु उद्यम करने को उत्सुक नहीं होता, उसे 'रागादिक आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, वे तो परभाव हैं, परकृत अर्थात् कर्मकृत परिणाम हैं। – इस प्रकार निमित्त कारण की मुख्यता से कथन करके – सम्यक् श्रद्धान के सम्मख कराया है। यह भी सापेक्ष कथन है जो कि पर्यायदष्टि के एकांतावलम्बी को लक्ष्य करके किया गया है। उस पर्यायमूढ़ को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि द्रव्यदृष्टि की विषयभूत वस्तु अर्थात् आत्मस्वभाव भूतार्थ है, अत: उसका श्रद्धान करने से ही सम्यग्दर्शन होगा।
इसी सन्दर्भ में पण्डित जी आगे लिखते हैं कि उक्त दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर ही सत्य श्रद्धान होगा।' आशय यह है कि ये रागद्वेषादिक भाव आत्मा के स्वभाव-भाव नहीं हैं - आत्मा का स्वभाव-भाव तो नित्य-शुद्ध ज्ञान-दर्शनात्मक चैतन्य है। तो भी, अनादिकालीन कर्म-सम्बन्ध के निमित्त से यह आत्मा रागद्वेषरूप विकारी परिणमन करते हुए अशुद्ध हो रहा है; अतः ये रागादिक आत्मा के अस्तित्व में विभाव-पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। अब इस आकुलताजनक, दुःखरूप, विकारी परिणमन का अभाव करके मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, और मैं यह अवश्य कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा परिणमन मेरा स्वभाव नहीं है - जब इस प्रकार द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्यविशेषात्मक आत्म-वस्तु का निर्णय होगा तब सम्यग्दर्शन की उपयुक्त भूमिका बनेगी।
आगम में जीव-अजीवादि सात तत्त्वों के ज्ञान के द्वारा भी तत्त्वजिज्ञासुओं को सामान्यविशेषात्मक वस्तुस्वरूप के निर्णय की ओर ही अग्रसर किया गया है। वहाँ आस्रव-बन्ध-संवर-निर्जरा-मोक्ष, ये पाँच तत्त्व तो स्पष्टतः ही वस्तु-विशेष हैं – भावानव-बन्ध आदि तो