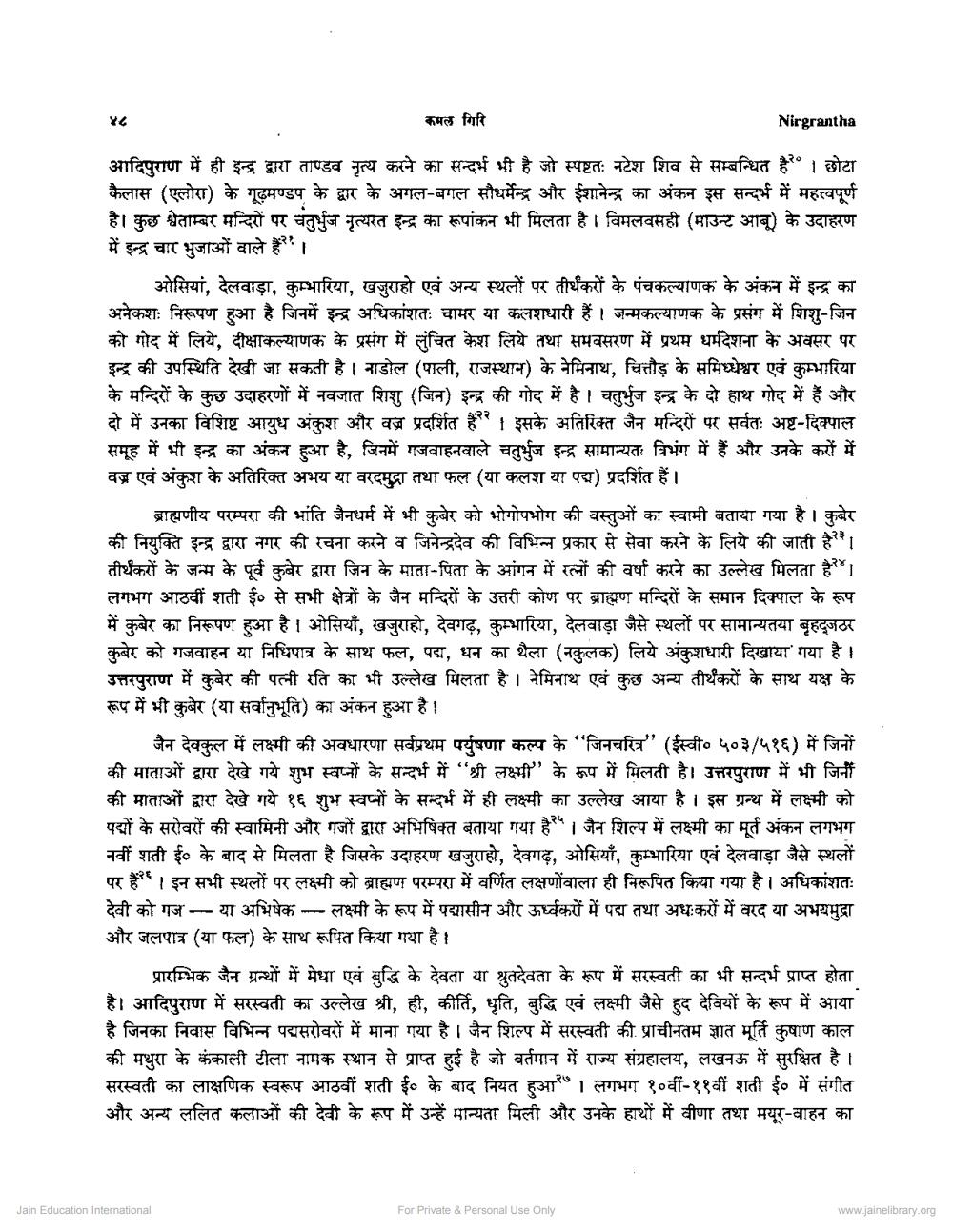________________
कमल गिरि
Nirgrantha
आदिपुराण में ही इन्द्र द्वारा ताण्डव नृत्य करने का सन्दर्भ भी है जो स्पष्टत: नटेश शिव से सम्बन्धित है । छोटा कैलास (एलोरा) के गूढमण्डप के द्वार के अगल-बगल सौधर्मेन्द्र और ईशानेन्द्र का अंकन इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है। कुछ श्वेताम्बर मन्दिरों पर चतुर्भुज नृत्यरत इन्द्र का रूपांकन भी मिलता है। विमलवसही (माउन्ट आबू) के उदाहरण में इन्द्र चार भुजाओं वाले हैं।
__ ओसियां, देलवाड़ा, कुम्भारिया, खजुराहो एवं अन्य स्थलों पर तीर्थंकरों के पंचकल्याणक के अंकन में इन्द्र का अनेकशः निरूपण हुआ है जिनमें इन्द्र अधिकांशतः चामर या कलशधारी हैं। जन्मकल्याणक के प्रसंग में शिशु-जिन को गोद में लिये, दीक्षाकल्याणक के प्रसंग में लुंचित केश लिये तथा समवसरण में प्रथम धर्मदेशना के अवसर पर इन्द्र की उपस्थिति देखी जा सकती है। नाडोल (पाली, राजस्थान) के नेमिनाथ, चित्तौड़ के समिध्धेश्वर एवं कुम्भारिया के मन्दिरों के कुछ उदाहरणों में नवजात शिशु (जिन) इन्द्र की गोद में है। चतुर्भुज इन्द्र के दो हाथ गोद में हैं और दो में उनका विशिष्ट आयुध अंकुश और वज्र प्रदर्शित हैं। इसके अतिरिक्त जैन मन्दिरों पर सर्वत: अष्ट-दिक्पाल समूह में भी इन्द्र का अंकन हुआ है, जिनमें गजवाहनवाले चतुर्भुज इन्द्र सामान्यतः त्रिभंग में हैं और उनके करों में वज्र एवं अंकुश के अतिरिक्त अभय या वरदमुद्रा तथा फल (या कलश या पद्य) प्रदर्शित हैं।
ब्राह्मणीय परम्परा की भांति जैनधर्म में भी कुबेर को भोगोपभोग की वस्तुओं का स्वामी बताया गया है। कुबेर की नियुक्ति इन्द्र द्वारा नगर की रचना करने व जिनेन्द्रदेव की विभिन्न प्रकार से सेवा करने के लिये की जाती है। तीर्थंकरों के जन्म के पूर्व कुबेर द्वारा जिन के माता-पिता के आंगन में रत्नों की वर्षा करने का उल्लेख मिलता है। लगभग आठवीं शती ई० से सभी क्षेत्रों के जैन मन्दिरों के उत्तरी कोण पर ब्राह्मण मन्दिरों के समान दिक्पाल के रूप में कुबेर का निरूपण हुआ है। ओसियाँ, खजुराहो, देवगढ़, कुम्भारिया, देलवाड़ा जैसे स्थलों पर सामान्यतया बृहद्जठर कुबेर को गजवाहन या निधिपात्र के साथ फल, पद्म, धन का थैला (नकुलक) लिये अंकुशधारी दिखाया गया है। उत्तरपुराण में कुबेर की पत्नी रति का भी उल्लेख मिलता है। नेमिनाथ एवं कुछ अन्य तीर्थंकरों के साथ यक्ष के रूप में भी कुबेर (या सर्वानुभूति) का अंकन हुआ है।
जैन देवकुल में लक्ष्मी की अवधारणा सर्वप्रथम पर्युषणा कल्प के "जिनचरित्र" (ईस्वी० ५०३/५१६) में जिनों की माताओं द्वारा देखे गये शुभ स्वप्नों के सन्दर्भ में "श्री लक्ष्मी" के रूप में मिलती है। उत्तरपुराण में भी जिनौं की माताओं द्वारा देखे गये १६ शुभ स्वप्नों के सन्दर्भ में ही लक्ष्मी का उल्लेख आया है। इस ग्रन्थ में लक्ष्मी को पद्मों के सरोवरों की स्वामिनी और गजों द्वारा अभिषिक्त बताया गया है। जैन शिल्प में लक्ष्मी का मूर्त अंकन लगभग नवीं शती ई० के बाद से मिलता है जिसके उदाहरण खजुराहो, देवगढ़, ओसियाँ, कुम्भारिया एवं देलवाड़ा जैसे स्थलों पर हैं । इन सभी स्थलों पर लक्ष्मी को ब्राह्मण परम्परा में वर्णित लक्षणोंवाला ही निरूपित किया गया है। अधिकांशतः देवी को गज-या अभिषेक - लक्ष्मी के रूप में पद्मासीन और ऊर्ध्वकरों में पद्म तथा अधःकरों में वरद या अभयमुद्रा और जलपात्र (या फल) के साथ रूपित किया गया है।
प्रारम्भिक जैन ग्रन्थों में मेधा एवं बुद्धि के देवता या श्रुतदेवता के रूप में सरस्वती का भी सन्दर्भ प्राप्त होता है। आदिपुराण में सरस्वती का उल्लेख श्री, ही, कीर्ति, धृति, बुद्धि एवं लक्ष्मी जैसे हुद देवियों के रूप में आया है जिनका निवास विभिन्न पद्मसरोवरों में माना गया है। जैन शिल्प में सरस्वती की प्राचीनतम ज्ञात मूर्ति कुषाण काल की मथुरा के कंकाली टीला नामक स्थान से प्राप्त हुई है जो वर्तमान में राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षित है। सरस्वती का लाक्षणिक स्वरूप आठवीं शती ई० के बाद नियत हुआ । लगभग १०वीं-११वीं शती ई० में संगीत और अन्य ललित कलाओं की देवी के रूप में उन्हें मान्यता मिली और उनके हाथों में वीणा तथा मयूर-वाहन का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org