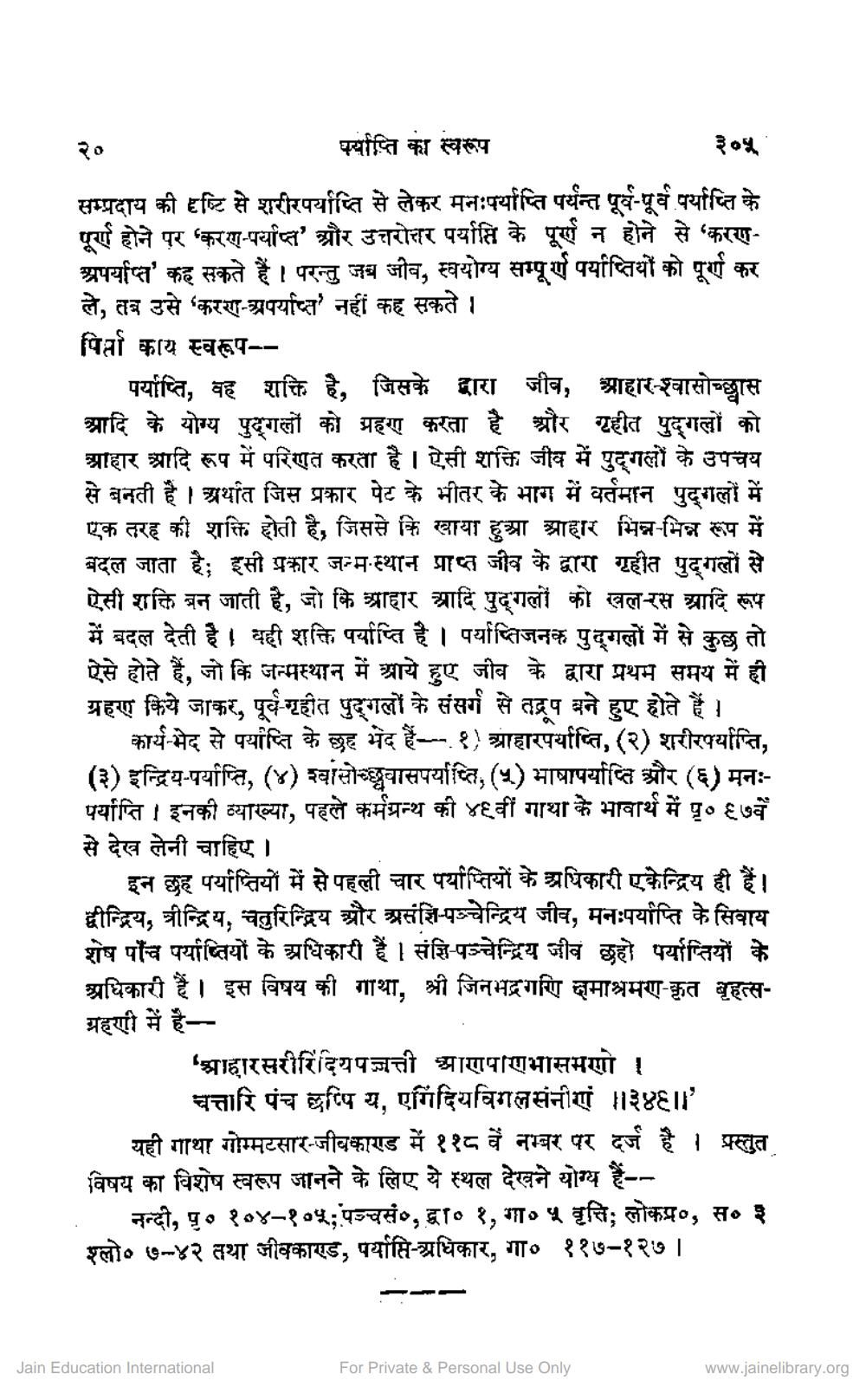________________
२०
पर्याप्ति का स्वरूप
३०५
सम्प्रदाय की दृष्टि से शरीर पर्याप्ति से लेकर मनःपर्याप्ति पर्यन्त पूर्व-पूर्व पर्याप्ति के पूर्ण होने पर 'करण- पर्याप्त' और उत्तरोत्तर पर्याप्ति के पूर्ण न होने से 'करणपर्याप्त' कह सकते हैं । परन्तु जब जीव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याप्तियों को पूर्ण कर ले, तब उसे 'करण-अपर्याप्त नहीं कह सकते ।
पिर्ता काय स्वरूप --
पर्याप्ति, वह शक्ति है, जिसके द्वारा जीव, आहार-श्वासोच्छ्वास आदि के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और गृहीत पुद्गलों को आहार आदि रूप में परिणत करता है । ऐसी शक्ति जीव में पुद्गलों के उपचय से बनती हैं । अर्थात जिस प्रकार पेट के भीतर के भाग में वर्तमान पुद्गलों में एक तरह की शक्ति होती है, जिससे कि खाया हुआ आहार भिन्न-भिन्न रूप में बदल जाता है; इसी प्रकार जन्म स्थान प्राप्त जीव के द्वारा गृहीत पुद्गलों से ऐसी शक्ति बन जाती है, जो कि आहार आदि पुद्गलों को खल-रस आदि रूप में बदल देती है । वही शक्ति पर्याप्ति है । पर्याप्तिजनक पुद्गलों में से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थान में आये हुए जीव के द्वारा प्रथम समय में ही ग्रहण किये जाकर, पूर्व-गृहीत पुद्गलों के संसर्ग से तद्रूप ब हुए होते हैं ।
कार्य-भेद से पर्याप्त के छह भेद हैं--- १) श्राहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय-पर्याप्ति, (४) श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति, (५) भाषापर्याप्ति और (६) मनःपर्याप्ति । इनकी व्याख्या, पहले कर्मग्रन्थ की ४९ वीं गाथा के भावार्थ में पृ० ६७ वें से देख लेनी चाहिए ।
इन छह पर्याप्तियों में से पहली चार पर्याप्तियों के अधिकारी एकेन्द्रिय ही हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और संज्ञि - पञ्चेन्द्रिय जीव, मनः पर्याप्ति के सिवाय शेष पाँच पर्याप्तियों के अधिकारी हैं। संशि- पञ्चेन्द्रिय जीव छहो पर्याप्तियों के अधिकारी हैं । इस विषय की गाथा, श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण- कृत बृहत्सग्रहणी में है
'श्राहारसरीरिदिय पज्जत्ती आणपाणभासमणो । चत्तारि पंच छप्पिय, एगिंदियविगलसंनीयं ||३४६॥'
यही गाथा गोम्मटसार-जीवकाण्ड में ११८ वें नम्बर पर दर्ज है । प्रस्तुत विषय का विशेष स्वरूप जानने के लिए ये स्थल देखने योग्य हैं-
नन्दी, पृ० १०४ - १०५ पञ्चसं०, द्वा० १, गा० ५ वृत्ति; लोकप्र०, स० ३ श्लो० ७-४२ तथा जीवकाएड, पर्याप्ति अधिकार, गा० ११७- १२७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org