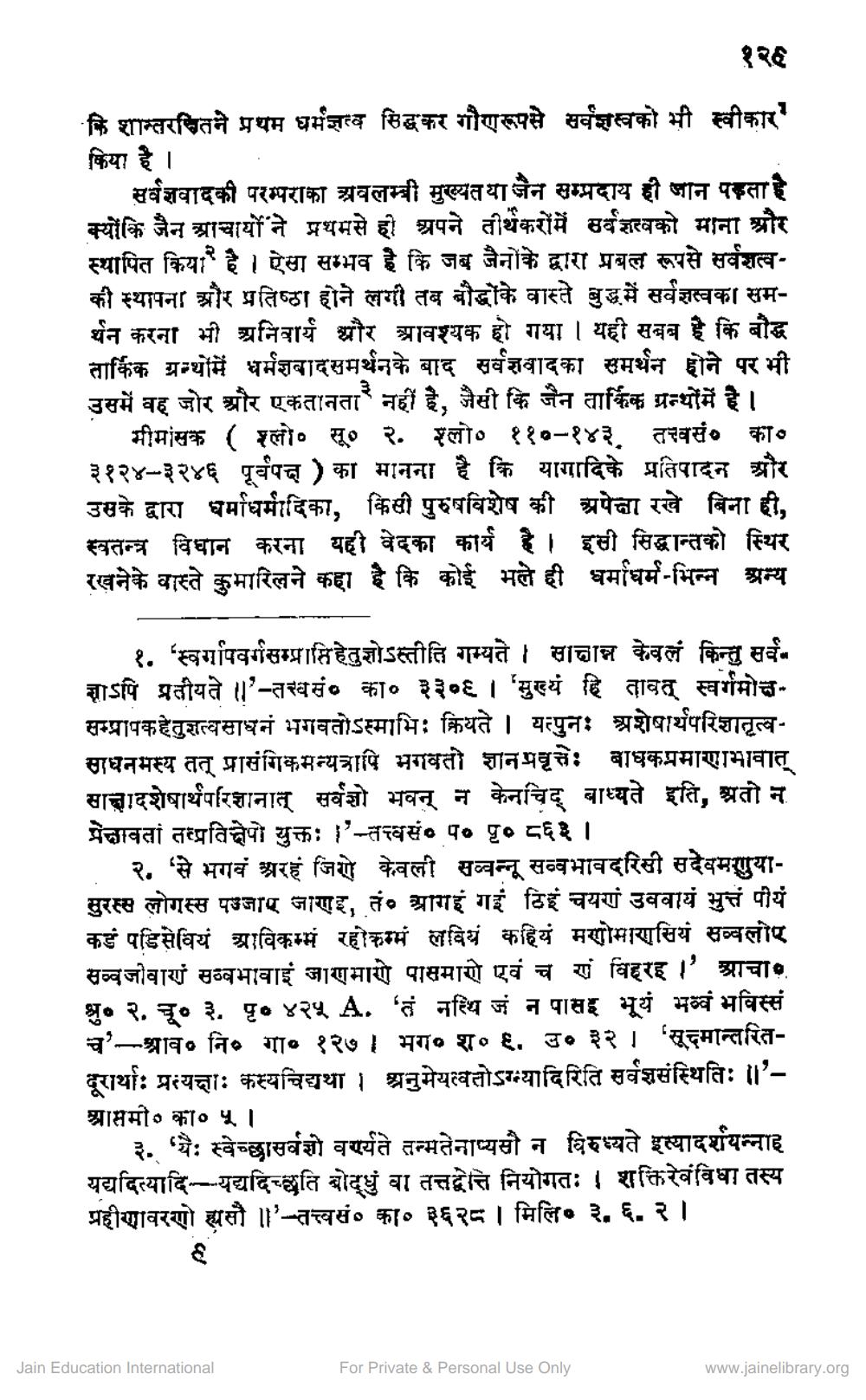________________
१२६
कि शान्तरक्षितने प्रथम धर्मज्ञत्व सिद्धकर गौणरूप से सर्वज्ञस्त्रको भी स्वीकार किया है ।
daaraat परम्पराका अवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पड़ता है क्योंकि जैनाचार्यों ने प्रथमसे ही अपने तीर्थकरों में सर्वज्ञत्वको माना और स्थापित किया है । ऐसा सम्भव है कि जब जैनोंके द्वारा प्रबल रूप से सर्वशत्व - की स्थापना और प्रतिष्ठा होने लगी तब बौद्धों के वास्ते बुद्ध में सर्वज्ञस्वका समर्थन करना भी अनिवार्य और आवश्यक हो गया । यही सबब है कि बौद्ध तार्किक ग्रन्थोंमें धर्मज्ञवादसमर्थन के बाद सर्वज्ञवादका समर्थन होने पर भी उसमें वह जोर और एकतानता नहीं है, जैसी कि जैन तार्किक ग्रन्थोंमें है।
३
मीमांसक ( श्लो० सू० २. श्लो० ११० - १४३, तवर्स० का० ३१२४ - ३२४६ पूर्वपक्ष ) का मानना है कि यागादिके प्रतिपादन और उसके द्वारा धर्माधर्मादिका, किसी पुरुषविशेष की अपेक्षा रखे बिना ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेदका कार्य है । इसी सिद्धान्तको स्थिर रखने के वास्ते कुमारिलने कहा है कि कोई भले ही धर्माधर्म-भिन्न अन्य
१. 'स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साक्षान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञाऽपि प्रतीयते ॥ ' - तस्वसं० का० ३३०६ । 'मुख्यं हि तावत् स्वर्गमोक्षसम्प्रापक हेतुज्ञत्वसाधनं भगवतोऽस्माभिः क्रियते । यत्पुनः शेषार्थपरिज्ञातृत्व - साधनमस्य तत् प्रासंगिकमन्यत्रापि भगवतो ज्ञान प्रवृत्तेः बाधकप्रमाणाभावात् साक्षादशेषार्थपरिज्ञानात् सर्वज्ञो भवन् न केनचिद् बाध्यते इति श्रतो न प्रेक्षावतां तत्प्रतिक्षेपो युक्तः ।' -तत्त्वसं० प० पृ० ८६३ |
2
२. ' से भगवं श्ररहं जिणे केवली सव्वन्नू सव्वभावदरिसी सदेवमरणुयासुररस लोगस्स पजाब जाणइ, तं० श्रागई गईं ठिहं चयणं उववायं भुक्तं पीयं कडं पडिसेवियं श्राविकम्मं रहोकम्मं लवियं कहियं मणोमाणसियं सव्वलोए सव्वजीवाणं सव्वभावाई जाणभागे पासमाणे एवं च णं विहरह ।' आचा०. श्रु० २. चू० ३. पृ० ४२५ A. 'तं नस्थि जं न पासइ भूयं भव्वं भविस्सं च' – श्राव० नि० गा० १२७ । भग० श० ६. उ० ३२ । 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । श्रनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥ 'श्रसमी०
[० का० ५ ।
३. ‘यैः स्वेच्छ्रासर्वज्ञो वर्यते तन्मतेनाप्यसौ न विरुध्यते इत्यादर्शयन्नाह यद्यदित्यादि --- यद्यदिच्छति बोद्धुं वा तत्तद्वेत्ति नियोगतः । शक्तिरेवंविधा तस्य प्रहीयावरणो ह्यसौ ॥' - तत्त्वसं० का० ३६२८ । मिलि० ३.६.२ ।
६
Jain Education International
*
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org