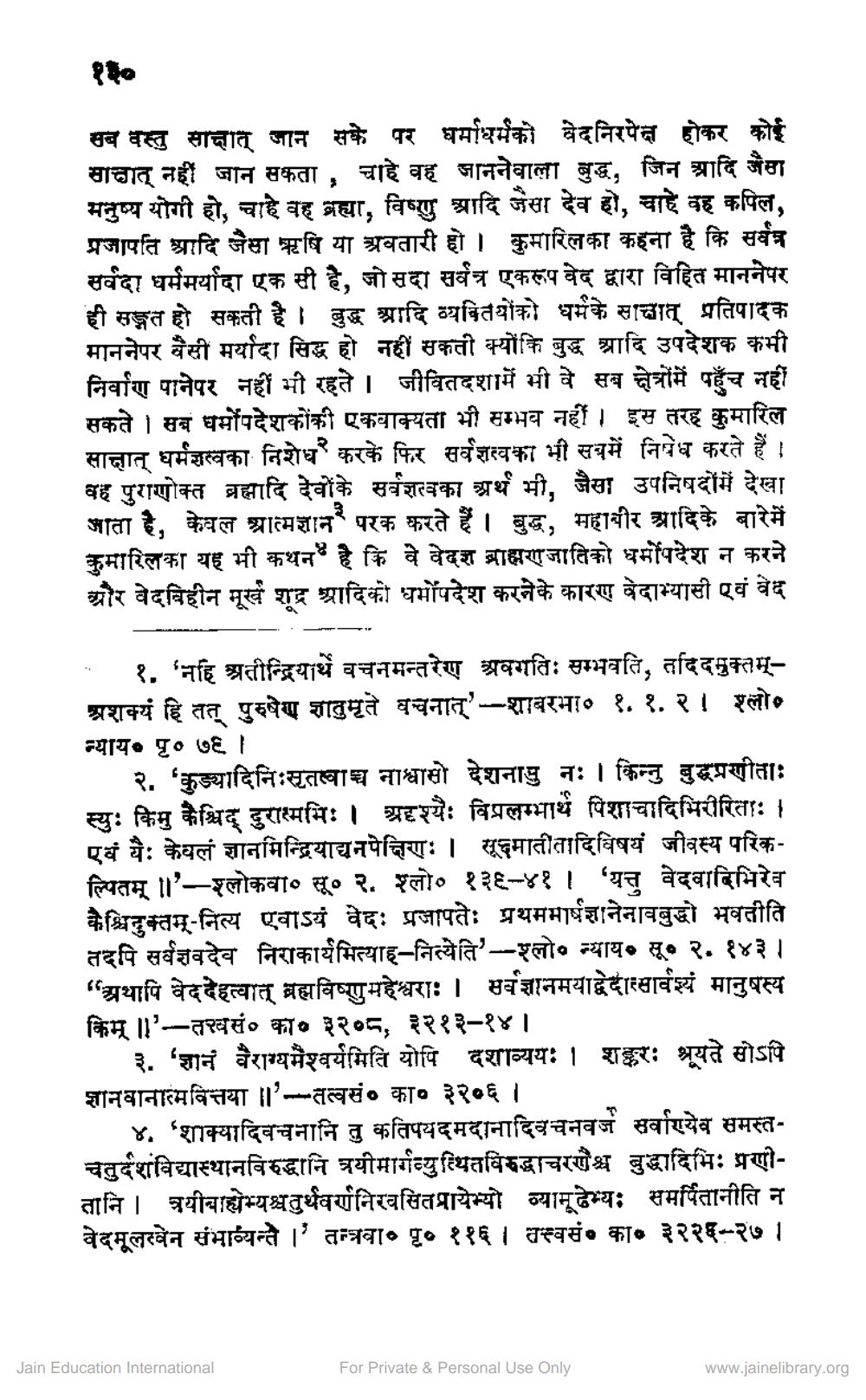________________
१३०
"
सब वस्तु साक्षात् जान सके पर धर्माधर्मको वेदनिरपेक्ष होकर कोई साक्षात् नहीं जान सकता चाहे वह जाननेवाला बुद्ध, जिन श्रादि जैसा मनुष्य योगी हो, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु आदि जैसा देव हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति श्रादि जैसा ऋषि या अवतारी हो । कुमारिलका कहना है कि सर्वत्र सर्वदा धर्ममर्यादा एक सी है, जो सदा सर्वत्र एकरूप वेद द्वारा विहित माननेपर ही सङ्गत हो सकती है । बुद्ध आदि व्यक्तियोंको धर्मके साक्षात् प्रतिपादक माननेपर वैसी मर्यादा सिद्ध हो नहीं सकती क्योंकि बुद्ध श्रादि उपदेशक कभी निर्वाण पानेपर नहीं भी रहते । जीवितदशामें भी वे सब क्षेत्रों में पहुँच नहीं सकते । सब धर्मोपदेशकों की एकवाक्यता भी सम्भव नहीं । इस तरह कुमारिल साक्षात् धर्मacant निशेध करके फिर सर्वज्ञत्वका भी सब में निषेध करते हैं । वह पुराणोक्त ब्रह्मादि देवों के सर्वशत्वका अर्थ भी, जैसा उपनिषदों में देखा जाता है, केवल श्रात्मज्ञान र परक करते हैं । बुद्ध, महावीर श्रादिके बारेमें कुमारिका यह भी कथन है कि वे वेदश ब्राह्मणजातिको धर्मोपदेश न करने और वेदविहीन मूर्ख शूद्र श्रादिको धर्मोपदेश करने के कारण वेदाभ्यासी एवं वेद
१. 'नहि श्रतीन्द्रियार्थे वचनमन्तरेण अवगतिः सम्भवति, तदिदमुक्तम्श्रशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात् ' - शाबरभा० १.१.२ | श्लो० न्याय० पृ० ७६ ।
:
२. 'कुड्यादिनिःसृतत्वाच्च नाश्वासो देशनासु नः । किन्नु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद् दुरात्मभिः । श्रदृश्यैः विप्रलम्भार्थ पिशाचादिभिरीरिताः । एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । सूक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम् ॥ ' - श्लोकवा० सू० २ श्लो० १३६-४१ । 'यत्तु वेदवादिभिरेव कैश्चिदुक्तम्- नित्य एवाऽयं वेदः प्रजापतेः प्रथममार्षज्ञानेनावबुद्धो भवतीति तदपि सर्वज्ञवदेव निराकार्यमित्याह - नित्येति' - श्लो० न्याय० सू० २. १४३ । “अथापि वेददेहत्वात् ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । सर्वज्ञानमयाद्वेदात्सार्वश्यं मानुषस्य किम् ॥ ' - तवसं ० का ० ३२०८, ३२१३–१४ ।
३. 'ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमिति योपि दशाव्ययः । शङ्करः श्रूयते सोऽपि ज्ञानवानात्मवित्तया ॥ ' - तत्वसं ० का ० ३२०६ ।
४. ' शाक्यादिवचनानि तु कतिपयद मदानादिवचनवर्जे सर्वाण्येव समस्त - चतुर्दशविद्यास्थानविरुद्धानि त्रयीमार्गव्यु स्थितविरुद्धाचरणैथ बुद्धादिभिः प्रणीतानि । त्रयीबाह्येभ्यश्चतुर्थवर्णनिरवसितप्रायेभ्यो व्यामूढेभ्यः समर्पितानीति न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते । तन्त्रवा० पृ० ११६ । तस्वसं० का ० ३२२६-२७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org