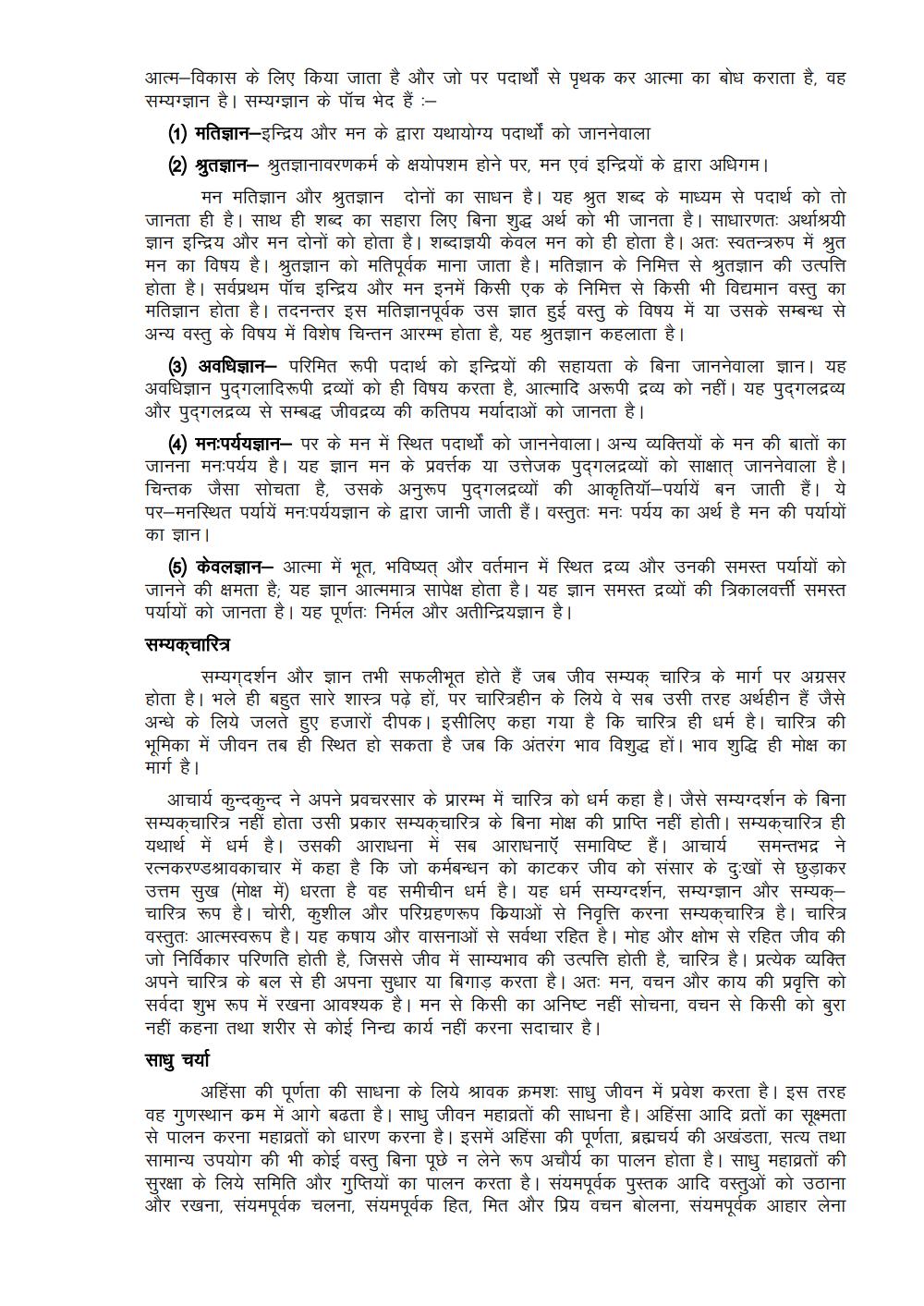________________
आत्म-विकास के लिए किया जाता है और जो पर पदार्थों से पृथक कर आत्मा का बोध कराता है, वह सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञान के पाँच भेद हैं :(1) मतिज्ञान-इन्द्रिय और मन के द्वारा यथायोग्य पदार्थों को जाननेवाला (2) श्रुतज्ञान- श्रुतज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम होने पर, मन एवं इन्द्रियों के द्वारा अधिगम।
___ मन मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों का साधन है। यह श्रुत शब्द के माध्यम से पदार्थ को तो जानता ही है। साथ ही शब्द का सहारा लिए बिना शुद्ध अर्थ को भी जानता है। साधारणतः अर्थाश्रयी ज्ञान इन्द्रिय और मन दोनों को होता है। शब्दाज्ञयी केवल मन को ही होता है। अतः स्वतन्त्ररुप में श्रुत मन का विषय है। श्रुतज्ञान को मतिपूर्वक माना जाता है। मतिज्ञान के निमित्त से श्रुतज्ञान की उत्पत्ति होता है। सर्वप्रथम पाँच इन्द्रिय और मन इनमें किसी एक के निमित्त से किसी भी विद्यमान वस्तु का मतिज्ञान होता है। तदनन्तर इस मतिज्ञानपूर्वक उस ज्ञात हुई वस्तु के विषय में या उसके सम्बन्ध से अन्य वस्तु के विषय में विशेष चिन्तन आरम्भ होता है, यह श्रुतज्ञान कहलाता है।
(6) अवधिज्ञान- परिमित रूपी पदार्थ को इन्द्रियों की सहायता के बिना जाननेवाला ज्ञान। यह अवधिज्ञान पुद्गलादिरूपी द्रव्यों को ही विषय करता है, आत्मादि अरूपी द्रव्य को नहीं। यह पुद्गलद्रव्य और पुद्गलद्रव्य से सम्बद्ध जीवद्रव्य की कतिपय मर्यादाओं को जानता है।
(4) मनःपर्ययज्ञान- पर के मन में स्थित पदार्थों को जाननेवाला। अन्य व्यक्तियों के मन की बातों का जानना मनःपर्यय है। यह ज्ञान मन के प्रवर्तक या उत्तेजक पुद्गलद्रव्यों को साक्षात् जाननेवाला है। चिन्तक जैसा सोचता है, उसके अनुरूप पुदगलद्रव्यों की आकृतियाँ-पर्यायें बन जाती हैं। ये पर-मनस्थित पर्यायें मनःपर्ययज्ञान के द्वारा जानी जाती हैं। वस्तुतः मनः पर्यय का अर्थ है मन की पर्यायों का ज्ञान।
(5) केवलज्ञान- आत्मा में भूत, भविष्यत् और वर्तमान में स्थित द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को जानने की क्षमता है; यह ज्ञान आत्ममात्र सापेक्ष होता है। यह ज्ञान समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को जानता है। यह पूर्णतः निर्मल और अतीन्द्रियज्ञान है। सम्यक्चारित्र
सम्यग्दर्शन और ज्ञान तभी सफलीभूत होते हैं जब जीव सम्यक चारित्र के मार्ग पर अग्रसर होता है। भले ही बहुत सारे शास्त्र पढ़े हों, पर चारित्रहीन के लिये वे सब उसी तरह अर्थहीन हैं जैसे अन्धे के लिये जलते हुए हजारों दीपक। इसीलिए कहा गया है कि चारित्र ही धर्म है। चारित्र की भूमिका में जीवन तब ही स्थित हो सकता है जब कि अंतरंग भाव विशुद्ध हों। भाव शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है।
आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने प्रवचरसार के प्रारम्भ में चारित्र को धर्म कहा है। जैसे सम्यग्दर्शन के बिना सम्यकचारित्र नहीं होता उसी प्रकार सम्यकचारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सम्यकचारित्र ही यथार्थ में धर्म है। उसकी आराधना में सब आराधनाएँ समाविष्ट हैं। आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्डश्रावकाचार में कहा है कि जो कर्मबन्धन को काटकर जीव को संसार के दुःखों से छुड़ाकर उत्तम सुख (मोक्ष में) धरता है वह समीचीन धर्म है। यह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप है। चोरी, कुशील और परिग्रहणरूप कियाओं से निवृत्ति करना सम्यक्चारित्र है। चारित्र वस्तुतः आत्मस्वरूप है। यह कषाय और वासनाओं से सर्वथा रहित है। मोह और क्षोभ से रहित जीव की जो निर्विकार परिणति होती है, जिससे जीव में साम्यभाव की उत्पत्ति होती है, चारित्र है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारित्र के बल से ही अपना सुधार या बिगाड़ करता है। अतः मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को सर्वदा शुभ रूप में रखना आवश्यक है। मन से किसी का अनिष्ट नहीं सोचना, वचन से किसी को बुरा नहीं कहना तथा शरीर से कोई निन्द्य कार्य नहीं करना सदाचार है। साधु चर्या
अहिंसा की पूर्णता की साधना के लिये श्रावक क्रमशः साधु जीवन में प्रवेश करता है। इस तरह वह गुणस्थान क्रम में आगे बढ़ता है। साधु जीवन महाव्रतों की साधना है। अहिंसा आदि व्रतों का सूक्ष्मता से पालन करना महाव्रतों को धारण करना है। इसमें अहिंसा की पूर्णता, ब्रह्मचर्य की अखंडता, सत्य तथा सामान्य उपयोग की भी कोई वस्तु बिना पूछे न लेने रूप अचौर्य का पालन होता है। साधु महाव्रतों की सुरक्षा के लिये समिति और गुप्तियों का पालन करता है। संयमपूर्वक पुस्तक आदि वस्तुओं को उठाना और रखना, संयमपूर्वक चलना, संयमपूर्वक हित, मित और प्रिय वचन बोलना, संयमपूर्वक आहार लेना