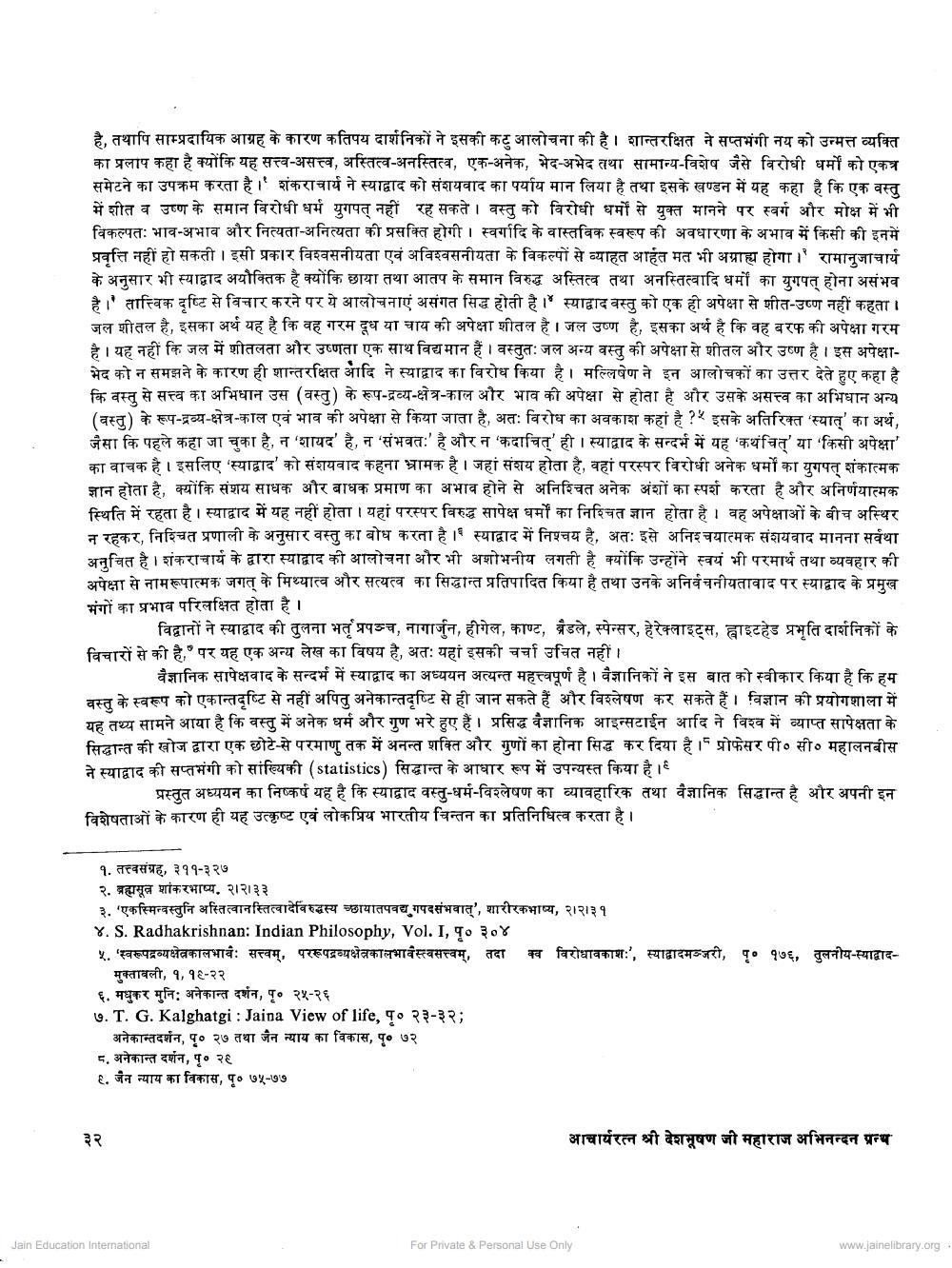________________ है, तथापि साम्प्रदायिक आग्रह के कारण कतिपय दार्शनिकों ने इसकी कटु आलोचना की है। शान्तरक्षित ने सप्तभंगी नय को उन्मत्त व्यक्ति का प्रलाप कहा है क्योंकि यह सत्त्व-असत्त्व, अस्तित्व-अनस्तित्व, एक-अनेक, भेद-अभेद तथा सामान्य-विशेष जैसे विरोधी धर्मों को एकत्र समेटने का उपक्रम करता है।' शंकराचार्य ने स्याद्वाद को संशयवाद का पर्याय मान लिया है तथा इसके खण्डन में यह कहा है कि एक वस्तु में शीत व उष्ण के समान विरोधी धर्म युगपत् नहीं रह सकते। वस्तु को विरोधी धर्मों से युक्त मानने पर स्वर्ग और मोक्ष में भी विकल्पतः भाव-अभाव और नित्यता-अनित्यता की प्रसक्ति होगी। स्वर्गादि के वास्तविक स्वरूप की अवधारणा के अभाव में किसी की इनमें प्रवत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार विश्वसनीयता एवं अविश्वसनीयता के विकल्पों से व्याहत आहेत मत भी अग्राह्य होगा। रामानुजाचार्य के अनुसार भी स्याद्वाद अयौक्तिक है क्योंकि छाया तथा आतप के समान विरुद्ध अस्तित्व तथा अनस्तित्वादि धर्मों का युगपत् होना असंभव है। तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर ये आलोचनाएं असंगत सिद्ध होती है।' स्याद्वाद वस्तु को एक ही अपेक्षा से शीत-उष्ण नहीं कहता। जल शीतल है, इसका अर्थ यह है कि वह गरम दूध या चाय की अपेक्षा शीतल है / जल उष्ण है, इसका अर्थ है कि वह बरफ की अपेक्षा गरम है। यह नहीं कि जल में शीतलता और उष्णता एक साथ विद्यमान हैं / वस्तुतः जल अन्य वस्तु की अपेक्षा से शीतल और उष्ण है। इस अपेक्षाभेद को न समझने के कारण ही शान्तरक्षित आदि ने स्याद्वाद का विरोध किया है। मल्लिषेण ने इन आलोचकों का उत्तर देते हुए कहा है कि वस्तु से सत्त्व का अभिधान उस (वस्तु) के रूप-द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव की अपेक्षा से होता है और उसके असत्त्व का अभिधान अन्य (वस्तु) के रूप-द्रव्य-क्षेत्र-काल एवं भाव की अपेक्षा से किया जाता है, अत: विरोध का अवकाश कहां है ?5 इसके अतिरिक्त स्यात्' का अर्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, न 'शायद' है, न संभवतः' है और न 'कदाचित्' ही / स्याद्वाद के सन्दर्भ में यह कथंचित्' या किसी अपेक्षा' का वाचक है। इसलिए 'स्याद्वाद' को संशयवाद कहना भ्रामक है। जहां संशय होता है, वहां परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का युगपत् शंकात्मक ज्ञान होता है, क्योंकि संशय साधक और बाधक प्रमाण का अभाव होने से अनिश्चित अनेक अंशों का स्पर्श करता है और अनिर्णयात्मक स्थिति में रहता है। स्याद्वाद में यह नहीं होता। यहां परस्पर विरुद्ध सापेक्ष धर्मों का निश्चित ज्ञान होता है। वह अपेक्षाओं के बीच अस्थिर न रहकर, निश्चित प्रणाली के अनुसार वस्तु का बोध करता है / स्याद्वाद में निश्चय है, अतः इसे अनिश्चयात्मक संशयवाद मानना सर्वथा अनचित है। शंकराचार्य के द्वारा स्याद्वाद की आलोचना और भी अशोभनीय लगती है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी परमार्थ तथा व्यवहार की अपेक्षा से नामरूपात्मक जगत् के मिथ्यात्व और सत्यत्व का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है तथा उनके अनिर्वचनीयतावाद पर स्याद्वाद के प्रमुख मंगों का प्रभाव परिलक्षित होता है। विद्वानों ने स्याद्वाद की तुलना भर्तृ प्रपञ्च, नागार्जुन, हीगेल, काण्ट, ड्रडले, स्पेन्सर, हेरेक्लाइट्स, ह्वाइटहेड प्रभृति दार्शनिकों के विचारों से की है, पर यह एक अन्य लेख का विषय है, अतः यहां इसकी चर्चा उचित नहीं। वैज्ञानिक सापेक्षवाद के सन्दर्भ में स्याद्वाद का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम वस्त के स्वरूप को एकान्तदृष्टि से नहीं अपितु अनेकान्तदृष्टि से ही जान सकते हैं और विश्लेषण कर सकते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में यह तथ्य सामने आया है कि वस्तु में अनेक धर्म और गुण भरे हुए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्सटाईन आदि ने विश्व में व्याप्त सापेक्षता के सिद्धान्त की खोज द्वारा एक छोटे-से परमाणु तक में अनन्त शक्ति और गुणों का होना सिद्ध कर दिया है। प्रोफेसर पी० सी० महालनबीस ने स्याद्वाद की सप्तभंगी को सांख्यिकी (statistics) सिद्धान्त के आधार रूप में उपन्यस्त किया है। प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि स्याद्वाद वस्तु-धर्म-विश्लेषण का व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक सिद्धान्त है और अपनी इन विशेषताओं के कारण ही यह उत्कृष्ट एवं लोकप्रिय भारतीय चिन्तन का प्रतिनिधित्व करता है। 1. तत्त्वसंग्रह, 311-327 2. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, 2 / 2 / 33 3. 'एकस्मिन्वस्तुनि अस्तित्वानस्तित्वादेविरुद्धस्य च्छायातपवद्य गपदसंभवात्', शारीरकभाष्य, 2 / 2 / 31 4. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy, Vol. I, पृ० 304 5. 'स्वरूपद्रव्यक्षेत्रकालभावः सत्त्वम्, पररूपद्रव्यक्षेत्रकालभावस्त्वसत्त्वम्, तदा क्य विरोधावकाशः', स्याद्वादमञ्जरी, पृ. 176, तुलनीय-स्याद्वाद मुक्तावली, 1, 19-22 6. मधुकर मुनि: अनेकान्त दर्शन, पृ० 25-26 7. T. G. Kalghatgi : Jaina View of life, पृ० 23-32; ___अनेकान्तदर्शन, पृ० 27 तथा जैन न्याय का विकास, पु०७२ 8. अनेकान्त दर्शन, पृ० 26 6. जैन न्याय का विकास, पृ० 75-77 10.22 32 आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन प्रन्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org