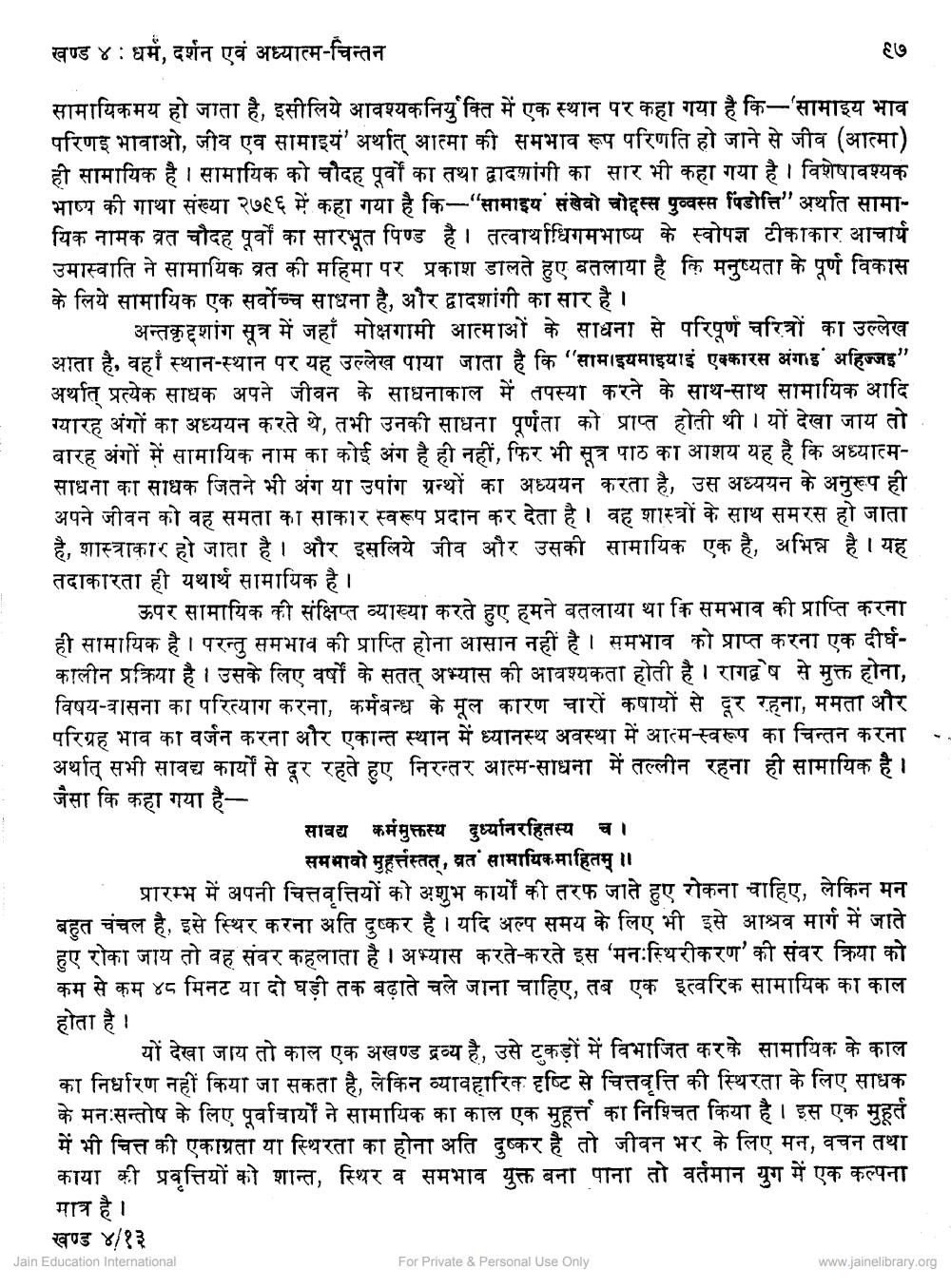________________
खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन
१७
सामायिकमय हो जाता है, इसीलिये आवश्यकनियुक्ति में एक स्थान पर कहा गया है कि-'सामाइय भाव परिणइ भावाओ, जीव एव सामाइयं' अर्थात् आत्मा की समभाव रूप परिणति हो जाने से जीव (आत्मा) ही सामायिक है । सामायिक को चौदह पूर्वो का तथा द्वादशांगी का सार भी कहा गया है। विशेषावश्यक भाष्य की गाथा संख्या २७६६ में कहा गया है कि-“सामाइय संखेवो चोद्दस्स पुव्वस्स पिंडोत्ति" अर्थात सामायिक नामक व्रत चौदह पूर्वो का सारभूत पिण्ड है। तत्वार्थाधिगमभाष्य के स्वोपज्ञ टीकाकार आचार्य उमास्वाति ने सामायिक व्रत की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि मनुष्यता के पूर्ण विकास के लिये सामायिक एक सर्वोच्च साधना है, और द्वादशांगी का सार है।।
अन्तकृद्दशांग सूत्र में जहाँ मोक्षगामी आत्माओं के साधना से परिपूर्ण चरित्रों का उल्लेख आता है, वहाँ स्थान-स्थान पर यह उल्लेख पाया जाता है कि "सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाई अहिज्जइ" अर्थात् प्रत्येक साधक अपने जीवन के साधनाकाल में तपस्या करने के साथ-साथ सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन करते थे, तभी उनकी साधना पूर्णता को प्राप्त होती थी। यों देखा जाय तो बारह अंगों में सामायिक नाम का कोई अंग है ही नहीं, फिर भी सूत्र पाठ का आशय यह है कि अध्यात्मसाधना का साधक जितने भी अंग या उपांग ग्रन्थों का अध्ययन करता है, उस अध्ययन के अनुरूप ही अपने जीवन को वह समता का साकार स्वरूप प्रदान कर देता है। वह शास्त्रों के साथ समरस हो जाता है, शास्त्राकार हो जाता है। और इसलिये जीव और उसकी सामायिक एक है, अभिन्न है। यह तदाकारता ही यथार्थ सामायिक है।
ऊपर सामायिक की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए हमने बतलाया था कि समभाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है । परन्तु समभाव की प्राप्ति होना आसान नहीं है। समभाव को प्राप्त करना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। उसके लिए वर्षों के सतत् अभ्यास की आवश्यकता होती है । रागद्वष से मुक्त होना, विषय-वासना का परित्याग करना, कर्मबन्ध के मूल कारण चारों कषायों से दूर रहना, ममता और परिग्रह भाव का वर्जन करना और एकान्त स्थान में ध्यानस्थ अवस्था में आत्म-स्वरूप का चिन्तन करना .. अर्थात् सभी सावध कार्यों से दूर रहते हुए निरन्तर आत्म-साधना में तल्लीन रहना ही सामायिक है। जैसा कि कहा गया है
सावध कर्म मुक्तस्य दुर्ध्यानरहितस्य च ।
समभावो मुहूर्तस्तत्, व्रत सामायिकमाहितम् ।। प्रारम्भ में अपनी चित्तवृत्तियों को अशुभ कार्यों की तरफ जाते हुए रोकना चाहिए, लेकिन मन बहुत चंचल है, इसे स्थिर करना अति दुष्कर है । यदि अल्प समय के लिए भी इसे आश्रव मार्ग में जाते हुए रोका जाय तो वह संवर कहलाता है । अभ्यास करते-करते इस 'मनःस्थिरीकरण' की संवर क्रिया को कम से कम ४८ मिनट या दो घड़ी तक बढ़ाते चले जाना चाहिए, तब एक इत्वरिक सामायिक का काल होता है।
यों देखा जाय तो काल एक अखण्ड द्रव्य है, उसे टुकड़ों में विभाजित कर के सामायिक के काल का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से चित्तवृत्ति की स्थिरता के लिए साधक के मनःसन्तोष के लिए पूर्वाचार्यों ने सामायिक का काल एक मुहूर्त का निश्चित किया है । इस एक मुहूर्त में भी चित्त की एकाग्रता या स्थिरता का होना अति दुष्कर है तो जीवन भर के लिए मन, वचन तथा काया की प्रवृत्तियों को शान्त, स्थिर व समभाव युक्त बना पाना तो वर्तमान युग में एक कल्पना मात्र है। खण्ड ४/१३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org