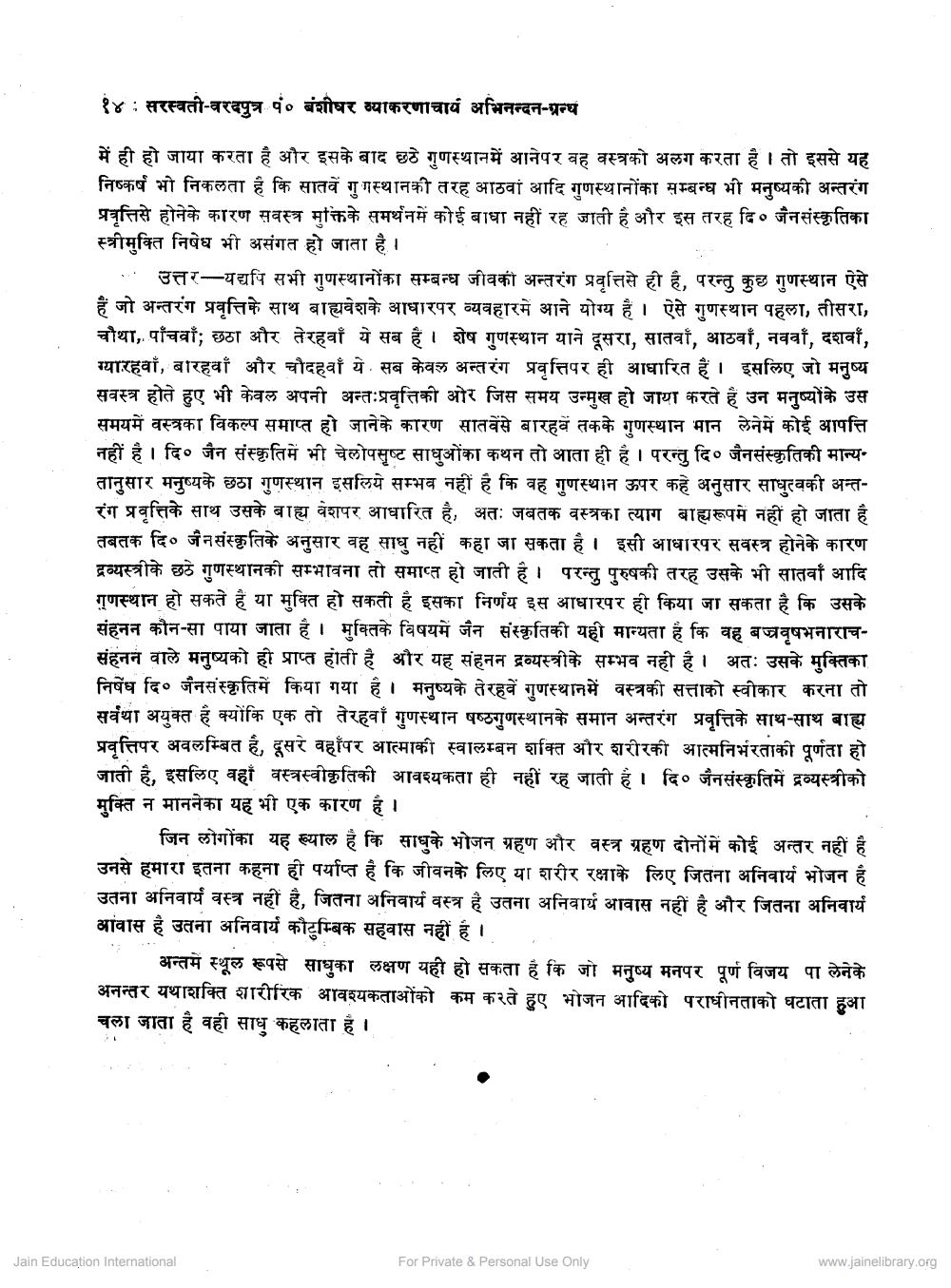________________ 14 : सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-प्रन्ध में ही हो जाया करता है और इसके बाद छठे गुणस्थानमें आनेपर वह वस्त्रको अलग करता है / तो इससे यह निष्कर्ष भो निकलता है कि सातवें गुणस्थानकी तरह आठवां आदि गुणस्थानोंका सम्बन्ध भी मनुष्यकी अन्तरंग प्रवृत्तिसे होनेके कारण सवस्त्र मक्तिके समर्थनमें कोई बाधा नहीं रह जाती है और इस तरह दि० जैनसंस्कृतिका स्त्रीमुक्ति निषेध भी असंगत हो जाता है। उत्तर-यद्यपि सभी गणस्थानोंका सम्बन्ध जीवको अन्तरंग प्रवृत्तिसे ही है, परन्तु कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जो अन्तरंग प्रवृत्ति के साथ बाह्यवेशके आधारपर व्यवहारमें आने योग्य है। ऐसे गुणस्थान पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ; छठा और तेरहवाँ ये सब है। शेष गुणस्थान याने दूसरा, सातवाँ, आठवाँ, नववाँ, दशवाँ, ग्यारहवाँ, बारहवाँ और चौदहवां ये सब केवल अन्तरंग प्रवृत्तिपर ही आधारित हैं। इसलिए जो मनुष्य सवस्त्र होते हुए भी केवल अपनी अन्तःप्रवृत्तिकी ओर जिस समय उन्मुख हो जाया करते है उन मनुष्योंके उस समयमें वस्त्रका विकल्प समाप्त हो जानेके कारण सातवेंसे बारहवें तकके गणस्थान मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है / दि० जैन संस्कृतिमें भी चेलोपसृष्ट साधुओंका कथन तो आता ही है / परन्तु दि० जैनसंस्कृतिकी मान्यतानुसार मनुष्यके छठा गुणस्थान इसलिये सम्भव नहीं है कि वह गुणस्थान ऊपर कहे अनुसार साधुत्वकी अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ उसके बाह्य वेशपर आधारित है, अतः जबतक वस्त्रका त्याग बाह्यरूपमें नहीं हो जाता है तबतक दि० जैन संस्कृतिके अनुसार वह साधु नहीं कहा जा सकता है। इसी आधारपर सवस्त्र होनेके कारण द्रव्यस्त्रीके छठे गुणस्थानको सम्भावना तो समाप्त हो जाती है। परन्तु पुरुषकी तरह उसके भी सातवाँ आदि गुणस्थान हो सकते है या मुक्ति हो सकती है इसका निर्णय इस आधारपर ही किया जा सकता है कि उसके संहनन कौन-सा पाया जाता है / मुक्तिके विषयमें जैन संस्कृतिकी यही मान्यता है कि वह बज्रवृषभनाराचसंहनन वाले मनुष्यको ही प्राप्त होती है और यह संहनन द्रव्यस्त्रीके सम्भव नही है। अतः उसके मुक्तिका निषेध दि० जनसंस्कृतिमें किया गया है। मनुष्यके तेरहवें गणस्थानमें वस्त्रकी सत्ताको स्वीकार करना तो सर्वथा अयुक्त है क्योंकि एक तो तेरहवाँ गुणस्थान षष्ठगुणस्थानके समान अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ-साथ बाह्य प्रवृत्तिपर अवलम्बित है, दूसरे वहाँपर आत्माकी स्वालम्बन शक्ति और शरीरकी आत्मनिर्भरताको पूर्णता हो जाती है, इसलिए वहाँ वस्त्रस्वीकृतिकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। दि० जनसंस्कृतिमें द्रव्यस्त्रीको मुक्ति न माननेका यह भी एक कारण है। जिन लोगोंका यह ख्याल है कि साधुके भोजन ग्रहण और वस्त्र ग्रहण दोनों में कोई अन्तर नहीं है उनसे हमारा इतना कहना ही पर्याप्त है कि जीवनके लिए या शरीर रक्षाके लिए जितना अनिवार्य भोजन है उतना अनिवार्य वस्त्र नहीं है, जितना अनिवार्य वस्त्र है उतना अनिवार्य आवास नहीं है और जितना अनिवार्य आवास है उतना अनिवार्य कौटुम्बिक सहवास नहीं है। अन्तमें स्थूल रूपसे साधुका लक्षण यही हो सकता है कि जो मनुष्य मनपर पूर्ण विजय पा लेनेके अनन्तर यथाशक्ति शारीरिक आवश्यकताओंको कम करते हए भोजन आदिको पराधीनताको घटाता हुआ चला जाता है वही साधु कहलाता है / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org