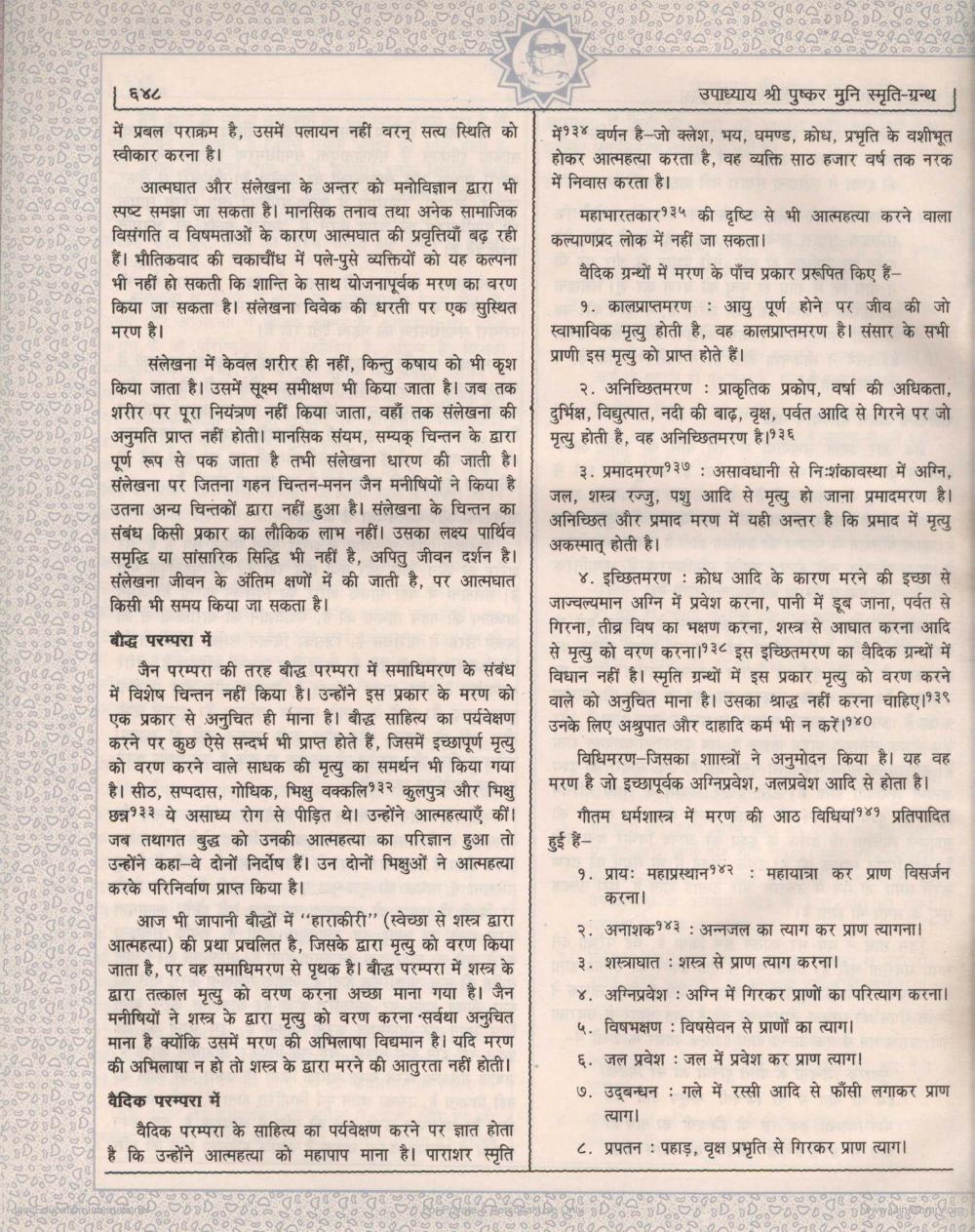________________
Page
६४८
में प्रबल पराक्रम है, उसमें पलायन नहीं वरन् सत्य स्थिति को स्वीकार करना है।
आत्मघात और संलेखना के अन्तर को मनोविज्ञान द्वारा भी स्पष्ट समझा जा सकता है। मानसिक तनाव तथा अनेक सामाजिक विसंगति व विषमताओं के कारण आत्मघात की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। भौतिकवाद की चकाचौंध में पले-पुसे व्यक्तियों को यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि शान्ति के साथ योजनापूर्वक मरण का वरण किया जा सकता है। संलेखना विवेक की धरती पर एक सुस्थित मरण है।
संलेखना में केवल शरीर ही नहीं, किन्तु कषाय को भी कृश किया जाता है। उसमें सूक्ष्म समीक्षण भी किया जाता है। जब तक शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं किया जाता, वहाँ तक संलेखना की अनुमति प्राप्त नहीं होती। मानसिक संयम, सम्यक् चिन्तन के द्वारा पूर्ण रूप से पक जाता है तभी संलेखना धारण की जाती है। संलेखना पर जितना गहन चिन्तन-मनन जैन मनीषियों ने किया है उतना अन्य चिन्तकों द्वारा नहीं हुआ है। संलेखना के चिन्तन का संबंध किसी प्रकार का लौकिक लाभ नहीं उसका लक्ष्य पार्थिव समृद्धि या सांसारिक सिद्धि भी नहीं है, अपितु जीवन दर्शन है। संलेखना जीवन के अंतिम क्षणों में की जाती है, पर आत्मघात किसी भी समय किया जा सकता है।
बौद्ध परम्परा में
जैन परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा में समाधिमरण के संबंध में विशेष चिन्तन नहीं किया है। उन्होंने इस प्रकार के मरण को एक प्रकार से अनुचित ही माना है। बौद्ध साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर कुछ ऐसे सन्दर्भ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें इच्छापूर्ण मृत्यु को वरण करने वाले साधक की मृत्यु का समर्थन भी किया गया है। सीठ, सप्पदास, गोधिक भिक्षु वक्कलि १३२ कुलपुत्र और भिक्षु छन्न १३३ ये असाध्य रोग से पीड़ित थे। उन्होंने आत्महत्याएँ कीं । जब तथागत बुद्ध को उनकी आत्महत्या का परिज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा- वे दोनों निर्दोष हैं उन दोनों भिक्षुओं ने आत्महत्या करके परिनिर्वाण प्राप्त किया है।
"
आज भी जापानी बौद्धों में "हाराकीरी" (स्वेच्छा से शस्त्र द्वारा आत्महत्या) की प्रथा प्रचलित है, जिसके द्वारा मृत्यु को वरण किया जाता है, पर वह समाधिमरण से पृथक है। बौद्ध परम्परा में शस्त्र के द्वारा तत्काल मृत्यु को वरण करना अच्छा माना गया है। जैन मनीषियों ने शस्त्र के द्वारा मृत्यु को वरण करना सर्वथा अनुचित माना है क्योंकि उसमें मरण की अभिलाषा विद्यमान है। यदि मरण की अभिलाषा न हो तो शस्त्र के द्वारा मरने की आतुरता नहीं होती। वैदिक परम्परा में
वैदिक परम्परा के साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने आत्महत्या को महापाप माना है। पाराशर स्मृति
GRO
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
१३४ वर्णन है जो क्लेश, भय, घमण्ड, क्रोध, प्रभृति के वशीभूत होकर आत्महत्या करता है, वह व्यक्ति साठ हजार वर्ष तक नरक में निवास करता है।
महाभारतकार १३५ की दृष्टि से भी आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोक में नहीं जा सकता।
वैदिक ग्रन्थों में मरण के पाँच प्रकार प्ररूपित किए हैं
१. कालप्राप्तमरण : आयु पूर्ण होने पर जीव की जो स्वाभाविक मृत्यु होती है, वह कालप्राप्तमरण है। संसार के सभी प्राणी इस मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
२. अनिच्छितमरण प्राकृतिक प्रकोप वर्षा की अधिकता, दुर्भिक्ष, विद्युत्पात, नदी की बाढ़, वृक्ष, पर्वत आदि से गिरने पर जो मृत्यु होती है, वह अनिच्छितमरण है। १३६
३. प्रमादमरण १३७ : असावधानी से निःशंकावस्था में अग्नि, जल, शस्त्र रज्जु, पशु आदि से मृत्यु हो जाना प्रमादमरण है। अनिच्छित और प्रमाद मरण में यही अन्तर है कि प्रमाद में मृत्यु अकस्मात् होती है।
४. इच्छितमरण : क्रोध आदि के कारण मरने की इच्छा से जाज्वल्यमान अग्नि में प्रवेश करना, पानी में डूब जाना, पर्वत से गिरना, तीव्र विष का भक्षण करना, शस्त्र से आघात करना आदि से मृत्यु को वरण करना। १३८ इस इच्छितमरण का वैदिक ग्रन्थों में विधान नहीं है। स्मृति ग्रन्थों में इस प्रकार मृत्यु को वरण करने वाले को अनुचित माना है। उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए । १३९ उनके लिए अनुपात और दाहादि कर्म भी न करें । १४०
विधिमरण- जिसका शास्त्रों ने अनुमोदन किया है। यह वह मरण है जो इच्छापूर्वक अग्निप्रवेश, जलप्रवेश आदि से होता है।
गौतम धर्मशास्त्र में मरण की आठ विधियां १४१ प्रतिपादित हुई हैं
१. प्रायः महाप्रस्थान १४२ : महायात्रा कर प्राण विसर्जन करना।
२. अनाशक १४३ : अन्नजल का त्याग कर प्राण त्यागना। शस्त्राघात : शस्त्र से प्राण त्याग करना ।
३.
४.
अग्निप्रवेश : अग्नि में गिरकर प्राणों का परित्याग करना। ५. विषभक्षण विषसेवन से प्राणों का त्याग।
:
६. जल प्रवेश : जल में प्रवेश कर प्राण त्याग ।
७. उद्बन्धन : गले में रस्सी आदि से फाँसी लगाकर प्राण त्याग।
८. प्रपतन: पहाड़, वृक्ष प्रभृति से गिरकर प्राण त्याग ।
0000
www.ny 200amkane