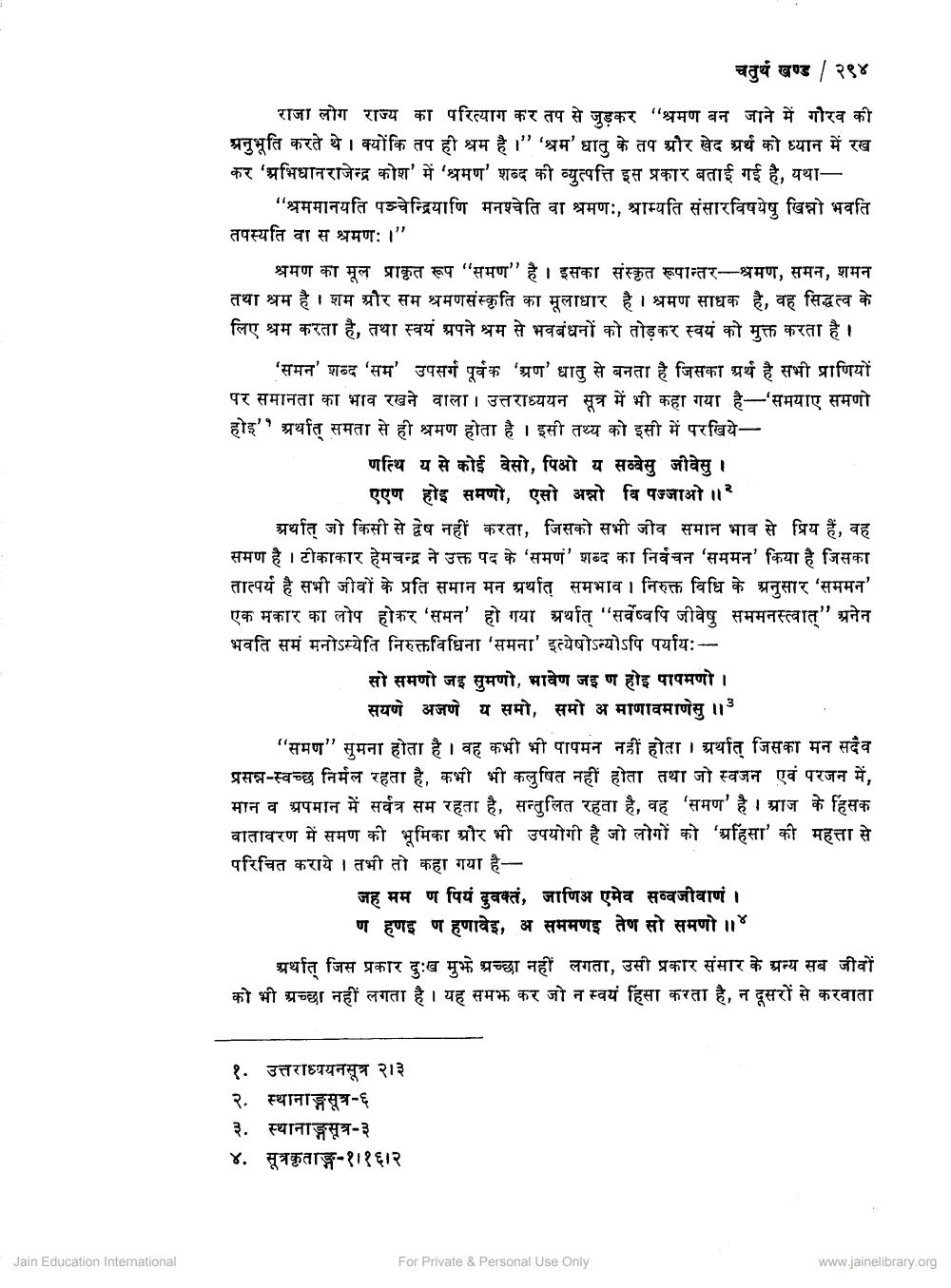________________
चतुर्थ खण्ड / २९४
राजा लोग राज्य का परित्याग कर तप से जुड़कर "श्रमण बन जाने में गौरव की अनुभूति करते थे। क्योंकि तप ही श्रम है।" 'श्रम' धातु के तप और खेद अर्थ को ध्यान में रख कर 'अभिधानराजेन्द्र कोश' में 'श्रमण' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है, यथा
"श्रममानयति पञ्चेन्द्रियाणि मनश्चेति वा श्रमणः, श्राम्यति संसारविषयेषु खिन्नो भवति तपस्यति वा स श्रमणः।"
श्रमण का मूल प्राकृत रूप "समण" है। इसका संस्कृत रूपान्तर-श्रमण, समन, शमन तथा श्रम है । शम और सम श्रमणसंस्कृति का मूलाधार है। श्रमण साधक है, वह सिद्धत्व के लिए श्रम करता है, तथा स्वयं अपने श्रम से भवबंधनों को तोड़कर स्वयं को मुक्त करता है।
'समन' शब्द 'सम' उपसर्ग पूर्वक 'अण' धातु से बनता है जिसका अर्थ है सभी प्राणियों पर समानता का भाव रखने वाला। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है-'समयाए समणो होइ'' अर्थात समता से ही श्रमण होता है । इसी तथ्य को इसी में परखिये
णत्थि य से कोई वेसो, पिओ य सम्वेसु जीवेसु ।
एएण होइ समणो, एसो अन्नो विपज्जाओ। अर्थात् जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसको सभी जीव समान भाव से प्रिय हैं, वह समण है । टीकाकार हेमचन्द्र ने उक्त पद के 'समणं' शब्द का निर्वचन 'सममन' किया है जिसका तात्पर्य है सभी जीवों के प्रति समान मन अर्थात् समभाव । निरुक्त विधि के अनुसार 'सममन' एक मकार का लोप होकर 'समन' हो गया अर्थात् "सर्वेष्वपि जीवेषु सममनस्त्वात्" अनेन भवति समं मनोऽस्येति निरुक्तविधिना 'समना' इत्येषोऽन्योऽपि पर्याय:
सो समणो जइ सुमणो, भावेण जइ ण होइ पापमणो ।
सयणे अजणे य समो, समो अमाणावमाणेसु ॥3 "समण" सुमना होता है। वह कभी भी पापमन नहीं होता । अर्थात् जिसका मन सदैव प्रसन्न-स्वच्छ निर्मल रहता है, कभी भी कलुषित नहीं होता तथा जो स्वजन एवं परजन में, मान व अपमान में सर्वत्र सम रहता है, सन्तुलित रहता है, वह 'समण' है। आज के हिंसक वातावरण में समण की भूमिका और भी उपयोगी है जो लोगों को 'अहिंसा' की महत्ता से परिचित कराये । तभी तो कहा गया है
जह मम ण पियं दुवक्तं, जाणिअ एमेव सव्वजीवाणं ।
ण हणइ ण हणावेइ, अ सममणइ तेण सो समणो॥४ अर्थात जिस प्रकार दु:ख मुझे अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संसार के अन्य सब जीवों को भी अच्छा नहीं लगता है। यह समझ कर जो न स्वयं हिंसा करता है, न दूसरों से करवाता
१. उत्तराध्ययनसूत्र २।३ २. स्थानाङ्गसूत्र-६ ३. स्थानाङ्गसूत्र-३ ४. सूत्रकृताङ्ग-१।१६।२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org