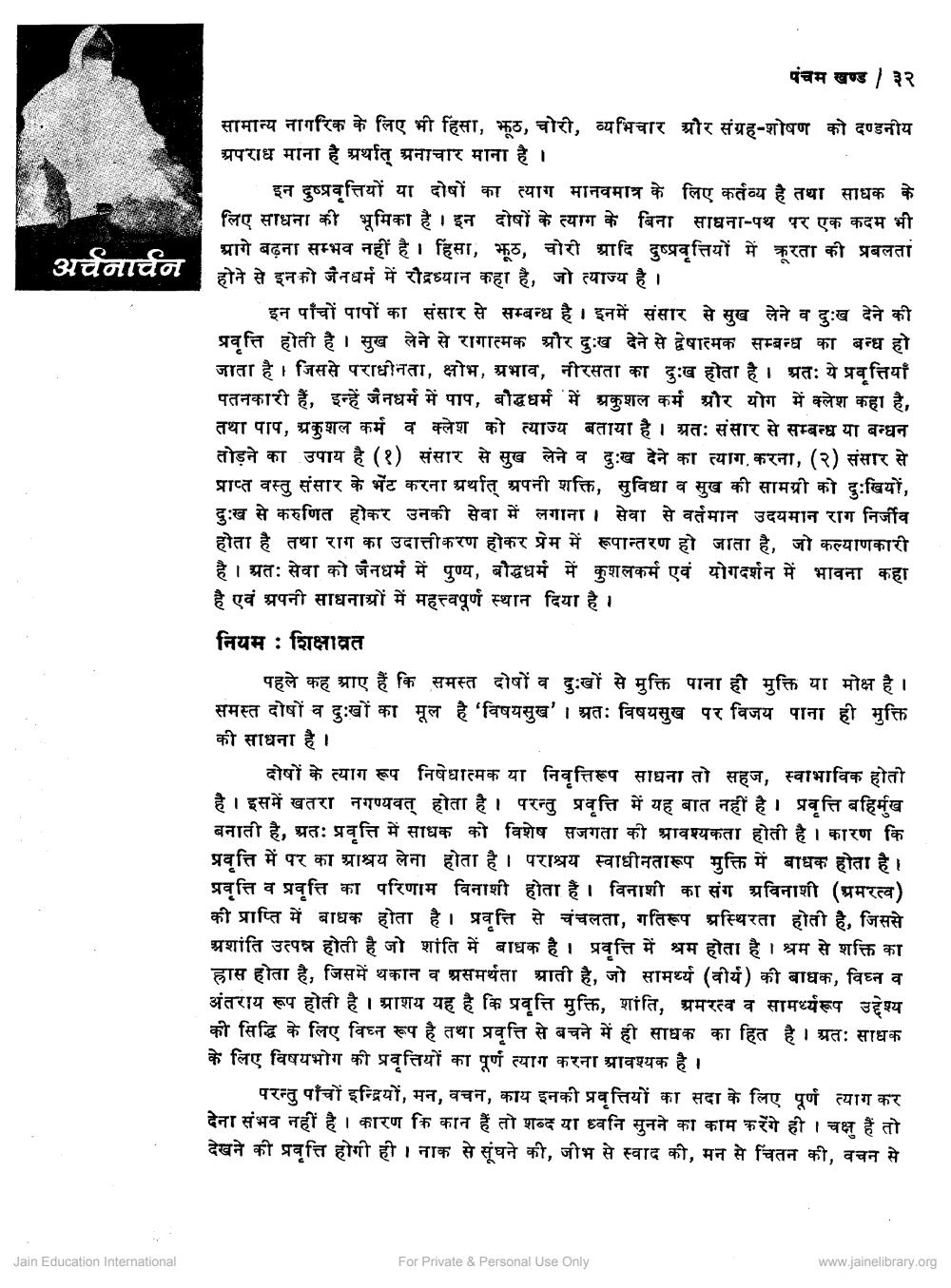________________
पंचम खण्ड | ३२
अर्चनार्चन
सामान्य नागरिक के लिए भी हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और संग्रह-शोषण को दण्डनीय अपराध माना है अर्थात् अनाचार माना है ।
इन दुष्प्रवृत्तियों या दोषों का त्याग मानवमात्र के लिए कर्तव्य है तथा साधक के लिए साधना की भूमिका है। इन दोषों के त्याग के बिना साधना-पथ पर एक कदम भी मागे बढ़ना सम्भव नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि दुष्प्रवृत्तियों में क्रूरता की प्रबलता होने से इनको जैनधर्म में रौद्रध्यान कहा है, जो त्याज्य है।
इन पाँचों पापों का संसार से सम्बन्ध है। इनमें संसार से सख लेने व दःख देने की प्रवृत्ति होती है। सुख लेने से रागात्मक और दुःख देने से द्वेषात्मक सम्बन्ध का बन्ध हो जाता है। जिससे पराधीनता, क्षोभ, अभाव, नीरसता का दुःख होता है। अतः ये प्रवृत्तियाँ पतनकारी हैं, इन्हें जैनधर्म में पाप, बौद्धधर्म में अकुशल कर्म और योग में क्लेश कहा है, तथा पाप, अकुशल कर्म व क्लेश को त्याज्य बताया है। अतः संसार से सम्बन्ध या बन्धन तोड़ने का उपाय है (१) संसार से सुख लेने व दुःख देने का त्याग करना, (२) संसार से प्राप्त वस्तु संसार के भेंट करना अर्थात् अपनी शक्ति, सुविधा व सुख की सामग्री को दुःखियों, दुःख से करुणित होकर उनकी सेवा में लगाना। सेवा से वर्तमान उदयमान राग निर्जीव होता है तथा राग का उदात्तीकरण होकर प्रेम में रूपान्तरण हो जाता है, जो कल्याणकारी है। अतः सेवा को जैनधर्म में पुण्य, बौद्धधर्म में कुशलकर्म एवं योगदर्शन में भावना कहा है एवं अपनी साधनाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है।
नियम : शिक्षावत
पहले कह पाए हैं कि समस्त दोषों व दुःखों से मुक्ति पाना ही मुक्ति या मोक्ष है। समस्त दोषों व दुःखों का मूल है 'विषयसुख' । अतः विषयसुख पर विजय पाना ही मुक्ति की साधना है।
दोषों के त्याग रूप निषेधात्मक या निवृत्तिरूप साधना तो सहज, स्वाभाविक होती है । इसमें खतरा नगण्यवत् होता है। परन्तु प्रवृत्ति में यह बात नहीं है। प्रवृत्ति बहिर्मुख बनाती है, अतः प्रवृत्ति में साधक को विशेष सजगता की आवश्यकता होती है। कारण कि प्रवृत्ति में पर का प्राश्रय लेना होता है। पराश्रय स्वाधीनतारूप मुक्ति में बाधक होता है। प्रवृत्ति व प्रवृत्ति का परिणाम विनाशी होता हैं। विनाशी का संग अविनाशी (अमरत्व) की प्राप्ति में बाधक होता है। प्रवृत्ति से चंचलता, गतिरूप अस्थिरता होती है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है जो शांति में बाधक है। प्रवृत्ति में श्रम होता है । श्रम से शक्ति का ह्रास होता है, जिसमें थकान व असमर्थता आती है, जो सामर्थ्य (वीर्य) की बाधक, विघ्न व अंतराय रूप होती है । आशय यह है कि प्रवृत्ति मुक्ति, शांति, अमरत्व व सामर्थ्यरूप उद्देश्य की सिद्धि के लिए विघ्न रूप है तथा प्रवृत्ति से बचने में ही साधक का हित है। अतः साधक के लिए विषयभोग की प्रवृत्तियों का पूर्ण त्याग करना आवश्यक है।
परन्तु पाँचों इन्द्रियों, मन, वचन, काय इनकी प्रवृत्तियों का सदा के लिए पूर्ण त्याग कर देना संभव नहीं है। कारण कि कान हैं तो शब्द या ध्वनि सुनने का काम करेंगे ही । चक्षु हैं तो देखने की प्रवृत्ति होगी ही। नाक से सूंघने की, जीभ से स्वाद की, मन से चितन की, वचन से
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org