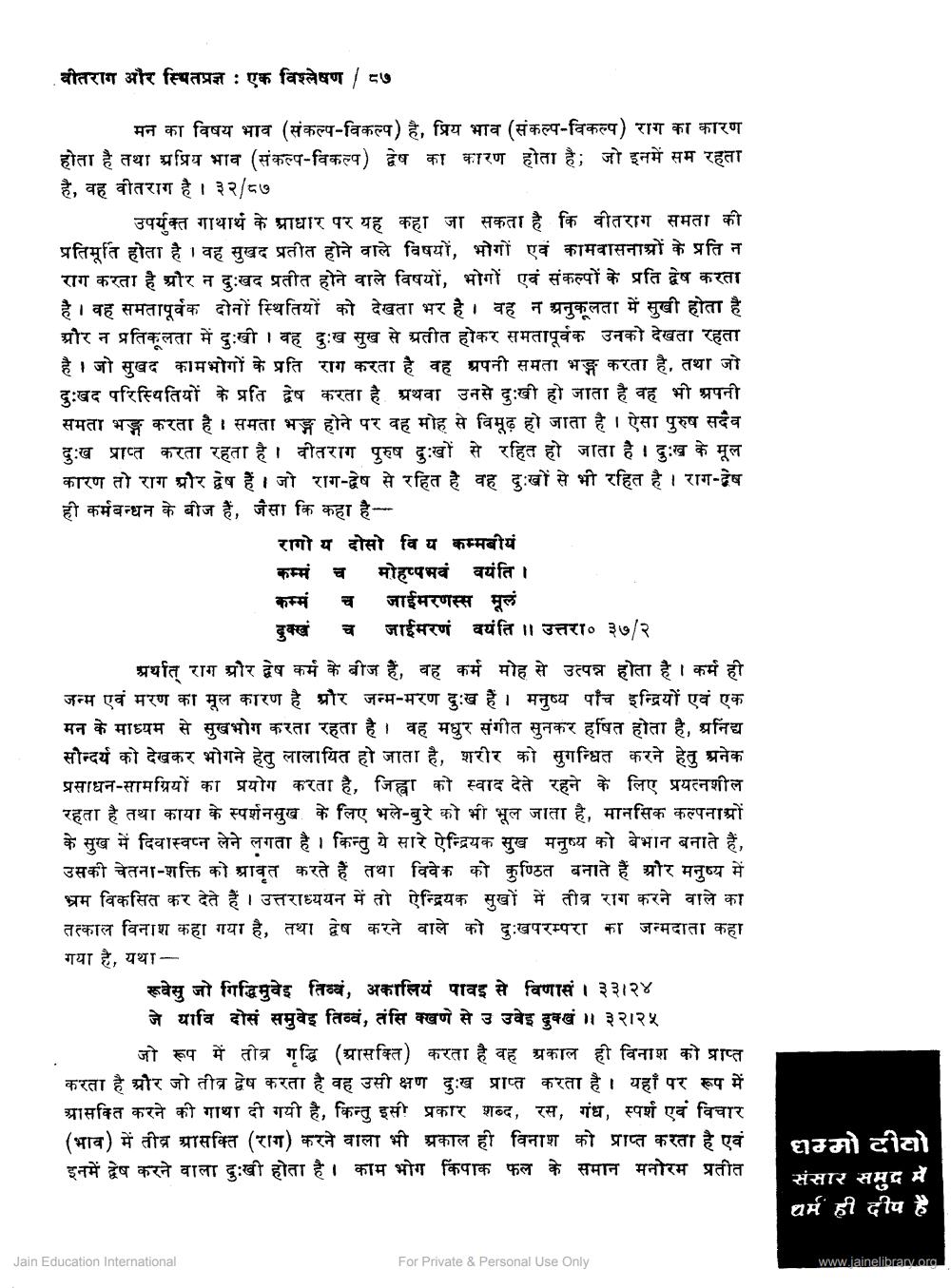________________
वीतराग और स्थितप्रज्ञ : एक विश्लेषण | ८७
मन का विषय भाव (संकल्प-विकल्प) है, प्रिय भाव (संकल्प-विकल्प) राग का कारण होता है तथा अप्रिय भाव (संकल्प-विकल्प) द्वेष का कारण होता है; जो इनमें सम रहता है, वह वीतराग है । ३२/८७
उपर्युक्त गाथार्थ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वीतराग समता की प्रतिमूर्ति होता है । वह सुखद प्रतीत होने वाले विषयों, भोगों एवं कामवासनामों के प्रति राग करता है और न दुःखद प्रतीत होने वाले विषयों, भोगों एवं संकल्पों के प्रति द्वेष करता है। वह समतापूर्वक दोनों स्थितियों को देखता भर है। वह न अनुकूलता में सुखी होता है और न प्रतिकूलता में दुःखी । वह दुःख सुख से प्रतीत होकर समतापूर्वक उनको देखता रहता है । जो सुखद कामभोगों के प्रति राग करता है वह अपनी समता भङ्ग करता है, तथा जो दुःखद परिस्थितियों के प्रति द्वेष करता है अथवा उनसे दुःखी हो जाता है वह भी अपनी समता भङ्ग करता है । समता भङ्ग होने पर वह मोह से विमूढ़ हो जाता है । ऐसा पुरुष सदैव दु:ख प्राप्त करता रहता है। वीतराग पुरुष दु:खों से रहित हो जाता है। दु:ख के मूल कारण तो राग और द्वेष हैं। जो राग-द्वेष से रहित है वह दुःखों से भी रहित है। राग-द्वेष ही कर्मबन्धन के बीज हैं, जैसा कि कहा है
रागो य दोसो विय कम्मबीयं कम्मं च मोहप्पभवं वयंति । कम्मं च जाईमरणस्स मुलं
दुक्खं च जाईमरणं वयंति ॥ उत्तरा० ३७/२ अर्थात् राग और द्वेष कर्म के बीज हैं, वह कर्म मोह से उत्पन्न होता है । कर्म ही जन्म एवं मरण का मूल कारण है और जन्म-मरण दुःख हैं। मनुष्य पाँच इन्द्रियों एवं एक मन के माध्यम से सुखभोग करता रहता है। वह मधुर संगीत सुनकर हर्षित होता है, अनिंद्य सौन्दर्य को देखकर भोगने हेतु लालायित हो जाता है, शरीर को सुगन्धित करने हेतु अनेक प्रसाधन-सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिह्वा को स्वाद देते रहने के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा काया के स्पर्शनसुख के लिए भले-बुरे को भी भूल जाता है, मानसिक कल्पनाओं के सुख में दिवास्वप्न लेने लगता है। किन्तु ये सारे ऐन्द्रियक सुख मनुष्य को बेभान बनाते हैं, उसकी चेतना-शक्ति को प्रावृत करते हैं तथा विवेक को कुण्ठित बनाते हैं और मनुष्य में भ्रम विकसित कर देते हैं। उत्तराध्ययन में तो ऐन्द्रियक सुखों में तीव्र 'राग करने वाले का तत्काल विनाश कहा गया है, तथा द्वेष करने वाले को दुःखपरम्परा का जन्मदाता कहा गया है, यथा
रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं। ३३१२४ जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ॥ ३२॥२५
जो रूप में तीव्र गद्धि (प्रासक्ति) करता है वह अकाल ही विनाश को प्राप्त करता है और जो तीव्र द्वेष करता है वह उसी क्षण दुःख प्राप्त करता है। यहाँ पर रूप में आसक्ति करने की गाथा दी गयी है, किन्तु इसी प्रकार शब्द, रस, गंध, स्पर्श एवं विचार (भाव) में तीव्र आसक्ति (राग) करने वाला भी अकाल ही विनाश को प्राप्त करता है एवं इनमें द्वेष करने वाला दुःखी होता है। काम भोग किंपाक फल के समान मनोरम प्रतीत
धम्मो दीयो संसार समुद्र में चर्म ही दीय है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.iainelibrary.org