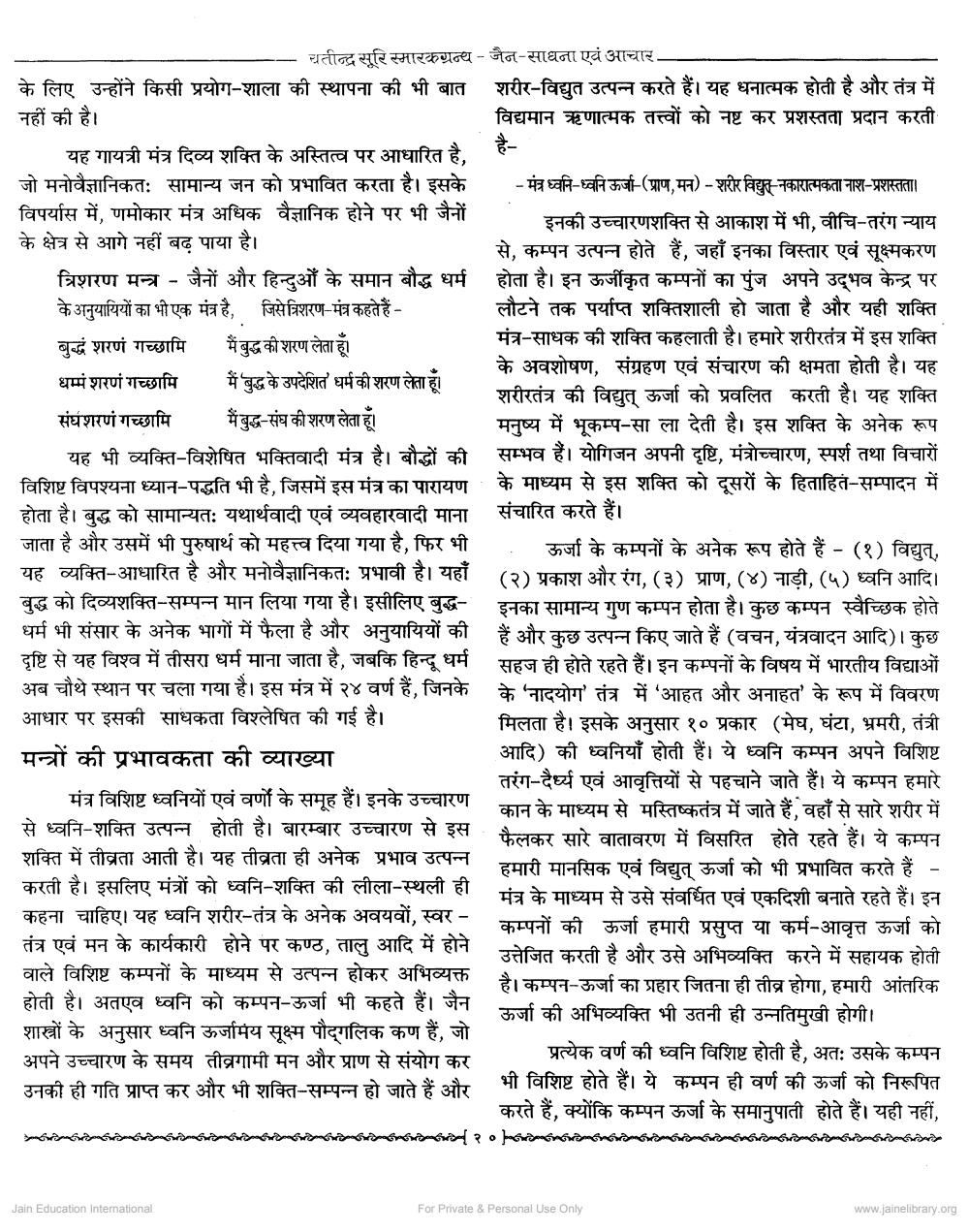________________
यतीन्द्र सूरि स्मारकग्रन्थ के लिए उन्होंने किसी प्रयोगशाला की स्थापना की भी बात नहीं की है।
यह गायत्री मंत्र दिव्य शक्ति के अस्तित्व पर आधारित है, जो मनोवैज्ञानिकतः सामान्य जन को प्रभावित करता है। इसके विपर्यास में, णमोकार मंत्र अधिक वैज्ञानिक होने पर भी जैनों के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाया है।
- मंत्र ध्वनि-ध्वनि ऊर्जा- (प्राण, मन ) - शरीर विद्युत्-नकारात्मकता नाश-प्रशस्तता।
इनकी उच्चारणशक्ति से आकाश में भी, वीचि - तरंग न्याय से, कम्पन उत्पन्न होते हैं, जहाँ इनका विस्तार एवं सूक्ष्मकरण त्रिशरण मन्त्र जैनों और हिन्दुओं के समान बौद्ध धर्म होता है। इन ऊर्जीकृत कम्पनों का पुंज अपने उद्भव केन्द्र पर अनुयायियों का भी एक मंत्र है, जिसे त्रिशरण- मंत्र कहते हैं
बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघशरणं गच्छामि
लौटने तक पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता है और यही शक्ति मंत्र-साधक की शक्ति कहलाती है । हमारे शरीरतंत्र में इस शक्ति के अवशोषण, संग्रहण एवं संचारण की क्षमता होती है। यह शरीरतंत्र की विद्युत् ऊर्जा को प्रवलित करती है। यह शक्ति मनुष्य में भूकम्प - सा ला देती है। इस शक्ति के अनेक रूप सम्भव हैं। योगिजन अपनी दृष्टि, मंत्रोच्चारण, स्पर्श तथा विचारों के माध्यम से इस शक्ति को दूसरों के हिताहित-सम्पादन में संचारित करते हैं।
बुद्ध-संघ की शरण लेता हूँ।
यह भी व्यक्ति विशेषित भक्तिवादी मंत्र है। बौद्धों की विशिष्ट विपश्यना ध्यान पद्धति भी है, जिसमें इस मंत्र का पारायण होता है। बुद्ध को सामान्यतः यथार्थवादी एवं व्यवहारवादी माना जाता है और उसमें भी पुरुषार्थ को महत्त्व दिया गया है, फिर भी यह व्यक्ति - आधारित है और मनोवैज्ञानिकतः प्रभावी है। यहाँ बुद्ध को दिव्यशक्ति-सम्पन्न मान लिया गया है। इसीलिए बुद्धधर्म भी संसार के अनेक भागों में फैला है और अनुयायियों की दृष्टि से यह विश्व में तीसरा धर्म माना जाता है, जबकि हिन्दू धर्म अब चौथे स्थान पर चला गया है। इस मंत्र में २४ वर्ण हैं, जिनके आधार पर इसकी साधकता विश्लेषित की गई है। मन्त्रों की प्रभावकता की व्याख्या
मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ।
मैं 'बुद्ध के उपदेशित' धर्म की शरण लेता हूँ।
मंत्र विशिष्ट ध्वनियों एवं वर्णों के समूह हैं। इनके उच्चारण से ध्वनि-शक्ति उत्पन्न होती है। बारम्बार उच्चारण से इस शक्ति में तीव्रता आती है। यह तीव्रता ही अनेक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसलिए मंत्रों को ध्वनि-शक्ति की लीला-स्थली ही कहना चाहिए। यह ध्वनि शरीर-तंत्र के अनेक अवयवों, स्वर - तंत्र एवं मन के कार्यकारी होने पर कण्ठ, तालु आदि में होने वाले विशिष्ट कम्पनों के माध्यम से उत्पन्न होकर अभिव्यक्त होती है। अतएव ध्वनि को कम्पन- ऊर्जा भी कहते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार ध्वनि ऊर्जामय सूक्ष्म पौद्गलिक कण हैं, जो अपने उच्चारण के समय तीव्रगामी मन और प्राण से संयोग कर उनकी ही गति प्राप्त कर और भी शक्ति-सम्पन्न हो जाते हैं और
Jain Education International
जैन-साधना एवं आचार.
शरीर-विद्युत उत्पन्न करते हैं। यह धनात्मक होती है और तंत्र में विद्यमान ऋणात्मक तत्त्वों को नष्ट कर प्रशस्तता प्रदान करती
मिले की कम ট{२०
ऊर्जा के कम्पनों के अनेक रूप होते हैं- (१) विद्युत्, (२) प्रकाश और रंग, (३) प्राण, (४) नाड़ी, (५) ध्वनि आदि। इनका सामान्य गुण कम्पन होता है। कुछ कम्पन स्वैच्छिक होते हैं और कुछ उत्पन्न किए जाते हैं (वचन, यंत्रवादन आदि) । कुछ सहज ही होते रहते हैं। इन कम्पनों के विषय में भारतीय विद्याओं के 'नादयोग' तंत्र में 'आहत और अनाहत' के रूप में विवरण मिलता है। इसके अनुसार १० प्रकार (मेघ, घंटा, भ्रमरी, तंत्री आदि) की ध्वनियाँ होती हैं। ये ध्वनि कम्पन अपने विशिष्ट तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्तियों से पहचाने जाते हैं। ये कम्पन हमारे कान के माध्यम से मस्तिष्कतंत्र में जाते हैं, वहाँ से सारे शरीर में फैलकर सारे वातावरण में विसरित होते रहते हैं। ये कम्पन हमारी मानसिक एवं विद्युत् ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। मंत्र के माध्यम से उसे संवर्धित एवं एकदिशी बनाते रहते हैं। इन कम्पनों की ऊर्जा हमारी प्रसुप्त या कर्म - आवृत्त ऊर्जा को उत्तेजित करती है और उसे अभिव्यक्ति करने में सहायक होती है। कम्पन- ऊर्जा का प्रहार जितना ही तीव्र होगा, हमारी आंतरिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति भी उतनी ही उन्नतिमुखी होगी।
प्रत्येक वर्ण की ध्वनि विशिष्ट होती है, अतः उसके कम्पन भी विशिष्ट होते हैं। ये कम्पन ही वर्ण की ऊर्जा को निरूपित करते हैं, क्योंकि कम्पन ऊर्जा के समानुपाती होते हैं। यही नहीं,
For Private Personal Use Only
www.jainelibrary.org