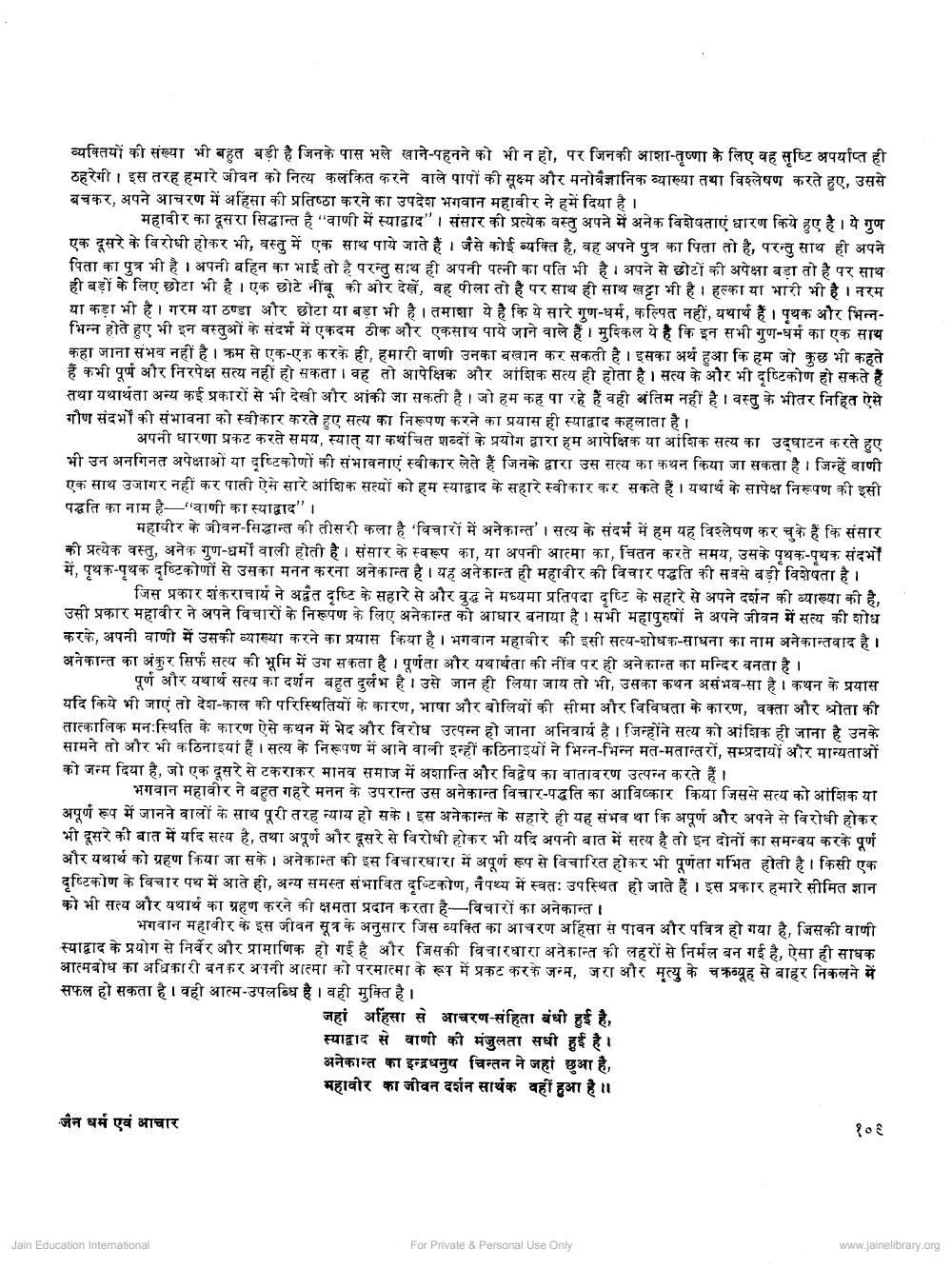________________ व्यक्तियों की संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके पास भले खाने-पहनने को भी न हो, पर जिनकी आशा-तृष्णा के लिए वह सृष्टि अपर्याप्त ही ठहरेगी। इस तरह हमारे जीवन को नित्य कलंकित करने वाले पापों की सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक व्याख्या तथा विश्लेषण करते हुए, उससे बचकर, अपने आचरण में अहिंसा की प्रतिष्ठा करने का उपदेश भगवान महावीर ने हमें दिया है। महावीर का दूसरा सिद्धान्त है "वाणी में स्याद्वाद" / संसार की प्रत्येक वस्तु अपने में अनेक विशेषताएं धारण किये हुए है। ये गुण एक दूसरे के विरोधी होकर भी, वस्तु में एक साथ पाये जाते हैं / जैसे कोई व्यक्ति है, वह अपने पुत्र का पिता तो है, परन्तु साथ ही अपने पिता का पुत्र भी है / अपनी बहिन का भाई तो है परन्तु साथ ही अपनी पत्नी का पति भी है। अपने से छोटों की अपेक्षा बड़ा तो है पर साथ ही बड़ों के लिए छोटा भी है / एक छोटे नींबू की ओर देखें, वह पीला तो है पर साथ ही साथ खट्टा भी है। हल्का या भारी भी है / नरम भिन्न होते हुए भी इन वस्तुओं के संदर्भ में एकदम ठीक और एकसाथ पाये जाने वाले हैं / मुश्किल ये है कि इन सभी गुण-धर्म का एक साथ कहा जाना संभव नहीं है। क्रम से एक-एक करके ही, हमारी वाणी उनका बखान कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि हम जो कुछ भी कहते हैं कभी पूर्ण और निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता। वह तो आपेक्षिक और आंशिक सत्य ही होता है। सत्य के और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं तथा यथार्थता अन्य कई प्रकारों से भी देखी और आंकी जा सकती है। जो हम कह पा रहे हैं वही अंतिम नहीं है। वस्तु के भीतर निहित ऐसे गौण संदर्भो की संभावना को स्वीकार करते हुए सत्य का निरूपण करने का प्रयास ही स्याद्वाद कहलाता है। अपनी धारणा प्रकट करते समय, स्यात् या कथंचित शब्दों के प्रयोग द्वारा हम आपेक्षिक या आंशिक सत्य का उद्घाटन करते हुए भी उन अनगिनत अपेक्षाओं या दृष्टिकोणों की संभावनाएं स्वीकार लेते हैं जिनके द्वारा उस सत्य का कथन किया जा सकता है। जिन्हें वाणी एक साथ उजागर नहीं कर पाती ऐसे सारे आंशिक सत्यों को हम स्याद्वाद के सहारे स्वीकार कर सकते हैं / यथार्थ के सापेक्ष निरूपण की इसी पद्धति का नाम है—'वाणी का स्याद्वाद" / महावीर के जीवन-सिद्धान्त की तीसरी कला है 'विचारों में अनेकान्त' / सत्य के संदर्भ में हम यह विश्लेषण कर चुके हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु, अनेक गुण-धर्मों वाली होती है। संसार के स्वरूप का, या अपनी आत्मा का, चितन करते समय, उसके पृथक-पृथक संदों में, पृथक-पृथक दृष्टिकोणों से उसका मनन करना अनेकान्त है। यह अनेकान्त ही महावीर की विचार पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। जिस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैत दृष्टि के सहारे से और बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा दृष्टि के सहारे से अपने दर्शन की व्याख्या की है, उसी प्रकार महावीर ने अपने विचारों के निरूपण के लिए अनेकान्त को आधार बनाया है। सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्य की शोध करके, अपनी वाणी में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। भगवान महावीर की इसी सत्य-शोधक-साधना का नाम अनेकान्तवाद है। अनेकान्त का अंकुर सिर्फ सत्य की भूमि में उग सकता है। पूर्णता और यथार्थता की नींव पर ही अनेकान्त का मन्दिर बनता है। पूर्ण और यथार्थ सत्य का दर्शन बहत दुर्लभ है। उसे जान ही लिया जाय तो भी, उसका कथन असंभव-सा है। कथन के प्रयास यदि किये भी जाएं तो देश-काल की परिस्थितियों के कारण, भाषा और बोलियों की सीमा और विविधता के कारण, वक्ता और श्रोता की तात्कालिक मनःस्थिति के कारण ऐसे कथन में भेद और विरोध उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है। जिन्होंने सत्य को आंशिक ही जाना है उनके सामने तो और भी कठिनाइयां हैं / सत्य के निरूपण में आने वाली इन्हीं कठिनाइयों ने भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों, सम्प्रदायों और मान्यताओं को जन्म दिया है, जो एक दूसरे से टकराकर मानव समाज में अशान्ति और विद्वेष का वातावरण उत्पन्न करते हैं।। भगवान महावीर ने बहत गहरे मनन के उपरान्त उस अनेकान्त विचार-पद्धति का आविष्कार किया जिससे सत्य को आंशिक या अपूर्ण रूप में जानने वालों के साथ पूरी तरह न्याय हो सके। इस अनेकान्त के सहारे ही यह संभव था कि अपूर्ण और अपने से विरोधी होकर भी दूसरे की बात में यदि सत्य है, तथा अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि अपनी बात में सत्य है तो इन दोनों का समन्वय करके पूर्ण और यथार्थ को ग्रहण किया जा सके। अनेकान्त की इस विचारधारा में अपूर्ण रूप से विचारित होकर भी पूर्णता गभित होती है। किसी एक दृष्टिकोण के विचार पथ में आते ही, अन्य समस्त संभावित दृष्टिकोण, नैपथ्य में स्वतः उपस्थित हो जाते हैं / इस प्रकार हमारे सीमित ज्ञान को भी सत्य और यथार्थ का ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है—विचारों का अनेकान्त / भगवान महावीर के इस जीवन सूत्र के अनुसार जिस व्यक्ति का आचरण अहिंसा से पावन और पवित्र हो गया है, जिसकी वाणी स्याद्वाद के प्रयोग से निर्वैर और प्रामाणिक हो गई है और जिसकी विचारधारा अनेकान्त की लहरों से निर्मल बन गई है, ऐसा ही साधक आत्मबोध का अधिकारी बनकर अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रकट करके जन्म, जरा और मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सफल हो सकता है / वही आत्म-उपलब्धि है / वही मुक्ति है। जहां अहिंसा से आचरण-संहिता बंधी हुई है, स्याद्वाद से वाणी को मंजुलता सधी हुई है। अनेकान्त का इन्द्रधनुष चिन्तन ने जहां छुआ है, महावीर का जीवन दर्शन सार्थक वहीं हुआ है। जैन धर्म एवं आचार Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org