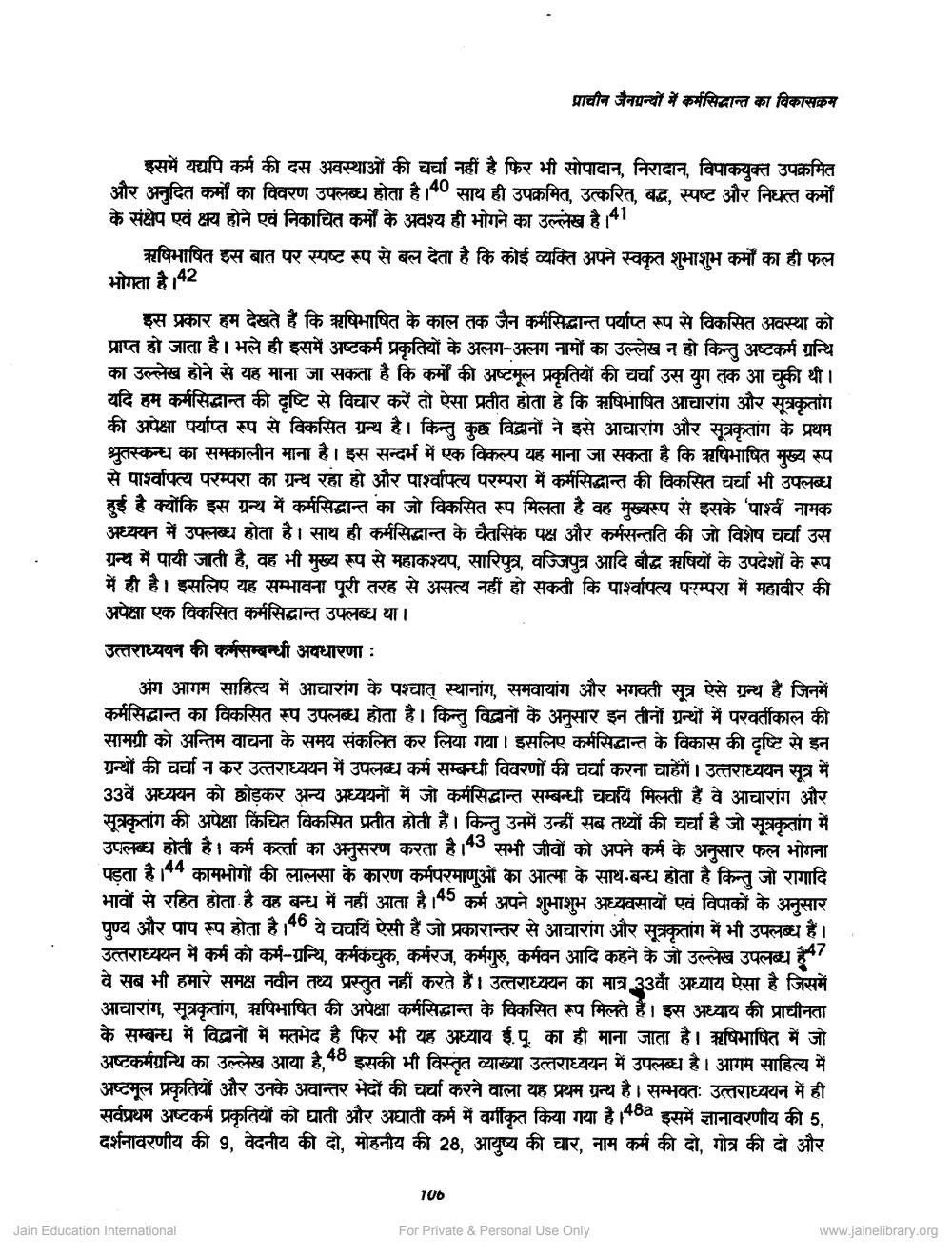________________
इसमें यद्यपि कर्म की दस अवस्थाओं की चर्चा नहीं है फिर भी सोपादान, निरादान, विपाकयुक्त उपक्रमित और अनुदित कर्मों का विवरण उपलब्ध होता है। 40 साथ ही उपक्रमित, उत्करित, बद्ध, स्पष्ट और निधत्त कर्मों के संक्षेप एवं क्षय होने एवं निकाचित कर्मों के अवश्य ही भोगने का उल्लेख है। 41
प्राचीन जैनग्रन्थों में कर्मसिद्धान्त का विकासक्रम
ऋषिभाषित इस बात पर स्पष्ट रूप से बल देता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वकृत शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगता है। 42
इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋषिभाषित के काल तक जैन कर्मसिद्धान्त पर्याप्त रूप से विकसित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भले ही इसमें अष्टकर्म प्रकृतियों के अलग-अलग नामों का उल्लेख न हो किन्तु अष्टकर्म ग्रन्थि का उल्लेख होने से यह माना जा सकता है कि कर्मों की अष्टमूल प्रकृतियों की चर्चा उस युग तक आ चुकी थी । यदि हम कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता हे कि ऋषिभाषित आचारांग और सूत्रकृतांग की अपेक्षा पर्याप्त रूप से विकसित ग्रन्थ है। किन्तु कुछ विद्वानों ने इसे आचारांग और सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का समकालीन माना है। इस सन्दर्भ में एक विकल्प यह माना जा सकता है कि ऋषिभाषित मुख्य रूप से पार्श्वपत्य परम्परा का ग्रन्थ रहा हो और पार्श्वपत्य परम्परा में कर्मसिद्धान्त की विकसित चर्चा भी उपलब्ध हुई है क्योंकि इस ग्रन्थ में कर्मसिद्धान्त का जो विकसित रूप मिलता है वह मुख्यरूप से इसके 'पार्श्वं नामक अध्ययन में उपलब्ध होता है। साथ ही कर्मसिद्धान्त के चैतसिक पक्ष और कर्मसन्तति की जो विशेष चर्चा उस ग्रन्थ में पायी जाती है, वह भी मुख्य रूप से महाकश्यप सारिपुत्र, वज्जिपुत्र आदि बौद्ध ऋषियों के उपदेशों के रूप में ही है। इसलिए यह सम्भावना पूरी तरह से असत्य नहीं हो सकती कि पार्श्वपत्य परम्परा में महावीर की अपेक्षा एक विकसित कर्मसिद्धान्त उपलब्ध था ।
उत्तराध्ययन की कर्मसम्बन्धी अवधारणा :
अंग आगम साहित्य में आचारांग के पश्चात् स्थानांग, समवायांग और भगवती सूत्र ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें कर्मसिद्धान्त का विकसित रूप उपलब्ध होता है। किन्तु विद्वानों के अनुसार इन तीनों ग्रन्थों में परवर्तीकाल की सामग्री को अन्तिम वाचना के समय संकलित कर लिया गया। इसलिए कर्मसिद्धान्त के विकास की दृष्टि से इन ग्रन्थों की चर्चा न कर उत्तराध्ययन में उपलब्ध कर्म सम्बन्धी विवरणों की चर्चा करना चाहेंगें। उत्तराध्ययन सूत्र में 33वें अध्ययन को छोड़कर अन्य अध्ययनों में जो कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी चर्चायें मिलती हैं वे आचारांग और सूत्रकृतांग की अपेक्षा किंचित विकसित प्रतीत होती हैं। किन्तु उनमें उन्हीं सब तथ्यों की चर्चा है जो सूत्रकृतांग में उपलब्ध होती है। कर्म कर्त्ता का अनुसरण करता है। 43 सभी जीवों को अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है 44 कामभोगों की लालसा के कारण कर्मपरमाणुओं का आत्मा के साथ-बन्ध होता है किन्तु जो रागादि भावों से रहित होता है वह बन्ध में नहीं आता है। 45 कर्म अपने शुभाशुभ अध्यवसायों एवं विपाकों के अनुसार पुण्य और पाप रूप होता है 46 ये चर्चायें ऐसी हैं जो प्रकारान्तर से आचारांग और सूत्रकृतांग में भी उपलब्ध हैं। उत्तराध्ययन में कर्म को कर्म-ग्रन्थि, कर्मकंचुक, कर्मरज, कर्मगुरु, कर्मवन आदि कहने के जो उल्लेख उपलब्ध है47 वे सब भी हमारे समक्ष नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। उत्तराध्ययन का मात्र 33वाँ अध्याय ऐसा है जिसमें आचारांग, सूत्रकृतांग, ऋषिभाषित की अपेक्षा कर्मसिद्धान्त के विकसित रूप मिलते हैं। इस अध्याय की प्राचीनता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है फिर भी यह अध्याय ई.पू. का ही माना जाता है। ऋषिभाषित में जो अष्टकर्मग्रन्थि का उल्लेख आया है, 48 इसकी भी विस्तृत व्याख्या उत्तराध्ययन में उपलब्ध है। आगम साहित्य में अष्टमूल प्रकृतियों और उनके अवान्तर भेदों की चर्चा करने वाला यह प्रथम ग्रन्थ है। सम्भवतः उत्तराध्ययन में ही सर्वप्रथम अष्टकर्म प्रकृतियों को घाती और अघाती कर्म में वर्गीकृत किया गया है। 48a इसमें ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की दो, मोहनीय की 28, आयुष्य की चार, नाम कर्म की दो, गोत्र की दो और
Jain Education International
106
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org