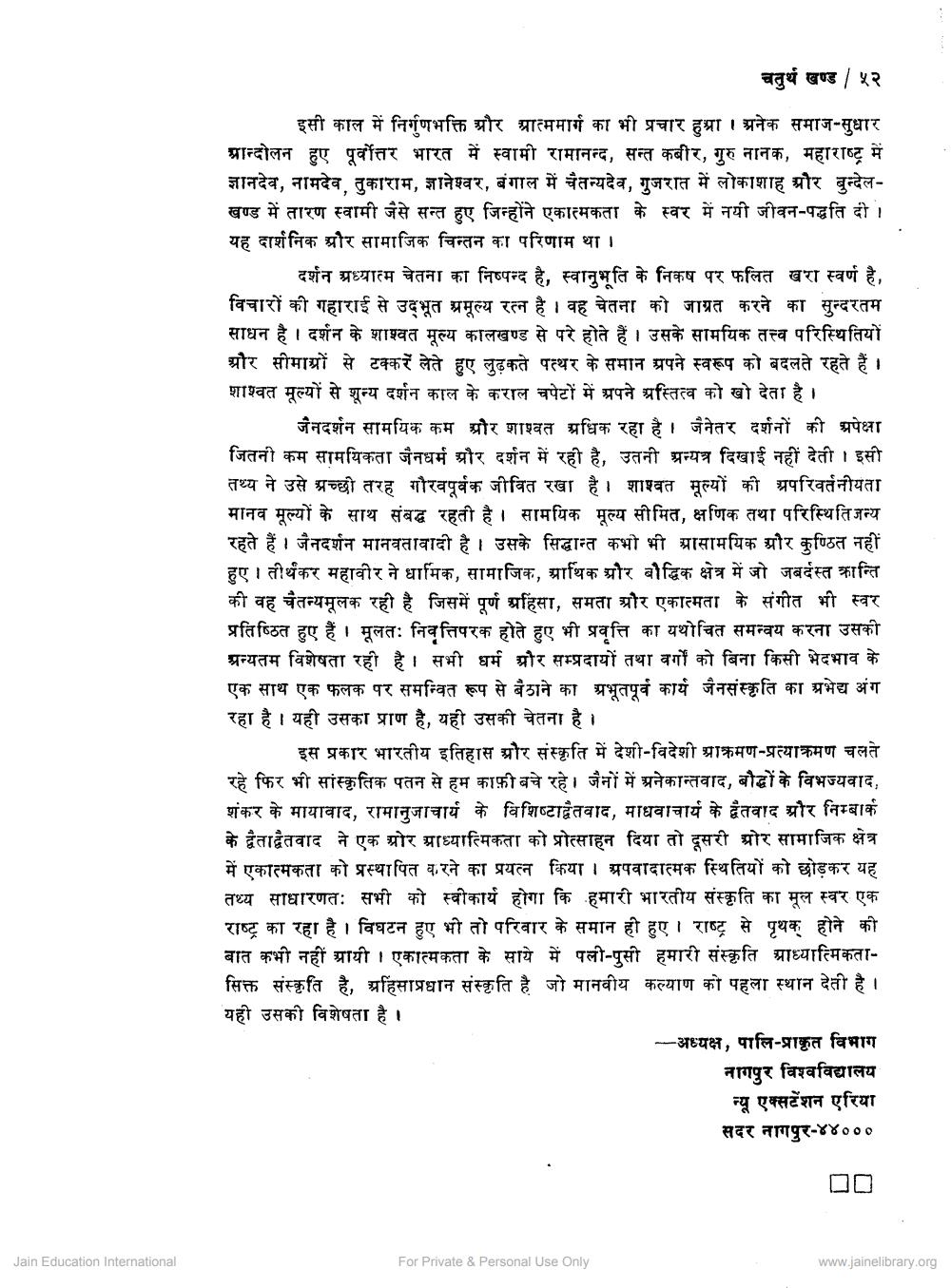________________ चतुर्थ खण्ड | 52 इसी काल में निर्गणभक्ति और प्रात्ममार्ग का भी प्रचार हा / अनेक समाज-सुधार आन्दोलन हुए पूर्वोत्तर भारत में स्वामी रामानन्द, सन्त कबीर, गुरु नानक, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव तुकाराम, ज्ञानेश्वर, बंगाल में चैतन्यदेव, गुजरात में लोकाशाह और बुन्देलखण्ड में तारण स्वामी जैसे सन्त हुए जिन्होंने एकात्मकता के स्वर में नयी जीवन-पद्धति दी। यह दार्शनिक और सामाजिक चिन्तन का परिणाम था। दर्शन अध्यात्म चेतना का निष्पन्द है, स्वानुभूति के निकष पर फलित खरा स्वर्ण है, विचारों की गहाराई से उदभूत अमूल्य रत्न है। वह चेतना को जाग्रत करने का सुन्दरतम साधन है / दर्शन के शाश्वत मूल्य कालखण्ड से परे होते हैं। उसके सामयिक तत्त्व परिस्थितियों और सीमाओं से टक्करें लेते हुए लुढ़कते पत्थर के समान अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। शाश्वत मूल्यों से शून्य दर्शन काल के कराल चपेटों में अपने अस्तित्व को खो देता है। जैनदर्शन सामयिक कम और शाश्वत अधिक रहा है। जैनेतर दर्शनों की अपेक्षा जितनी कम सामयिकता जैनधर्म और दर्शन में रही है, उतनी अन्यत्र दिखाई नहीं देती / इसी तथ्य ने उसे अच्छी तरह गौरवपूर्वक जीवित रखा है। शाश्वत मूल्यों की अपरिवर्तनीयता मानव मूल्यों के साथ संबद्ध रहती है। सामयिक मूल्य सीमित, क्षणिक तथा परिस्थितिजन्य रहते हैं। जैनदर्शन मानवतावादी है। उसके सिद्धान्त कभी भी प्रासामयिक और कुण्ठित नहीं हुए। तीर्थंकर महावीर ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षेत्र में जो जबर्दस्त क्रान्ति की वह चैतन्यमूलक रही है जिसमें पूर्ण अहिंसा, समता और एकात्मता के संगीत भी स्वर प्रतिष्ठित हुए हैं। मूलतः निवृत्तिपरक होते हुए भी प्रवत्ति का यथोचित समन्वय करना उसकी अन्यतम विशेषता रही है। सभी धर्म और सम्प्रदायों तथा वर्गों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक फलक पर समन्वित रूप से बैठाने का अभूतपूर्व कार्य जैनसंस्कृति का अभेद्य अंग रहा है। यही उसका प्राण है, यही उसकी चेतना है। इस प्रकार भारतीय इतिहास और संस्कृति में देशी-विदेशी आक्रमण-प्रत्याक्रमण चलते रहे फिर भी सांस्कृतिक पतन से हम काफ़ी बचे रहे। जैनों में अनेकान्तवाद, बौद्धों के विभज्यवाद, शंकर के मायावाद, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य के द्वैतवाद और निम्बार्क के द्वैताद्वैतवाद ने एक अोर आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन दिया तो दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में एकात्मकता को प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया। अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर यह तथ्य साधारणतः सभी को स्वीकार्य होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्वर एक राष्ट्र का रहा है / विघटन हुए भी तो परिवार के समान ही हुए / 'राष्ट्र से पृथक् होने की बात कभी नहीं पायी। एकात्मकता के साये में पली-पूसी हमारी संस्कृति आध्यात्मिकतासिक्त संस्कृति है, अहिंसाप्रधान संस्कृति है जो मानवीय कल्याण को पहला स्थान देती है। यही उसकी विशेषता है। -अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग नागपुर विश्वविद्यालय न्यू एक्सटेंशन एरिया सदर नागपुर-४४००० 00 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org