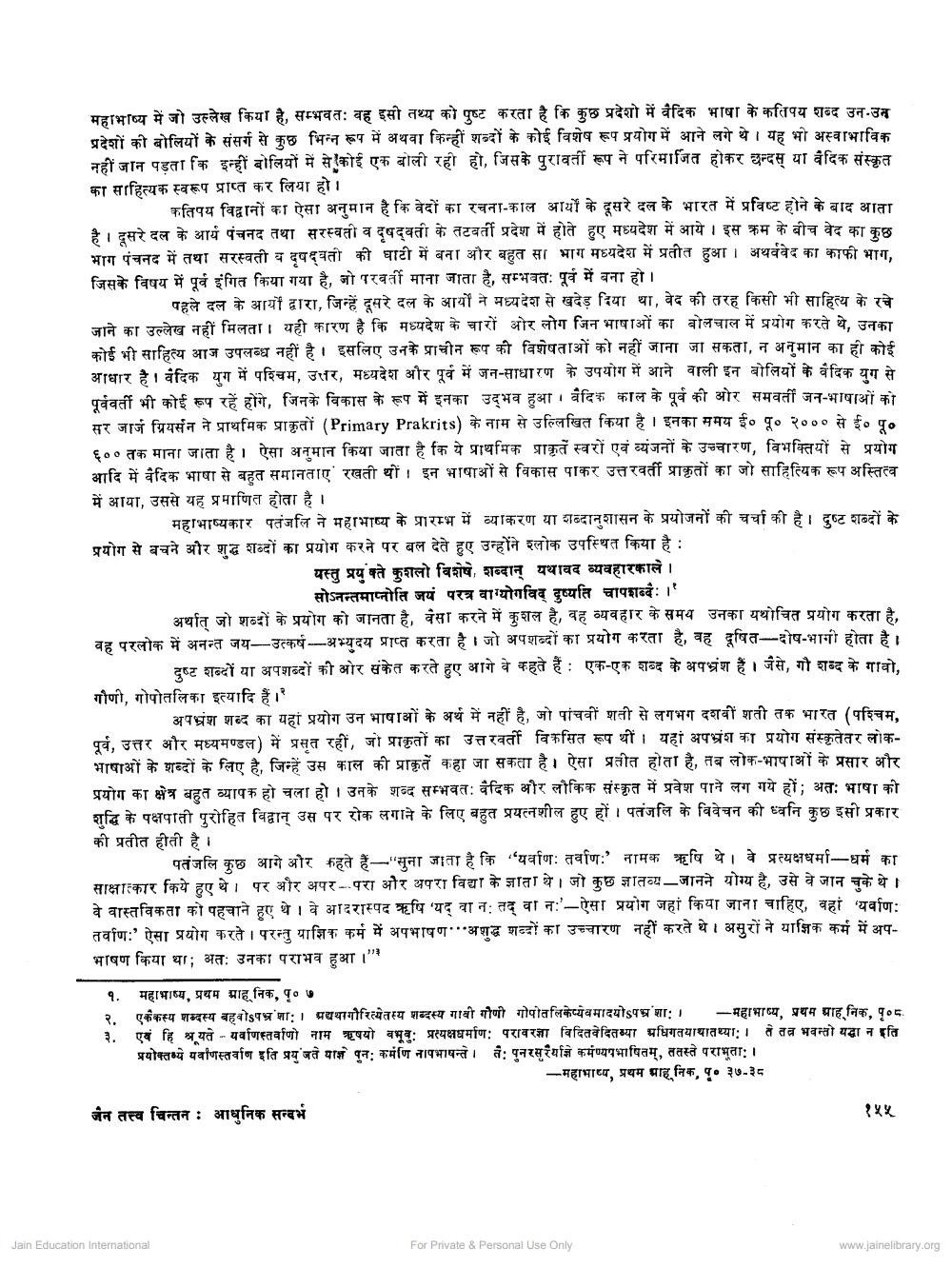________________
महाभाष्य में जो उल्लेख किया है, सम्भवतः बह इसी तथ्य को पुष्ट करता है कि कुछ प्रदेशो में वैदिक भाषा के कतिपय शब्द उन-उन प्रदेशों की बोलियों के संसर्ग से कुछ भिन्न रूप में अथवा किन्हीं शब्दों के कोई विशेष रूप प्रयोग में आने लगे थे। यह भी अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता कि इन्हीं बोलियों में से कोई एक बोली रही हो, जिसके पुरावर्ती रूप ने परिमाजित होकर छन्दस या वैदिक संस्कत का साहित्यक स्वरूप प्राप्त कर लिया हो।
कतिपय विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि वेदों का रचना-काल आर्यों के दूसरे दल के भारत में प्रविष्ट होने के बाद आता है। दूसरे दल के आर्य पंचनद तथा सरस्वती व दृषद्वती के तटवर्ती प्रदेश में होते हुए मध्यदेश में आये । इस क्रम के बीच वेद का कह भाग पंचनद में तथा सरस्वती व दृषद्वती की घाटी में बना और बहुत सा भाग मध्यदेश में प्रतीत हुआ। अथर्ववेद का काफी भाग, जिसके विषय में पूर्व इंगित किया गया है, जो परवर्ती माना जाता है, सम्भवतः पूर्व में बना हो ।
पहले दल के आर्यों द्वारा, जिन्हें दूसरे दल के आर्यों ने मध्यदेश से खदेड़ दिया था, वेद की तरह किसी भी साहित्य के रचे जाने का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि मध्यदेश के चारों ओर लोग जिन भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग करते थे, उनका कोई भी साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके प्राचीन रूप की विशेषताओं को नहीं जाना जा सकता, न अनुमान का ही कोई आधार है। वैदिक युग में पश्चिम, उत्सर, मध्यदेश और पूर्व में जन-साधारण के उपयोग में आने वाली इन बोलियों के वैदिक यग से पूर्ववर्ती भी कोई रूप रहें होंगे, जिनके विकास के रूप में इनका उद्भव हुआ। वैदिक काल के पूर्व की ओर समवर्ती जन-भाषाओं को सर जार्ज ग्रियर्सन ने प्राथमिक प्राकृतों (Primary Prakrits) के नाम से उल्लिखित किया है । इनका समय ई० पू० २००० से ई०पू० ६०० तक माना जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये प्राथमिक प्राकृतें स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण, विभक्तियों से प्रयोग आदि में वैदिक भाषा से बहुत समानताए रखती थीं। इन भाषाओं से विकास पाकर उत्तरवर्ती प्राकृतों का जो साहित्यिक रूप अस्तित्व में आया, उससे यह प्रमाणित होता है ।
महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में व्याकरण या शब्दानुशासन के प्रयोजनों की चर्चा की है। दुष्ट शब्दों के प्रयोग से बचने और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने पर बल देते हुए उन्होंने श्लोक उपस्थित किया है :
यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे, शब्दान् यथावद व्यवहारकाले ।
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः ।' अर्थात् जो शब्दों के प्रयोग को जानता है, वैसा करने में कुशल है, वह व्यवहार के समय उनका यथोचित प्रयोग करता है, वह परलोक में अनन्त जय-उत्कर्ष-अभ्युदय प्राप्त करता है । जो अपशब्दों का प्रयोग करता है, वह दूषित-दोष-भागी होता है।
दुष्ट शब्दों या अपशब्दों की ओर संकेत करते हुए आगे वे कहते हैं : एक-एक शब्द के अपभ्रंश हैं। जैसे, गौ शब्द के गावो. गौणी, गोपोतलिका इत्यादि हैं।
अपभ्रंश शब्द का यहां प्रयोग उन भाषाओं के अर्थ में नहीं है, जो पांचवीं शती से लगभग दशवीं शती तक भारत (पश्चिम, पूर्व, उत्तर और मध्यमण्डल) में प्रसत रहीं, जो प्राकृतों का उत्तरवर्ती विकसित रूप थीं। यहां अपभ्रंश का प्रयोग संस्कृतेतर लोकभाषाओं के शब्दों के लिए है, जिन्हें उस काल की प्राकृतें कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, तब लोक-भाषाओं के प्रसार और प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चला हो । उनके शब्द सम्भवत: वैदिक और लौकिक संस्कृत में प्रवेश पाने लग गये हों; अत: भाषा की शुद्धि के पक्षपाती पुरोहित विद्वान् उस पर रोक लगाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हुए हों। पतंजलि के विवेचन की ध्वनि कुछ इसी प्रकार की प्रतीत होती है।
पतंजलि कुछ आगे और कहते हैं-"सुना जाता है कि “यर्वाण: तर्वाण:' नामक ऋषि थे। वे प्रत्यक्षधर्मा-धर्म का साक्षात्कार किये हुए थे। पर और अपर-परा और अपरा विद्या के ज्ञाता थे। जो कुछ ज्ञातव्य – जानने योग्य है, उसे वे जान चके थे। वे वास्तविकता को पहचाने हुए थे। वे आदरास्पद ऋषि 'यद् वा न: तद् वा नः'-ऐसा प्रयोग जहां किया जाना चाहिए, वहां यर्वाणः तर्वाणः' ऐसा प्रयोग करते । परन्तु याज्ञिक कर्म में अपभाषण 'अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं करते थे। असुरों ने याज्ञिक कर्म में अपभाषण किया था; अत: उनका पराभव हुआ।"
१. महाभाध्य, प्रथम प्राह निक, १०७ २. एकैकस्य शब्दस्य बहवोऽपभ्रशाः। प्रद्यथागोरित्येतस्य शब्दस्य गावी गौणी गोपोतलिकेप्येवमादयोऽपभ्रशाः। -महाभाष्य, प्रथम प्राह निक, ५०६ ३. एवं हि श्रयते - यणिस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवः प्रत्यक्षधर्माणः परावरज्ञा विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्याः। ते तत्र भवन्तो यद्धा न इति प्रयोक्तव्ये याणस्तर्वाण इति प्रयुजते याने पुनः कर्मणि नापभाषन्ते। तैः पुनरसुरैयज्ञि कर्मण्यपभाषितम्, ततस्ते पराभूताः।
-महाभाध्य, प्रथम माह निक,पृ. ३७.३८
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक सन्दर्भ
१५५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org