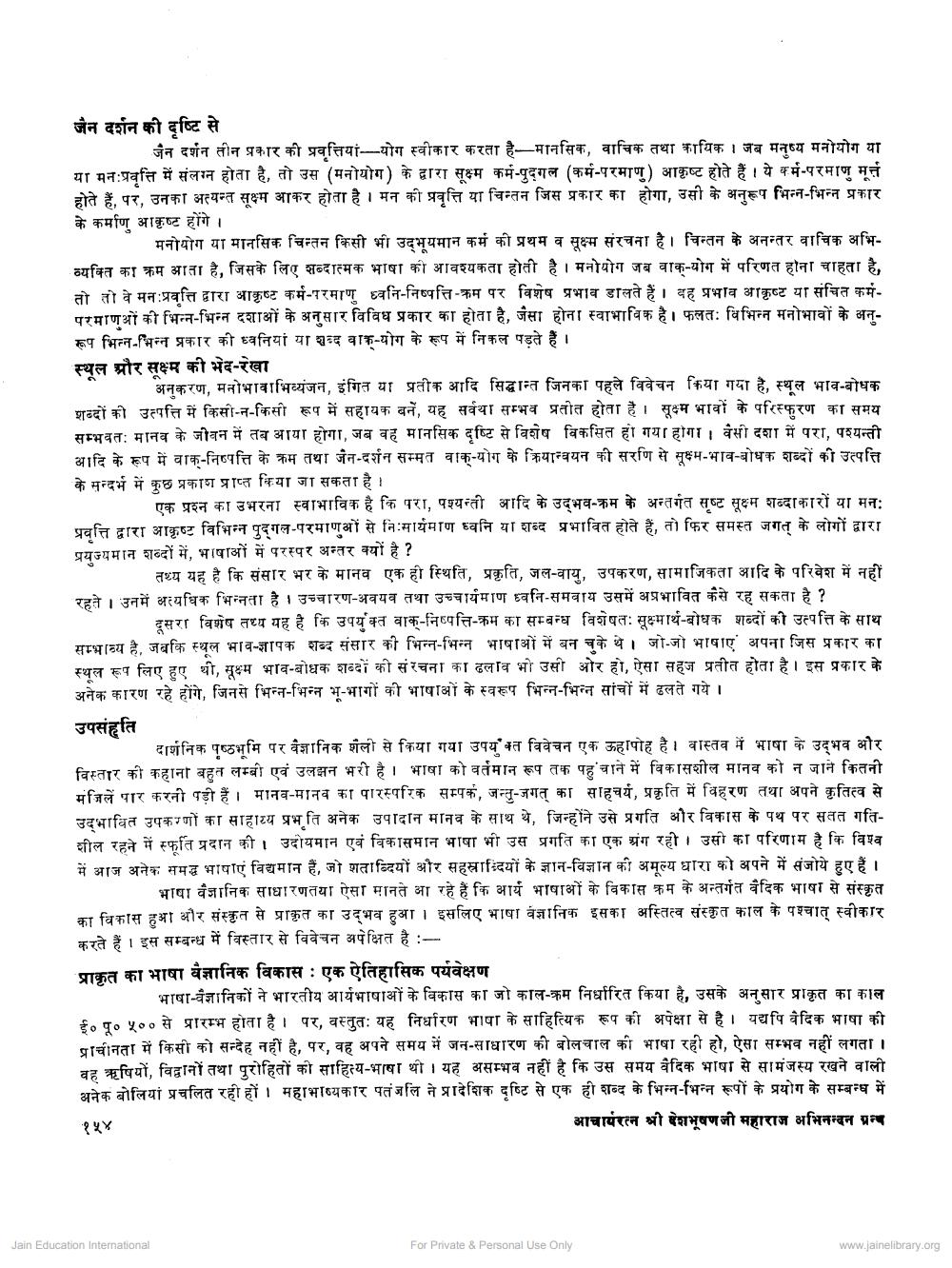________________
जैन दर्शन की दृष्टि से
।
जैन दर्शन तीन प्रकार की प्रवृत्तियां - योग स्वीकार करता है-मानसिक, वाचिक तथा कायिक । जब मनुष्य मनोयोग या या प्रवृत्ति में संलग्न होता है, तो उस (मनोयोग) के द्वारा सूक्ष्म कर्म-पुद्गल (कर्म-परमाणु आकृष्ट होते हैं ये धर्म-परमाणु मूर्त होते हैं, पर उनका अत्यन्त सूक्ष्म आकर होता है। मन की प्रवृत्ति या चिन्तन जिस प्रकार का होगा, उसी के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्माणु आकृष्ट होंगे ।
मनोयोग या मानसिक चिन्तन किसी भी उद्भूयमान कर्म की प्रथम व सूक्ष्म संरचना है। चिन्तन के अनन्तर वाचिक अभिव्यक्ति का क्रम आता है, जिसके लिए शब्दात्मक भाषा की आवश्यकता होती है। मनोयोग जब वाक्-योग में परिणत होना चाहता है, तो तो वे मनः प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट कर्म-परमाणु ध्वनि- निष्पत्ति क्रम पर विशेष प्रभाव डालते हैं । दह प्रभाव आकृष्ट या संचित कर्मपरमाणुओं की भिन्न-भिन्न दशाओं के अनुसार विविध प्रकार का होता है, जैसा होना स्वाभाविक है । फलतः विभिन्न मनोभावों के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियां या शब्द वाक्-योग के रूप में निकल पड़ते हैं ।
स्थूल और सूक्ष्म की भेद-रेखा
अनुकरण, मनोभावाभिव्यंजन इंगित मा प्रतीक आदि सिद्धान्त जिनका पहले विवेचन किया गया है, स्थूल भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति में किसी-न-किसी रूप में सहायक बनें, यह सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है। सूक्ष्म भावों के परिस्फुरण का समय सम्भवतः मानव के जीवन में तब आया होगा, जब वह मानसिक दृष्टि से विशेष विकसित हो गया होगा। वैसी दशा में परा, पश्यन्ती आदि के रूप में वाक्- निष्पत्ति के क्रम तथा जैन दर्शन सम्मत वाक्-योग के क्रियान्वयन की सरणि से सूक्ष्म-भाव-बोधक शब्दों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में कुछ प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है।
एक प्रश्न का उभरना स्वाभाविक है कि परा, पश्यन्ती आदि के उद्भव क्रम के अन्तर्गत सृष्ट सूक्ष्म शब्दाकारों या मनः प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट विभिन्न पुद्गल परमाणुओं से निःसार्यमाण ध्वनि या शब्द प्रभावित होते हैं, तो फिर समस्त जगत् के लोगों द्वारा प्रयुज्यमान शब्दों में, भाषाओं में परस्पर अन्तर क्यों है ?
तथ्य यह है कि संसार भर के मानव एक ही स्थिति, प्रकृति, जल-वायु, उपकरण, सामाजिकता आदि के परिवेश में नहीं रहते। उनमें अत्यधिक भिन्नता है। उच्चारण-अवयव तथा उच्चार्यमाण ध्वनि समवाय उसमें अप्रभावित कैसे रह सकता है ? दूसरा विशेष तथ्य यह है कि उपर्युक्त वाक्-निष्पत्ति क्रम का सम्बन्ध विशेषतः सूक्ष्मार्थ-बोधक शब्दों की उत्पत्ति के साथ सम्भाव्य है, जबकि स्थूल भाव ज्ञापक शब्द संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं में बन चुके थे । जो-जो भाषाएं अपना जिस प्रकार का स्थूल रूप लिए हुए थी, सूक्ष्म भाव-बोधक शब्दों की संरचना का ढलाव भी उसी ओर हो, ऐसा सहज प्रतीत होता है । इस प्रकार के अनेक कारण रहे होंगे, जिनसे भिन्न-भिन्न भू-भागों की भाषाओं के स्वरूप भिन्न-भिन्न सांचों में ढलते गये ।
उपसंहृति
दार्शनिक पृष्ठभूमि पर वैज्ञानिक शैली से किया गया उपयुक्त विवेचन एक ऊहापोह है । वास्तव में भाषा के उद्भव और विस्तार की कहानी बहुत लम्बी एवं उलझन भरी है। भाषा को वर्तमान रूप तक पहुंचाने में विकासशील मानव को न जाने कितनी मंजिलें पार करनी पड़ी हैं। मानव-मानव का पारस्परिक सम्पर्क, जन्तु जगत् का साहचर्य, प्रकृति में विहरण तथा अपने कृतित्व से उद्भावित उपकरणों का साहाय्य प्रभृति अनेक उपादान मानव के साथ थे, जिन्होंने उसे प्रगति और विकास के पथ पर सतत गतिशील रहने में स्फूर्ति प्रदान की । उदोयमान एवं विकासमान भाषा भी उस प्रगति का एक अंग रही। उसी का परिणाम है कि विश्व में आज अनेक समद्ध भाषाएं विद्यमान हैं, जो शताब्दियों और सहस्राब्दियों के ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य धारा को अपने में संजोये हुए हैं । भाषा वैज्ञानिक साधारणतया ऐसा मानते आ रहे हैं कि आर्य भाषाओं के विकास क्रम के अन्तर्गत वैदिक भाषा से संस्कृत का विकास हुआ और संस्कृत से प्राकृत का उद्भव हुआ । इसलिए भाषा वैज्ञानिक इसका अस्तित्व संस्कृत काल के पश्चात् स्वीकार करते हैं । इस सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन अपेक्षित है :
प्राकृत का भाषा वैज्ञानिक विकास एक ऐतिहासिक पर्यवेक्षण
भाषा-वैज्ञानिकों ने भारतीय आर्यभाषाओं के विकास का जो काल क्रम निर्धारित किया है, उसके अनुसार प्राकृत का काल ई० पू० ५०० से प्रारम्भ होता है। पर, वस्तुतः यह निर्धारण भाषा के साहित्यिक रूप की अपेक्षा से है । यद्यपि वैदिक भाषा की प्राचीनता में किसी को सन्देह नहीं है, पर, वह अपने समय में जन साधारण की बोलचाल की भाषा रही हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता । वह ऋषियों, विद्वानों तथा पुरोहितों की साहित्य-भाषा थी । यह असम्भव नहीं है कि उस समय वैदिक भाषा से सामंजस्य रखने वाली अनेक बोलियां प्रचलित रही हों । महाभाष्यकार पतंजलि ने प्रादेशिक दृष्टि से एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न रूपों के प्रयोग के सम्बन्ध में
१५४
आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org