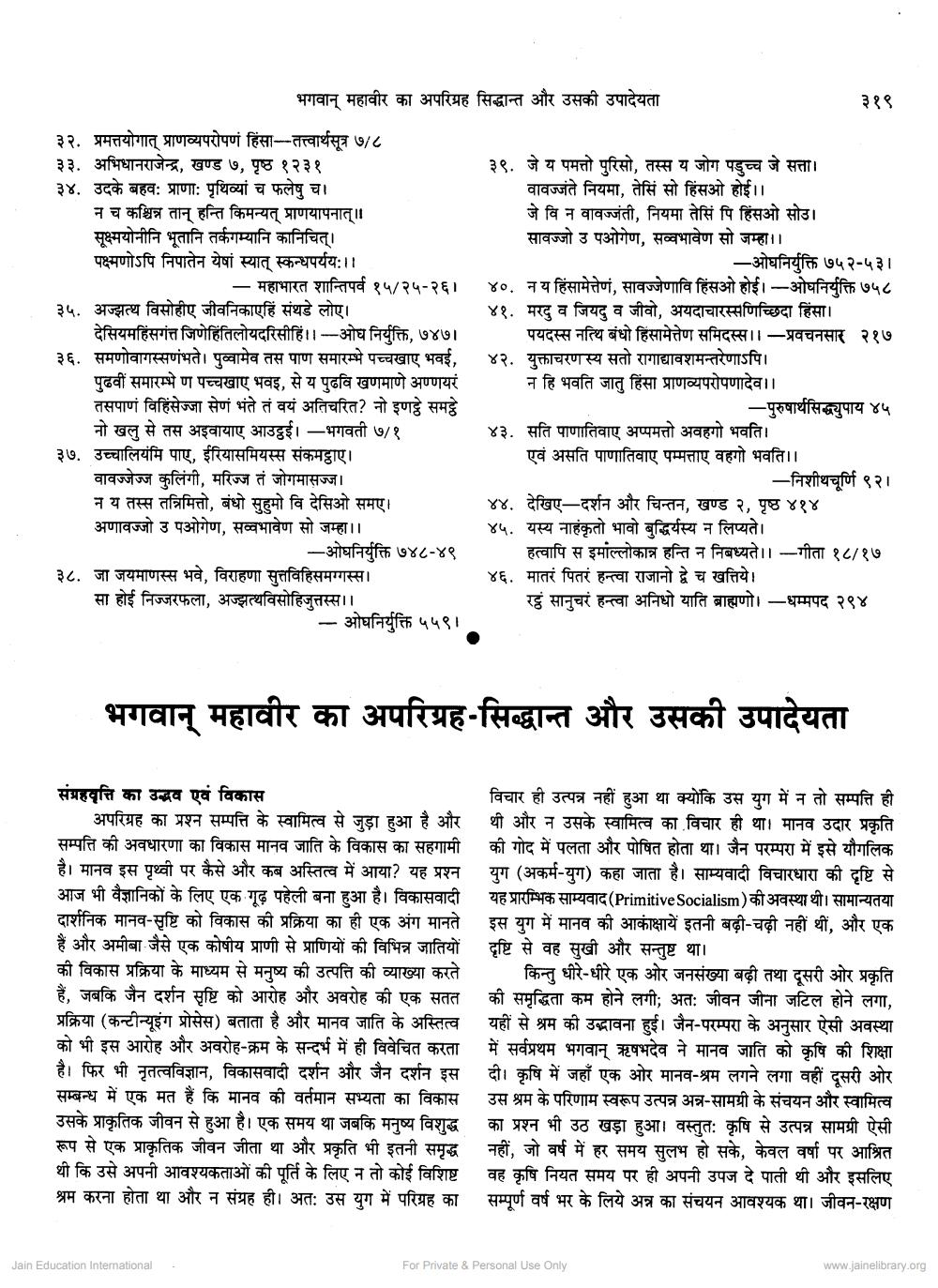________________ भगवान् महावीर का अपरिग्रह सिद्धान्त और उसकी उपादेयता 319 32. प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा-तत्त्वार्थसूत्र 7/8 33. अभिधानराजेन्द्र, खण्ड 7, पृष्ठ 1231 39. जे य पमत्तो पुरिसो, तस्स य जोग पडुच्च जे सत्ता। 34. उदके बहवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च। वावज्जते नियमा, तेसिं सो हिंसओ होई।।। न च कश्चिन्न तान् हन्ति किमन्यत् प्राणयापनात्। जे वि न वावज्जंती, नियमा तेसिं पि हिंसओ सोउ। सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्। सावज्जो उ पओगेण, सव्वभावेण सो जम्हा।। पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात् स्कन्धपर्ययः।। -ओघनियुक्ति 752-53 / - महाभारत शान्तिपर्व 15/25-26 / 40. न य हिंसामेत्तेणं, सावज्जेणावि हिंसओ होई। -ओघनियुक्ति 758 35. अज्झत्थ विसोहीए जीवनिकाएहिं संथडे लोए। 41. मरदु व जियदु व जीवो, अयदाचारस्सणिच्छिदा हिंसा। देसियमहिंसगंत्त जिणेहिंतिलोयदरिसीहिं।। -ओघ नियुक्ति, 747 / पयदस्स नत्थि बंधो हिसामेत्तेण समिदस्स।। -प्रवचनसार 217 36. समणोवागस्सणंभते। पुव्वामेव तस पाण समारम्भे पच्चखाए भवई, 42. युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावशमन्तरेणाऽपि। पुढवी समारम्भेण पच्चखाए भवइ, से य पुढवि खणमाणे अण्णयरं न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव।। तसपाणं विहिंसेज्जा सेणं भंते तं वयं अतिचरित? नो इणढे समढे -पुरुषार्थसिद्ध्युपाय 45 नो खलु से तस अइवायाए आउट्ठई। -भगवती 7/1 43. सति पाणातिवाए अप्पमत्तो अवहगो भवति। 37. उच्चालियंमि पाए, ईरियासमियस्स संकमट्ठाए। एवं असति पाणातिवाए पम्मत्ताए वहगो भवति।। वावज्जेज्ज कुलिंगी, मरिज्ज तं जोगमासज्ज। -निशीथचूर्णि 92 / न य तस्स तन्निमित्तो, बंधो सुहुमो वि देसिओ समए। 44. देखिए-दर्शन और चिन्तन, खण्ड 2, पृष्ठ 414 अणावज्जो उ पओगेण, सव्वभावेण सो जम्हा।। 45. यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। -ओघनियुक्ति 748-49 हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते।। -गीता 18/17 38. जा जयमाणस्स भवे, विराहणा सुत्तविहिसमग्गस्स। ___46. मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये। सा होई निज्जरफला, अज्झत्थविसोहिजुत्तस्स।। रटुं सानुचरं हन्त्वा अनिधो याति ब्राह्मणो। -धम्मपद 294 - ओघनियुक्ति 559 / भगवान् महावीर का अपरिग्रह-सिद्धान्त और उसकी उपादेयता संग्रहवृत्ति का उद्भव एवं विकास अपरिग्रह का प्रश्न सम्पत्ति के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है और सम्पत्ति की अवधारणा का विकास मानव जाति के विकास का सहगामी है। मानव इस पृथ्वी पर कैसे और कब अस्तित्व में आया? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक गूढ़ पहेली बना हुआ है। विकासवादी दार्शनिक मानव-सृष्टि को विकास की प्रक्रिया का ही एक अंग मानते हैं और अमीबा जैसे एक कोषीय प्राणी से प्राणियों की विभिन्न जातियों की विकास प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ था क्योंकि उस युग में न तो सम्पत्ति ही थी और न उसके स्वामित्व का विचार ही था। मानव उदार प्रकृति की गोद में पलता और पोषित होता था। जैन परम्परा में इसे यौगलिक युग (अकर्म-युग) कहा जाता है। साम्यवादी विचारधारा की दृष्टि से यह प्रारम्भिक साम्यवाद(PrimitiveSocialism) की अवस्था थी। सामान्यतया इस युग में मानव की आकाक्षायें इतनी बढ़ी-चढ़ी नहीं थीं, और एक दृष्टि से वह सुखी और सन्तुष्ट था। किन्तु धीरे-धीरे एक ओर जनसंख्या बढ़ी तथा दूसरी ओर प्रकृति प्रक्रिया (कन्टीन्यूइंग प्रोसेस) बताता है और मानव जाति के अस्तित्व यहीं से श्रम की उद्भावना हुई। जैन-परम्परा के अनुसार ऐसी अवस्था को भी इस आरोह और अवरोह-क्रम के सन्दर्भ में ही विवेचित करता में सर्वप्रथम भगवान् ऋषभदेव ने मानव जाति को कृषि की शिक्षा है। फिर भी नृतत्वविज्ञान, विकासवादी दर्शन और जैन दर्शन इस दी। कृषि में जहाँ एक ओर मानव-श्रम लगने लगा वहीं दूसरी ओर सम्बन्ध में एक मत हैं कि मानव की वर्तमान सभ्यता का विकास उस श्रम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अन्न-सामग्री के संचयन और स्वामित्व उसके प्राकृतिक जीवन से हुआ है। एक समय था जबकि मनुष्य विशुद्ध का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। वस्तुतः कृषि से उत्पन्न सामग्री ऐसी रूप से एक प्राकृतिक जीवन जीता था और प्रकृति भी इतनी समृद्ध नहीं, जो वर्ष में हर समय सुलभ हो सके, केवल वर्षा पर आश्रित थी कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न तो कोई विशिष्ट वह कृषि नियत समय पर ही अपनी उपज दे पाती थी और इसलिए श्रम करना होता था और न संग्रह ही। अत: उस युग में परिग्रह का सम्पूर्ण वर्ष भर के लिये अन्न का संचयन आवश्यक था। जीवन-रक्षण Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org