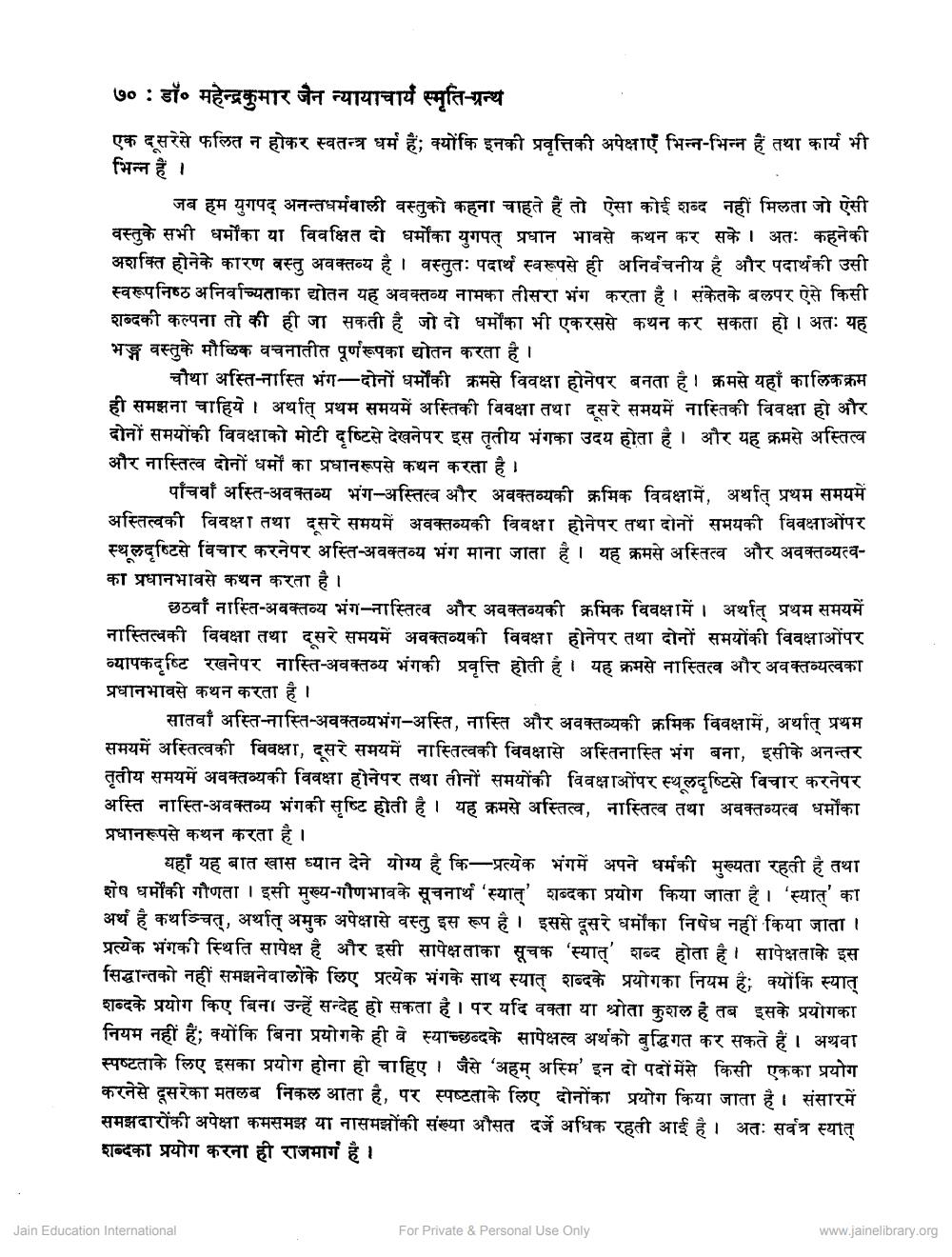________________
७० : डॉ. महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ एक दूसरेसे फलित न होकर स्वतन्त्र धर्म हैं; क्योंकि इनकी प्रवृत्तिकी अपेक्षाएं भिन्न-भिन्न हैं तथा कार्य भी भिन्न है ।
जब हम युगपद् अनन्तधर्मवाली वस्तुको कहना चाहते हैं तो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जो ऐसी वस्तुके सभी धर्मोंका या विवक्षित दो धर्मोंका युगपत् प्रधान भावसे कथन कर सके । अतः कहनेकी अशक्ति होनेके कारण वस्तु अवक्तव्य है। वस्तुतः पदार्थ स्वरूपसे ही अनिर्वचनीय है और पदार्थकी उसी स्वरूपनिष्ठ अनिर्वाच्यताका द्योतन यह अवक्तव्य नामका तीसरा भंग करता है। संकेतके बलपर ऐसे किसी शब्दकी कल्पना तो की ही जा सकती है जो दो धर्मोंका भी एकरससे कथन कर सकता हो । अतः यह भङ्ग वस्तुके मौलिक वचनातीत पूर्णरूपका द्योतन करता है।
चौथा अस्ति-नास्ति भंग-दोनों धर्मोंकी क्रमसे विवक्षा होनेपर बनता है। क्रमसे यहाँ कालिकक्रम ही समझना चाहिये। अर्थात् प्रथम समयमें अस्तिकी विवक्षा तथा दूसरे समयमें नास्तिकी विवक्षा हो और दोनों समयोंकी विवक्षाको मोटी दष्टिसे देखनेपर इस तृतीय भंगका उदय होता है। और यह क्रमसे अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों का प्रधानरूपसे कथन करता है।
पाँचवाँ अस्ति-अवक्तव्य भंग-अस्तित्व और अवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षामें, अर्थात् प्रथम समयम अस्तित्वकी विवक्षा तथा दसरे समयमें अवक्तव्यकी विवक्षा होनेपर तथा दोनों समयकी विवक्षाओंपर स्थलदष्टिसे विचार करनेपर अस्ति-अवक्तव्य भंग माना जाता है। यह क्रमसे अस्तित्व और अवक्तव्यत्वका प्रधानभावसे कथन करता है।
छठवाँ नास्ति-अवक्तव्य भंग-नास्तित्व और अवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षामें। अर्थात प्रथम समयमें नास्तित्वकी विवक्षा तथा दूसरे समयमें अवक्तव्यकी विवक्षा होनेपर तथा दोनों समयोंकी विवक्षाओंपर व्यापकदृष्टि रखनेपर नास्ति-अवक्तव्य भंगकी प्रवृत्ति होती है। यह क्रमसे नास्तित्व और अवक्तव्यत्वका प्रधानभावसे कथन करता है।
सातवाँ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यभंग-अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षामें, अर्थात् प्रथम समयमें अस्तित्वकी विवक्षा, दूसरे समयमें नास्तित्वकी विवक्षासे अस्तिनास्ति भंग बना, इसीके अनन्तर तृतीय समयमें अवक्तव्यकी विवक्षा होनेपर तथा तीनों समयोंकी विवक्षाओंपर स्थलदृष्टिसे विचार करनेपर अस्ति नास्ति-अवक्तव्य भंगकी सृष्टि होती है। यह क्रमसे अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मोका प्रधानरूपसे कथन करता है।
यहाँ यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक भंगमें अपने धर्मकी मुख्यता रहती है तथा शेष धर्मोकी गौणता । इसी मुख्य-गौणभावके सूचनार्थ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्' का अर्थ है कथञ्चित्, अर्थात् अमुक अपेक्षासे वस्तु इस रूप है। इससे दूसरे धर्मोंका निषेध नहीं किया जाता। प्रत्येक भंगकी स्थिति सापेक्ष है और इसी सापेक्षताका सूचक 'स्यात्' शब्द होता है। सापेक्षताके इस सिद्धान्तको नहीं समझनेवालोंके लिए प्रत्येक भंगके साथ स्यात् शब्दके प्रयोगका नियम है; क्योंकि स्यात् शब्दके प्रयोग किए बिना उन्हें सन्देह हो सकता है। पर यदि वक्ता या श्रोता कुशल है तब इसके प्रयोगका नियम नहीं हैं। क्योंकि बिना प्रयोगके ही वे स्याच्छब्दके सापेक्षत्व अर्थको बुद्धिगत कर सकते हैं। अथवा स्पष्टताके लिए इसका प्रयोग होना ही चाहिए। जैसे 'अहम् अस्मि' इन दो पदों मेंसे किसी एकका प्रयोग करनेसे दूसरेका मतलब निकल आता है, पर स्पष्टताके लिए दोनोंका प्रयोग किया जाता है। संसारमें समझदारोंकी अपेक्षा कमसमझ या नासमझोंकी संख्या औसत दर्जे अधिक रहती आई है। अतः सर्वत्र स्यात शब्दका प्रयोग करना ही राजमार्ग है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org