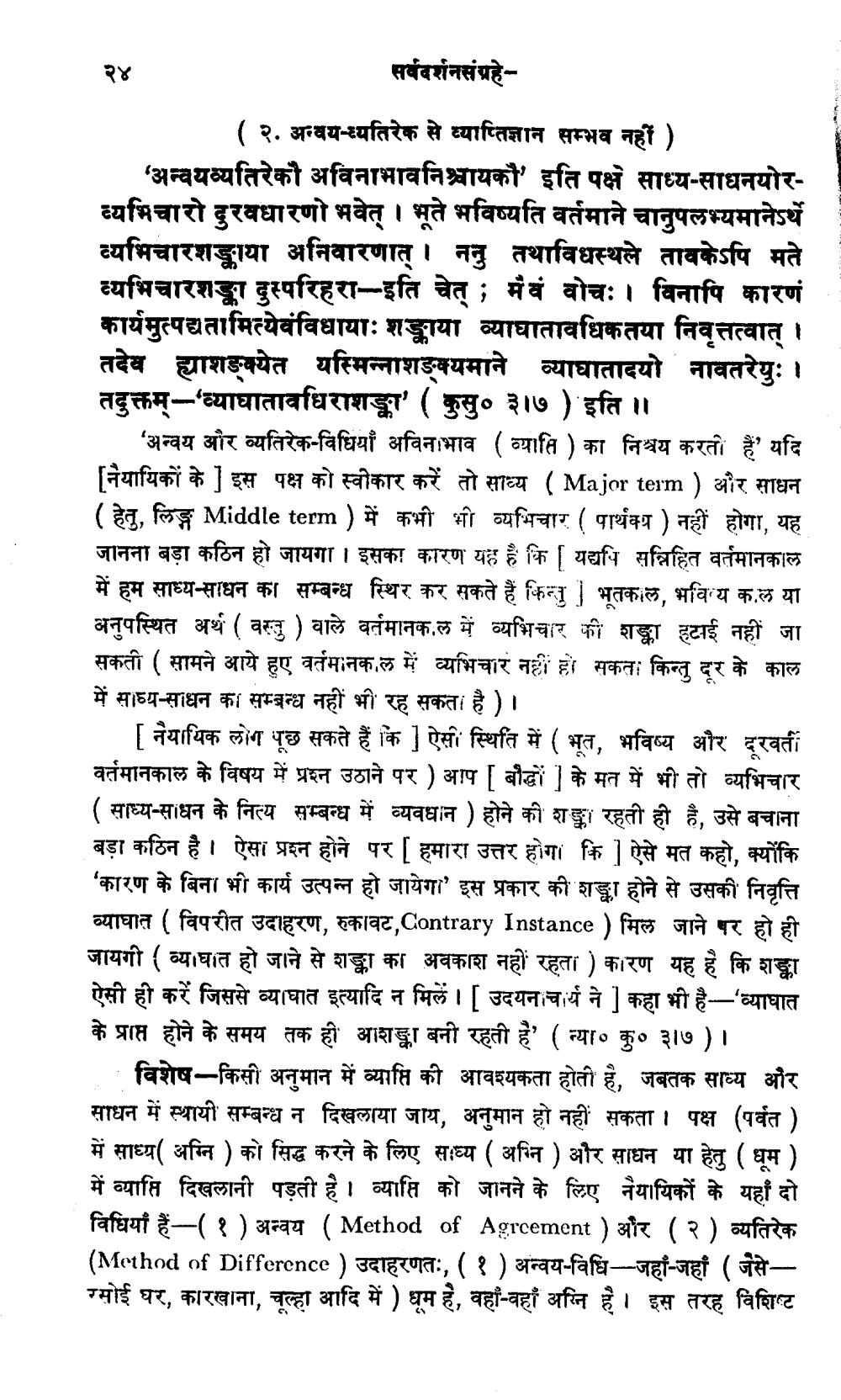________________
सर्वदर्शनसंग्रहे
( २. अन्वय-ध्यतिरेक से व्याप्तिज्ञान सम्भव नहीं ) 'अन्वयव्यतिरेको अविनाभावनिश्चायको' इति पक्षे साध्य-साधनयोरव्यभिचारो दुरवधारणो भवेत् । भूते भविष्यति वर्तमाने चानुपलभ्यमानेऽर्थे व्यभिचारशङ्काया अनिवारणात् । ननु तथाविधस्थले तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्का दुस्परिहरा-इति चेत् ; मैवं वोचः। विनापि कारणं कार्यमुत्पद्यतामित्येवंविधायाः शङ्काया व्याघातावधिकतया निवृत्तत्वात् । तदेव ह्याशङ्ख्येत यस्मिन्नाशङ्ख्यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः । तदुक्तम्-'व्याघातावधिराशङ्का' ( कुसु० ३७ ) इति ॥ ___ 'अन्वय और व्यतिरेक-विधियाँ अविनाभाव ( व्याति ) का निश्चय करती हैं यदि नैयायिकों के ] इस पक्ष को स्वीकार करें तो साध्य ( Major term ) और साधन ( हेतु, लिङ्ग Middle term ) में कभी भी व्यभिचार ( पार्थक्य ) नहीं होगा, यह जानना बड़ा कठिन हो जायगा । इसका कारण यह है कि [ यद्यपि सन्निहित वर्तमानकाल में हम साध्य-साधन का सम्बन्ध स्थिर कर सकते हैं किन्तु ] भूतकाल, भवि य क.ल या अनुपस्थित अर्थ ( वस्तु ) वाले वर्तमानक.ल में व्यभिचार की शङ्का हटाई नहीं जा सकती ( सामने आये हुए वर्तमानकाल में व्यभिचार नहीं हो सकता किन्तु दूर के काल में साध्य-साधन का सम्बन्ध नहीं भी रह सकता है )।
[ नैयायिक लोग पूछ सकते हैं कि ] ऐसी स्थिति में ( भूत, भविष्य और दूरवर्ती वर्तमानकाल के विषय में प्रश्न उठाने पर ) आप [ बौद्धों ] के मत में भी तो व्यभिचार ( साध्य-साधन के नित्य सम्बन्ध में व्यवधान ) होने की शङ्का रहती ही है, उसे बचाना बड़ा कठिन है। ऐसा प्रश्न होने पर [ हमारा उत्तर होगा कि ] ऐसे मत कहो, क्योंकि 'कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न हो जायेगा' इस प्रकार की शङ्का होने से उसकी निवृत्ति व्याघात ( विपरीत उदाहरण, रुकावट,Contrary Instance ) मिल जाने पर हो ही जायगी ( व्याघात हो जाने से शङ्का का अवकाश नहीं रहता ) कारण यह है कि शङ्का ऐसी ही करें जिससे व्याघात इत्यादि न मिलें। [ उदयनाचार्य ने ] कहा भी है—'व्याघात के प्राप्त होने के समय तक ही आशङ्का बनी रहती है' ( न्या० कु० ३७ )।
विशेष-किसी अनुमान में व्याप्ति की आवश्यकता होती है, जबतक साध्य और साधन में स्थायी सम्बन्ध न दिखलाया जाय, अनुमान हो नहीं सकता। पक्ष (पर्वत ) में साध्य( अग्नि ) को सिद्ध करने के लिए साध्य ( अग्नि ) और साधन या हेतु (धूम ) में व्याप्ति दिखलानी पड़ती है। व्याप्ति को जानने के लिए नैयायिकों के यहां दो विधियाँ हैं-( १ ) अन्वय ( Method of Agreement ) और ( २ ) व्यतिरेक (Method of Difference ) उदाहरणतः, ( १ ) अन्वय-विधि-जहाँ-जहाँ ( जैसेरसोई घर, कारखाना, चूल्हा आदि में ) धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि है। इस तरह विशिष्ट