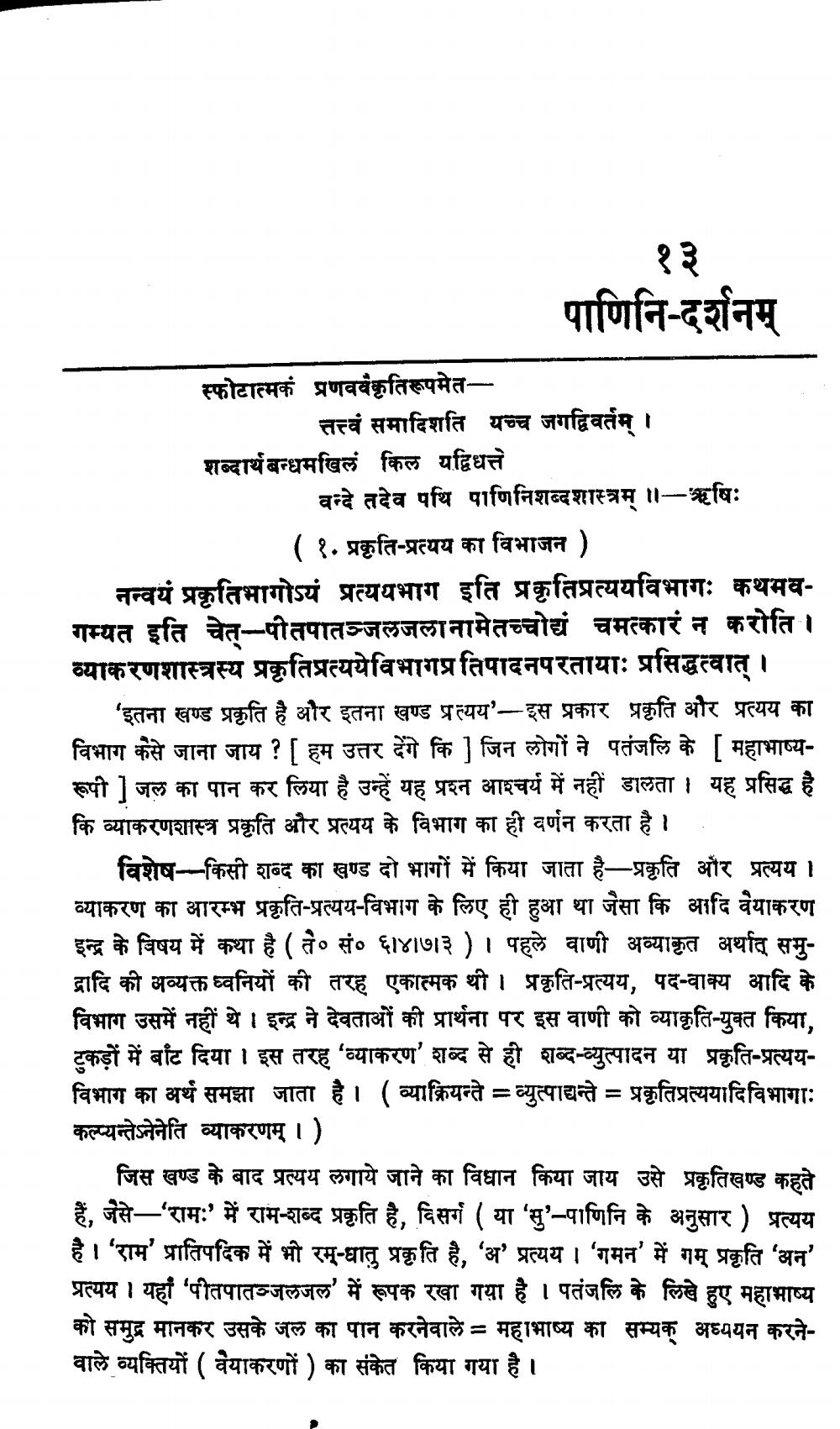________________
पाणिनि-दर्शनम्
स्फोटात्मकं प्रणववकृतिरूपमेत
तत्त्वं समादिशति यच्च जगद्विवर्तम् । शब्दार्थबन्धमखिलं किल यद्विधत्ते ।
वन्दे तदेव पथि पाणिनिशब्दशास्त्रम् ॥-ऋषिः
( १. प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन ) नन्वयं प्रकृतिभागोऽयं प्रत्ययभाग इति प्रकृतिप्रत्ययविभागः कथमवगम्यत इति चेत्-पीतपातञ्जलजलानामेतच्चोधे चमत्कारं न करोति । व्याकरणशास्त्रस्य प्रकृतिप्रत्ययेविभागप्रतिपादनपरतायाः प्रसिद्धत्वात् ।
'इतना खण्ड प्रकृति है और इतना खण्ड प्रत्यय'- इस प्रकार प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कैसे जाना जाय ? [ हम उत्तर देंगे कि ] जिन लोगों ने पतंजलि के [ महाभाष्यरूपी ] जल का पान कर लिया है उन्हें यह प्रश्न आश्चर्य में नहीं डालता। यह प्रसिद्ध है कि व्याकरणशास्त्र प्रकृति और प्रत्यय के विभाग का ही वर्णन करता है।
विशेष-किसी शब्द का खण्ड दो भागों में किया जाता है—प्रकृति और प्रत्यय । व्याकरण का आरम्भ प्रकृति-प्रत्यय-विभाग के लिए ही हुआ था जैसा कि आदि वैयाकरण इन्द्र के विषय में कथा है ( ते० सं० ६।४।७।३ )। पहले वाणी अव्याकृत अर्थात् समुद्रादि की अव्यक्त ध्वनियों की तरह एकात्मक थी। प्रकृति-प्रत्यय, पद-वाक्य आदि के विभाग उसमें नहीं थे। इन्द्र ने देवताओं की प्रार्थना पर इस वाणी को व्याकृति-युक्त किया, टुकड़ों में बाँट दिया । इस तरह 'व्याकरण' शब्द से ही शब्द-व्युत्पादन या प्रकृति-प्रत्ययविभाग का अर्थ समझा जाता है। ( व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते = प्रकृतिप्रत्ययादिविभागाः कल्प्यन्तेऽनेनेति व्याकरणम् । )
जिस खण्ड के बाद प्रत्यय लगाये जाने का विधान किया जाय उसे प्रकृतिखण्ड कहते हैं, जैसे—'रामः' में राम-शब्द प्रकृति है, विसर्ग ( या 'सु'-पाणिनि के अनुसार ) प्रत्यय है । 'राम' प्रातिपदिक में भी रम्-धातु प्रकृति है, 'अ' प्रत्यय । 'गमन' में गम् प्रकृति 'अन' प्रत्यय । यहाँ 'पीतपातञ्जलजल' में रूपक रखा गया है । पतंजलि के लिखे हुए महाभाष्य को समुद्र मानकर उसके जल का पान करनेवाले = महाभाष्य का सम्यक् अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों ( वैयाकरणों) का संकेत किया गया है।