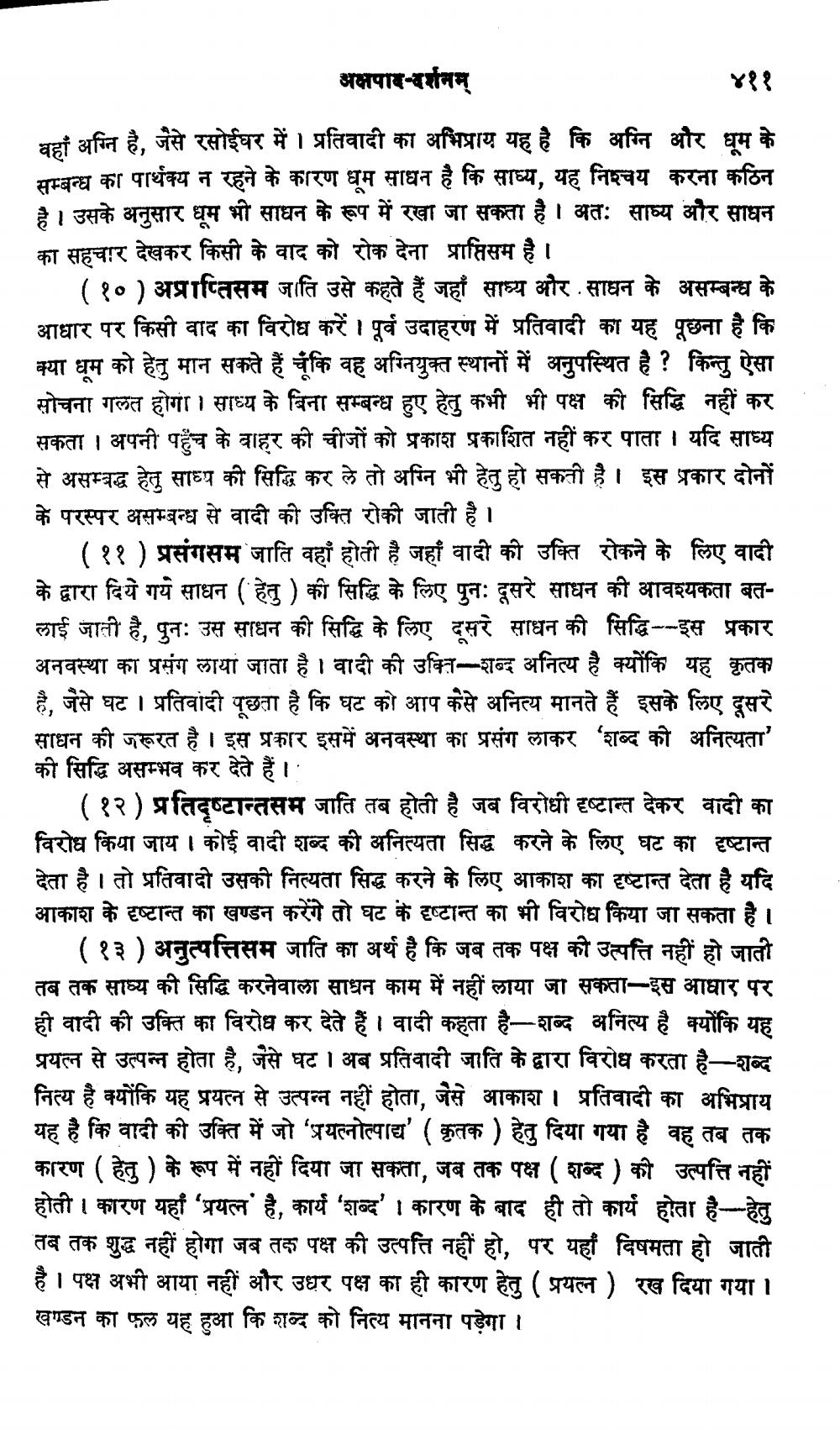________________
अक्षपाद-दर्शनम्
४११
वहाँ अग्नि है, जैसे रसोईघर में । प्रतिवादी का अभिप्राय यह है कि अग्नि और धूम के सम्बन्ध का पार्थक्य न रहने के कारण धूम साधन है कि साध्य, यह निश्चय करना कठिन है । उसके अनुसार धूम भी साधन के रूप में रखा जा सकता है । अत: साध्य और साधन का सहचार देखकर किसी के वाद को रोक देना प्राप्तिसम है ।
(१०) अप्राप्तिसम जाति उसे कहते हैं जहाँ साध्य और साधन के असम्बन्ध के आधार पर किसी वाद का विरोध करें । पूर्व उदाहरण में प्रतिवादी का यह पूछना है कि क्या धूम को हेतु मान सकते हैं चूंकि वह अग्नियुक्त स्थानों में अनुपस्थित है ? किन्तु ऐसा सोचना गलत होगा । साध्य के बिना सम्बन्ध हुए हेतु कभी भी पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता । अपनी पहुँच के बाहर की चीजों को प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाता । यदि साध्य से असम्बद्ध हेतु साध्य की सिद्धि कर ले तो अग्नि भी हेतु हो सकती है। इस प्रकार दोनों के परस्पर असम्बन्ध से वादी की उक्ति रोकी जाती है ।
.
( ११ ) प्रसंगसम जाति वहाँ होती है जहाँ वादी की उक्ति रोकने के लिए वादी के द्वारा दिये गये साधन ( हेतु ) की सिद्धि के लिए पुनः दूसरे साधन की आवश्यकता बतलाई जाती है, पुनः उस साधन की सिद्धि के लिए दूसरे साधन की सिद्धि - - इस प्रकार अनवस्था का प्रसंग लाया जाता है । वादी की उक्ति - शब्द अनित्य है क्योंकि यह कृतक है, जैसे घट । प्रतिवादी पूछता है कि घट को आप कैसे अनित्य मानते हैं इसके लिए दूसरे साधन की जरूरत है । इस प्रकार इसमें अनवस्था का प्रसंग लाकर ' शब्द की अनित्यता' की सिद्धि असम्भव कर देते हैं ।
(१२) प्रतिदृष्टान्तसम जाति तब होती है जब विरोधी दृष्टान्त देकर वादी का विरोध किया जाय । कोई वादी शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए घट का दृष्टान्त देता है । तो प्रतिवादी उसकी नित्यता सिद्ध करने के लिए आकाश का दृष्टान्त देता है यदि आकाश के दृष्टान्त का खण्डन करेंगे तो घट के दृष्टान्त का भी विरोध किया जा सकता है ।
-
(१३) अनुत्पत्तिसम जाति का अर्थ है कि जब तक पक्ष की उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक साध्य की सिद्धि करनेवाला साधन काम में नहीं लाया जा सकता -- इस आधार पर ही वादी की उक्ति का विरोध कर देते हैं । वादी कहता है— शब्द अनित्य है क्योंकि यह प्रयत्न से उत्पन्न होता है, जैसे घट । अब प्रतिवादी जाति के द्वारा विरोध करता है - शब्द नित्य है क्योंकि यह प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता, जैसे आकाश । प्रतिवादी का अभिप्राय यह है कि वादी की उक्ति में जो 'प्रयत्नोत्पाद्य' ( कृतक ) हेतु दिया गया है वह तब तक कारण ( हेतु ) के रूप में नहीं दिया जा सकता, जब तक पक्ष ( शब्द ) की उत्पत्ति नहीं होती । कारण यहाँ 'प्रयत्न' है, कार्य 'शब्द' । कारण के बाद ही तो कार्य होता है - हेतु तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक पक्ष की उत्पत्ति नहीं हो, पर यहाँ दिषमता हो जाती है | पक्ष अभी आया नहीं और उधर पक्ष का ही कारण हेतु ( प्रयत्न ) रख दिया गया । खण्डन का फल यह हुआ कि शब्द को नित्य मानना पड़ेगा ।