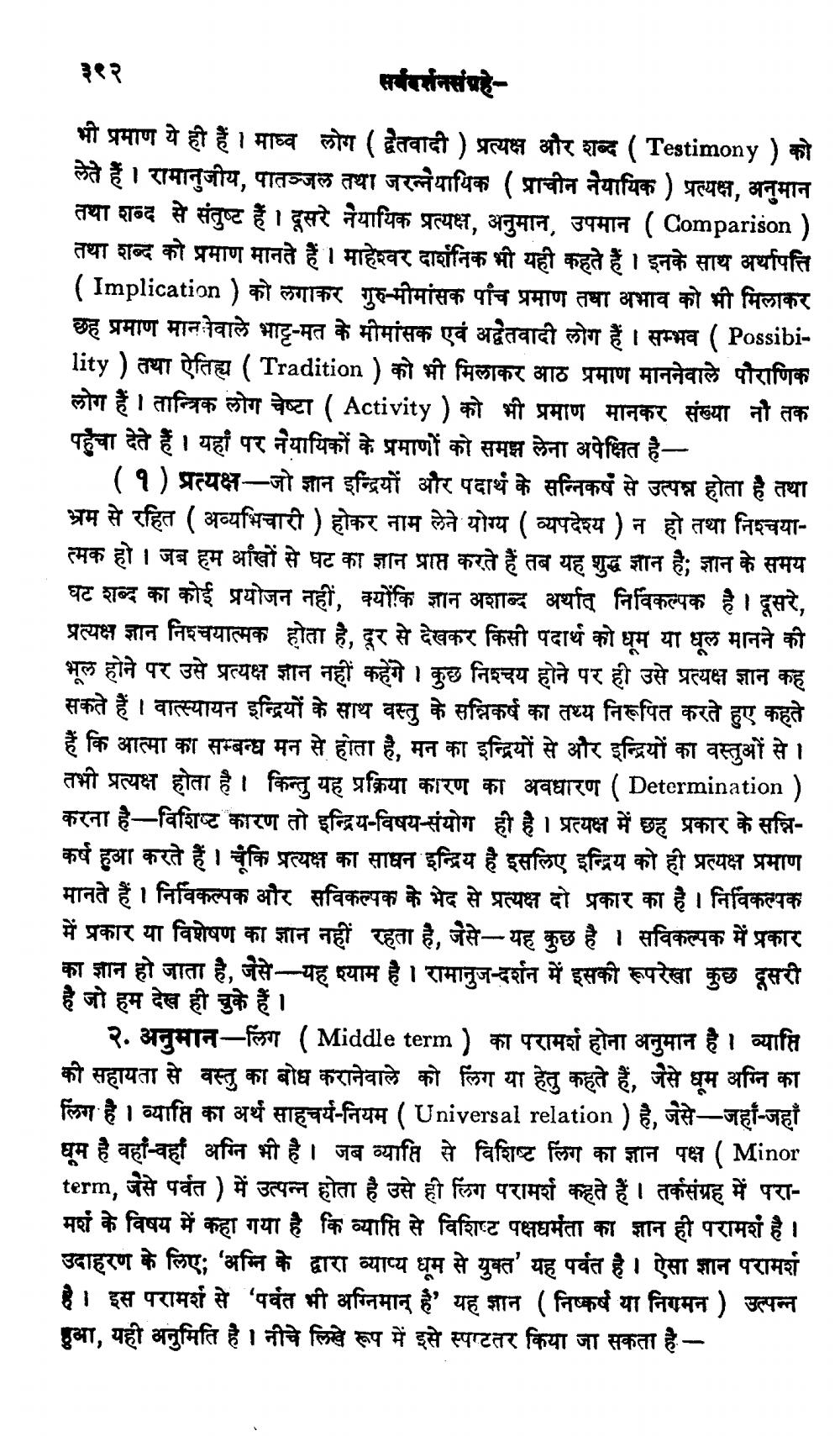________________
३९२
सर्वदर्शनसंग्रहे
भी प्रमाण ये ही हैं | माध्व लोग ( द्वैतवादी ) प्रत्यक्ष और शब्द ( Testimony ) को लेते हैं। रामानुजीय, पातञ्जल तथा जरन्नेयाथिक ( प्राचीन नैयायिक ) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द से संतुष्ट हैं । दूसरे नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ( Comparison ) तथा शब्द को प्रमाण मानते हैं । माहेश्वर दार्शनिक भी यही कहते हैं । इनके साथ अर्थापत्ति ( Implication ) को लगाकर गुरु-मीमांसक पांच प्रमाण तथा अभाव को भी मिलाकर छह प्रमाण माननेवाले भाट्ट-मत के मीमांसक एवं अद्वैतवादी लोग हैं । सम्भव ( Possibility ) तथा ऐतिह्य ( Tradition ) को भी मिलाकर आठ प्रमाण माननेवाले पौराणिक लोग हैं । तान्त्रिक लोग चेष्टा ( Activity ) को भी प्रमाण मानकर संख्या नौ तक पहुँचा देते हैं । यहाँ पर नैयायिकों के प्रमाणों को समझ लेना अपेक्षित है
( १ ) प्रत्यक्ष - जो ज्ञान इन्द्रियों और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है तथा भ्रम से रहित ( अव्यभिचारी ) होकर नाम लेने योग्य ( व्यपदेश्य ) न हो तथा निश्चयात्मक हो । जब हम आंखों से घट का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब यह शुद्ध ज्ञान है; ज्ञान के समय घट शब्द का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि ज्ञान अशाब्द अर्थात् निर्विकल्पक है । दूसरे, प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चयात्मक होता है, दूर से देखकर किसी पदार्थ को धूम या धूल मानने की भूल होने पर उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे । कुछ निश्चय होने पर ही उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं । वात्स्यायन इन्द्रियों के साथ वस्तु के सन्निकर्ष का तथ्य निरूपित करते हुए कहते हैं कि आत्मा का सम्बन्ध मन से होता है, मन का इन्द्रियों से और इन्द्रियों का वस्तुओं से । तभी प्रत्यक्ष होता है । किन्तु यह प्रक्रिया कारण का अवधारण ( Determination ) करना है - विशिष्ट कारण तो इन्द्रिय-विषय-संयोग ही है । प्रत्यक्ष में छह प्रकार के सन्नि कर्ष हुआ करते हैं । चूंकि प्रत्यक्ष का साधन इन्द्रिय है इसलिए इन्द्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं । निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का | निर्विकल्पक में प्रकार या विशेषण का ज्ञान नहीं रहता है, जैसे - यह कुछ है । सविकल्पक में प्रकार का ज्ञान हो जाता है, जैसे - यह श्याम है । रामानुज दर्शन में इसकी रूपरेखा कुछ दूसरी है जो हम देख ही चुके हैं ।
२. अनुमान - लिंग ( Middle term ) का परामर्श होना अनुमान है । व्याप्ति की सहायता से वस्तु का बोध करानेवाले को लिंग या हेतु कहते हैं, जैसे धूम अग्नि का लिंग है । व्याप्ति का अर्थ साहचर्य-नियम ( Universal relation ) है, जैसे- जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ वहीं अग्नि भी है। जब व्याप्ति से विशिष्ट लिंग का ज्ञान पक्ष ( Minor term, जैसे पर्वत ) में उत्पन्न होता है उसे ही लिंग परामर्श कहते हैं । तर्कसंग्रह में परामर्श के विषय में कहा गया है कि व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान ही परामर्श है । उदाहरण के लिए; 'अग्नि के द्वारा व्याप्य धूम से युक्त' यह पर्वत है । ऐसा ज्ञान परामर्श है। इस परामर्श से 'पर्वत भी अग्निमान् है' यह ज्ञान (निष्कर्ष या निगमन) उत्पन्न हुआ, यही अनुमिति है । नीचे लिखे रूप में इसे स्पष्टतर किया जा सकता है
――