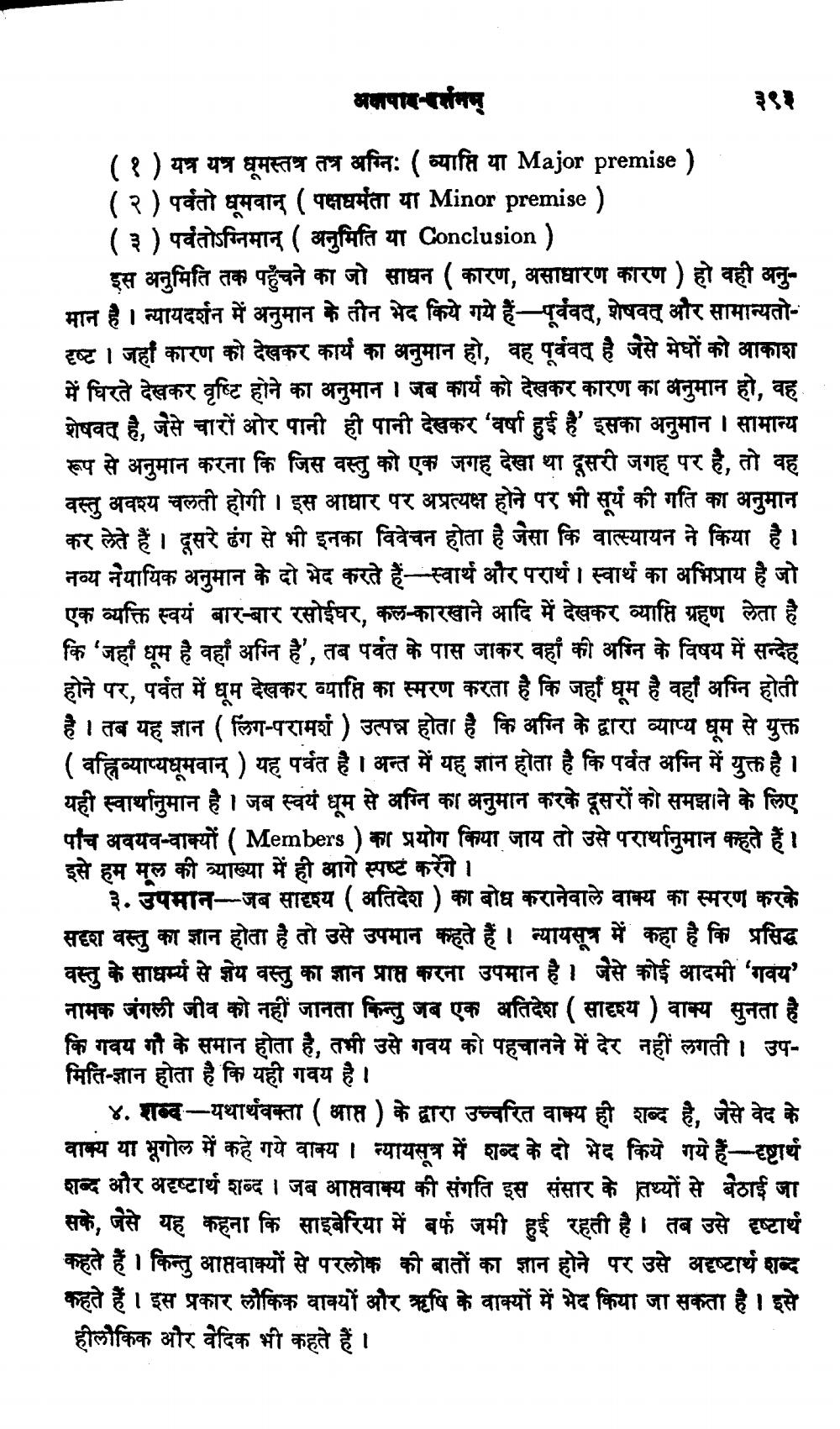________________
अक्षपारसनन्
( १ ) यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः ( व्याप्ति या Major premise ) (२) पर्वतो धूमवान् ( पक्षधर्मता या Minor premise ) (३) पर्वतोऽग्निमान ( अनुमिति या Conclusion)
इस अनुमिति तक पहुँचने का जो साधन ( कारण, असाधारण कारण ) हो वही अनुमान है । न्यायदर्शन में अनुमान के तीन भेद किये गये हैं—पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट । जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो, वह पूर्ववत् है जैसे मेघों को आकाश में घिरते देखकर वृष्टि होने का अनुमान । जब कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो, वह शेषवत् है, जैसे चारों ओर पानी ही पानी देखकर 'वर्षा हुई है। इसका अनुमान । सामान्य रूप से अनुमान करना कि जिस वस्तु को एक जगह देखा था दूसरी जगह पर है, तो वह वस्तु अवश्य चलती होगी। इस आधार पर अप्रत्यक्ष होने पर भी सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं। दूसरे ढंग से भी इनका विवेचन होता है जैसा कि वात्स्यायन ने किया है। नव्य नैयायिक अनुमान के दो भेद करते हैं- स्वार्थ और परार्थ । स्वार्थ का अभिप्राय है जो एक व्यक्ति स्वयं बार-बार रसोईघर, कल-कारखाने आदि में देखकर व्याप्ति ग्रहण लेता है कि 'जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है', तब पर्वत के पास जाकर वहाँ की अग्नि के विषय में सन्देह होने पर, पर्वत में धूम देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहां धूम है वहां अग्नि होती है । तब यह ज्ञान (लिंग-परामर्श) उत्पन्न होता है कि अग्नि के द्वारा व्याप्य धूम से युक्त ( वह्निव्याप्यधूमवान् ) यह पर्वत है । अन्त में यह ज्ञान होता है कि पर्वत अग्नि में युक्त है। यही स्वार्थानुमान है । जब स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझाने के लिए पांच अवयव-वाक्यों ( Members ) का प्रयोग किया जाय तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। इसे हम मूल की व्याख्या में ही आगे स्पष्ट करेंगे।
३. उपमान-जब सादृश्य ( अतिदेश ) का बोध करानेवाले वाक्य का स्मरण करके सदृश वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे उपमान कहते हैं । न्यायसूत्र में कहा है कि प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से शेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान है। जैसे कोई आदमी 'गवय' नामक जंगली जीव को नहीं जानता किन्तु जब एक अतिदेश ( सादृश्य ) वाक्य सुनता है कि गवय गौ के समान होता है, तभी उसे गवय को पहचानने में देर नहीं लगती। उपमिति-ज्ञान होता है कि यही गवय है।
४. शब्द-यथार्थवक्ता ( आप्त ) के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शब्द है, जैसे वेद के वाक्य या भूगोल में कहे गये वाक्य । न्यायसूत्र में शब्द के दो भेद किये गये हैं-दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द । जब आप्तवाक्य की संगति इस संसार के तथ्यों से बैठाई जा सके, जैसे यह कहना कि साइबेरिया में बर्फ जमी हुई रहती है। तब उसे दृष्टार्थ कहते हैं । किन्तु आप्तवाक्यों से परलोक की बातों का ज्ञान होने पर उसे अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं । इस प्रकार लौकिक वाक्यों और ऋषि के वाक्यों में भेद किया जा सकता है। इसे हीलौकिक और वैदिक भी कहते हैं ।