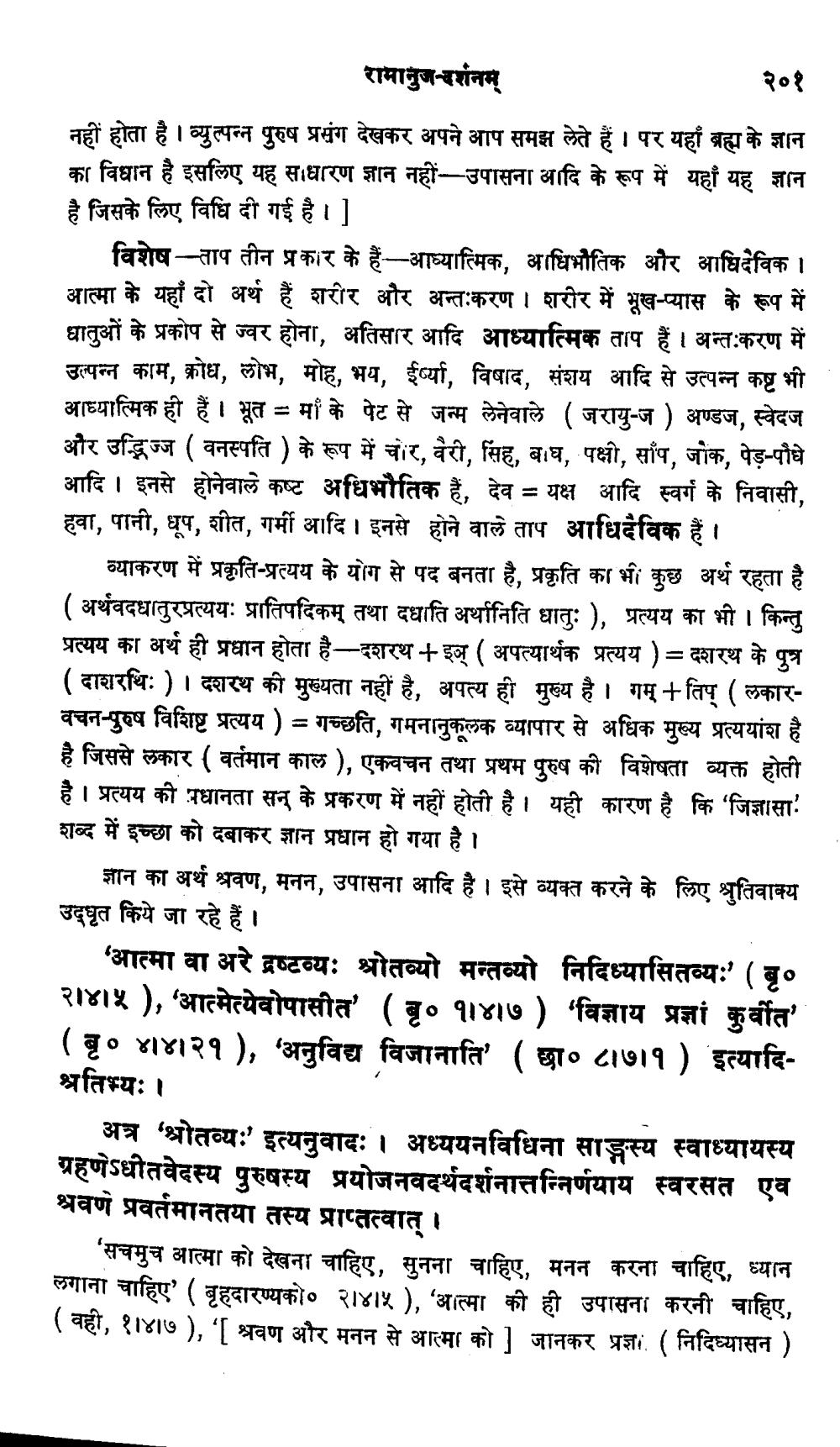________________
रामानुज दर्शनम्
२०१
नहीं होता है । व्युत्पन्न पुरुष प्रसंग देखकर अपने आप समझ लेते हैं । पर यहाँ ब्रह्म के ज्ञान का विधान है इसलिए यह साधारण ज्ञान नहीं - उपासना आदि के रूप में यहाँ यह ज्ञान है जिसके लिए विधि दी गई है । ]
विशेष- -ताप तीन प्रकार के हैं— आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । आत्मा के यहाँ दो अर्थ हैं शरीर और अन्तःकरण । शरीर में भूख-प्यास के रूप में धातुओं के प्रकोप से ज्वर होना, अतिसार आदि आध्यात्मिक ताप हैं । अन्तःकरण में उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद, संशय आदि से उत्पन्न कष्ट भी आध्यात्मिक ही हैं । भूत = माँ के पेट से जन्म लेनेवाले ( जरायु-ज ) अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज (वनस्पति) के रूप में चोर, वैरी, सिंह, बाघ, पक्षी, साँप, जोक, पेड़-पौधे आदि । इनसे होनेवाले कष्ट अधिभौतिक हैं, देव = यक्ष आदि स्वर्ग के निवासी, हवा, पानी, धूप, शीत, गर्मी आदि। इनसे होने वाले ताप आधिदैविक हैं ।
व्याकरण में प्रकृति - प्रत्यय के योग से पद बनता है, प्रकृति का भी कुछ अर्थ रहता है ( अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् तथा दधाति अर्थानिति धातुः ), प्रत्यय का भी । किन्तु प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान होता है - दशरथ + इञ् ( अपत्यार्थक प्रत्यय ) | = दशरथ के पुत्र ( दाशरथिः ) । दशरथ की मुख्यता नहीं है, अपत्य ही मुख्य है । गम् + तिप् ( लकारवचन - पुरुष विशिष्ट प्रत्यय ) = गच्छति, गमनानुकूलक व्यापार से अधिक मुख्य प्रत्ययांश है है जिससे लकार ( वर्तमान काल ), एकवचन तथा प्रथम पुरुष की विशेषता व्यक्त होती है । प्रत्यय की प्रधानता सन् के प्रकरण में नहीं होती है । यही कारण है कि 'जिज्ञासा' शब्द में इच्छा को दबाकर ज्ञान प्रधान हो गया है ।
ज्ञान का अर्थ श्रवण, मनन, उपासना आदि है । इसे व्यक्त करने के लिए श्रुतिवाक्य उद्धृत किये जा रहे हैं ।
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० २।४।५), 'आत्मेत्येवोपासीत' ( बृ० १।४।७ ) 'विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ' ( बृ० ४।४।२१ ), 'अनुविद्य विजानाति' ( छा० ८।७।१ ) इत्यादिश्रतिभ्यः
ः ।
अत्र 'श्रोतव्यः' इत्यनुवादः । अध्ययनविधिना साङ्गस्य स्वाध्यायस्य ग्रहणेऽधीतवेदस्य पुरुषस्य प्रयोजनवदर्थदर्शनात्तन्निर्णयाय स्वरसत एव श्रवणे प्रवर्तमानतया तस्य प्राप्तत्वात् ।
'सचमुच आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए' ( बृहदारण्यको ० २।४।५), 'आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, (वही, ११४१७ ), ' [ श्रवण और मनन से आत्मा को ] जानकर प्रज्ञा ( निदिध्यासन )