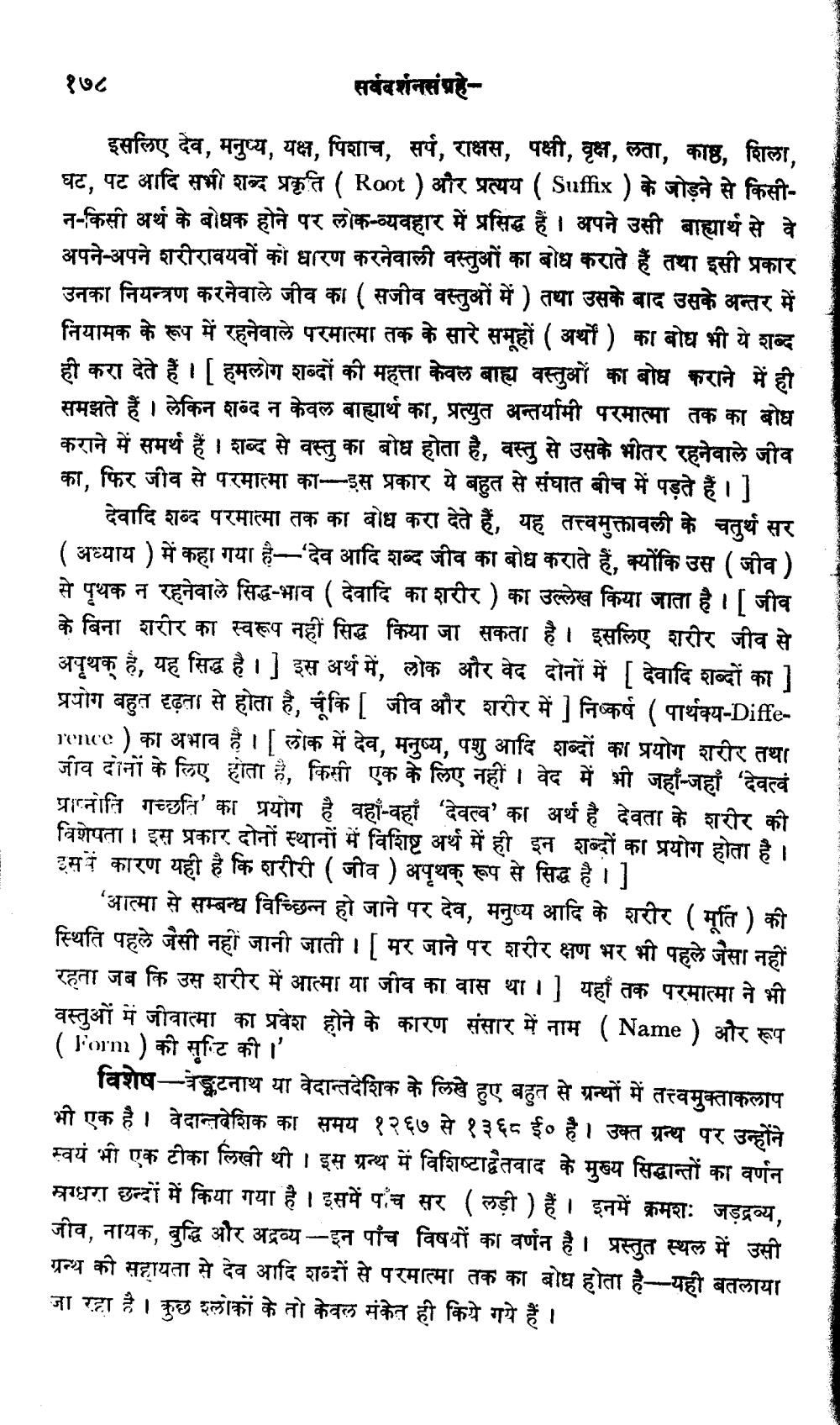________________
१७८
सर्वदर्शनसंग्रहे
इसलिए देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, सर्प, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, लता, काष्ठ, शिला, घट, पट आदि सभी शब्द प्रकृति ( Root ) और प्रत्यय ( Suffix ) के जोड़ने से किसीन-किसी अर्थ के बोधक होने पर लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध हैं। अपने उसी बाह्यार्थ से वे अपने-अपने शरीरावयवों को धारण करनेवाली वस्तुओं का बोध कराते हैं तथा इसी प्रकार उनका नियन्त्रण करनेवाले जीव का ( सजीव वस्तुओं में ) तथा उसके बाद उसके अन्तर में नियामक के रूप में रहनेवाले परमात्मा तक के सारे समूहों ( अर्थों ) का बोध भी ये शब्द ही करा देते हैं । [ हमलोग शब्दों की महत्ता केवल बाह्य वस्तुओं का बोध कराने में ही समझते हैं । लेकिन शब्द न केवल बाह्यार्थ का, प्रत्युत अन्तर्यामी परमात्मा तक का बोध कराने में समर्थ हैं । शब्द से वस्तु का बोध होता है, वस्तु से उसके भीतर रहनेवाले जीव का, फिर जीव से परमात्मा का-इस प्रकार ये बहुत से संघात बीच में पड़ते हैं।]
देवादि शब्द परमात्मा तक का बोध करा देते हैं, यह तत्त्वमुक्तावली के चतुर्थ सर ( अध्याय ) में कहा गया है-'देव आदि शब्द जीव का बोध कराते हैं, क्योंकि उस (जीव) से पृथक न रहनेवाले सिद्ध-भाव ( देवादि का शरीर ) का उल्लेख किया जाता है। [ जीव के बिना शरीर का स्वरूप नहीं सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए शरीर जीव से अपृथक् है, यह सिद्ध है। ] इस अर्थ में, लोक और वेद दोनों में [ देवादि शब्दों का ] प्रपोग बहुत दृढ़ता से होता है, चूंकि [ जीव और शरीर में ] निष्कर्ष ( पार्थक्य-Difference ) का अभाव है। लोक में देव, मनुष्य, पशु आदि शब्दों का प्रयोग शरीर तथा जीव दोनों के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं । वेद में भी जहाँ-जहाँ 'देवत्वं प्राप्नोति गच्छति' का प्रयोग है वहाँ-वहाँ 'देवत्व' का अर्थ है देवता के शरीर की विशेषता। इस प्रकार दोनों स्थानों में विशिष्ट अर्थ में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें कारण यही है कि शरीरी ( जीव ) अपृथक् रूप से सिद्ध है। ]
_ 'आत्मा से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर देव, मनुष्य आदि के शरीर ( मूर्ति ) की स्थिति पहले जैसी नहीं जानी जाती। [ मर जाने पर शरीर क्षण भर भी पहले जैसा नहीं रहता जब कि उस शरीर में आत्मा या जीव का वास था।] यहाँ तक परमात्मा ने भी वस्तुओं में जीवात्मा का प्रवेश होने के कारण संसार में नाम ( Name ) और रूप (Jorm ) की सृष्टि की।'
विशेष-वेङ्कटनाथ या वेदान्तदेशिक के लिखे हुए बहुत से ग्रन्थों में तत्त्वमुक्ताकलाप भी एक है। वेदान्तदेशिक का समय १२६७ से १३६८ ई० है। उक्त ग्रन्थ पर उन्होंने स्वयं भी एक टीका लिखी थी। इस ग्रन्थ में विशिष्टाद्वैतवाद के मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन स्रग्धरा छन्दों में किया गया है । इसमें पंच सर ( लड़ी ) हैं। इनमें क्रमशः जड़द्रव्य, जीव, नायक, बुद्धि और अद्रव्य-इन पाँच विषयों का वर्णन है। प्रस्तुत स्थल में उसी ग्रन्थ की सहायता से देव आदि शब्दों से परमात्मा तक का बोध होता है-यही बतलाया जा रहा है। कुछ श्लोकों के तो केवल संकेत ही किये गये हैं।