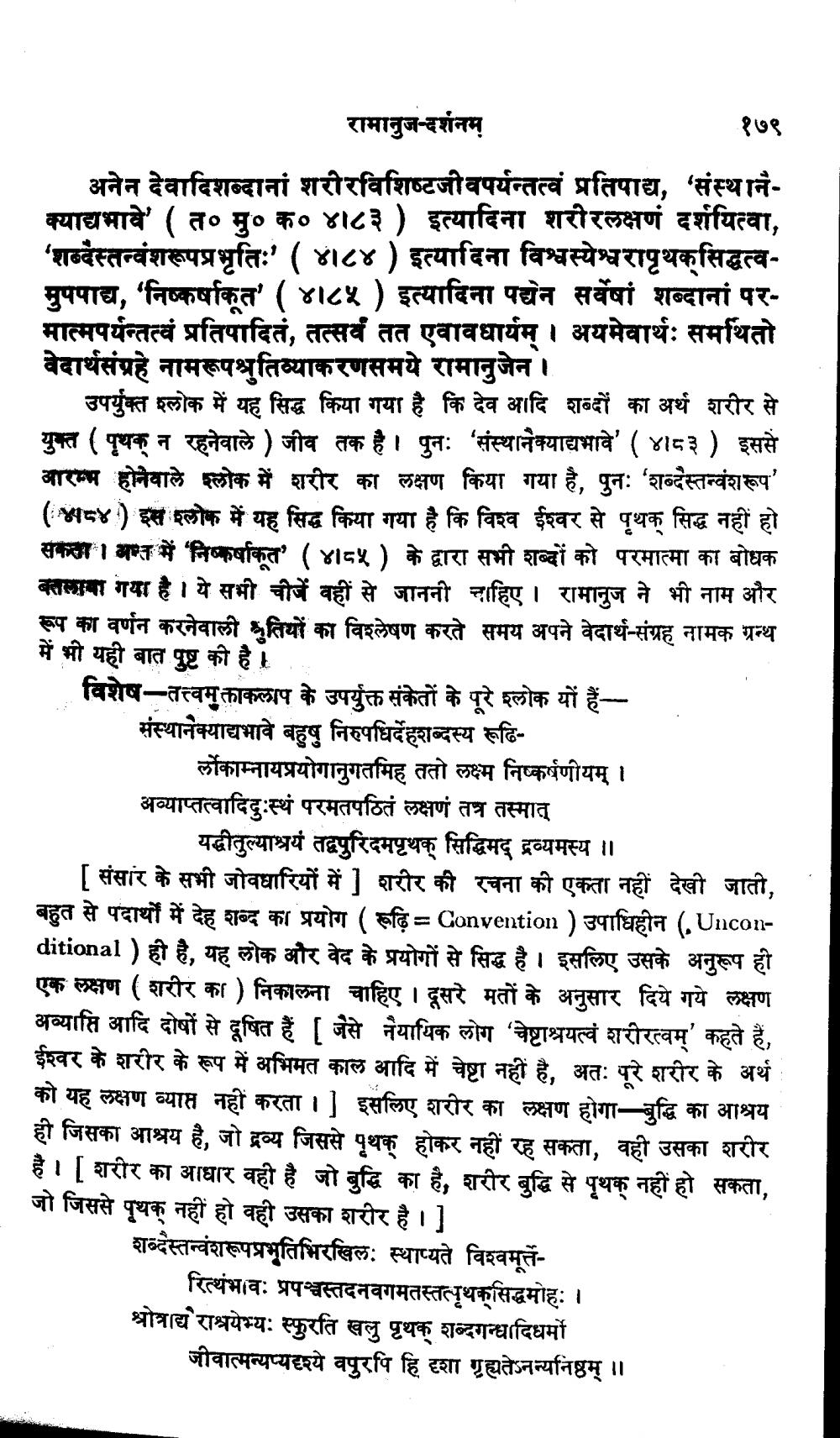________________
रामानुज-दर्शनम्
१७९ अनेन देवादिशब्दानां शरीरविशिष्टजीवपर्यन्तत्वं प्रतिपाद्य, 'संस्थानक्याद्यभावे ( त० मु० क० ४।८३) इत्यादिना शरीरलक्षणं दर्शयित्वा, 'शब्देस्तन्वंशरूपप्रभृतिः' ( ४८४ ) इत्यादिना विश्वस्येश्वरापृथसिद्धत्वमुपपाद्य, 'निष्कर्षाकृत' (४।८५) इत्यादिना पद्येन सर्वेषां शब्दानां परमात्मपर्यन्तत्वं प्रतिपादितं, तत्सर्व तत एवावधार्यम् । अयमेवार्थः समथितो वेदार्थसंग्रहे नामरूपश्रुतिव्याकरणसमये रामानुजेन ।
उपर्युक्त श्लोक में यह सिद्ध किया गया है कि देव आदि शब्दों का अर्थ शरीर से युक्त ( पृथक् न रहनेवाले ) जीव तक है। पुनः 'संस्थानक्याद्यभावे' ( ४१८३ ) इससे आरम्भ होनेवाले श्लोक में शरीर का लक्षण किया गया है, पुनः ‘शब्देस्तन्वंशरूप' (१८४) इस श्लोक में यह सिद्ध किया गया है कि विश्व ईश्वर से पृथक् सिद्ध नहीं हो सकता । अन्त में 'निष्कर्षाकत' ( ४८५) के द्वारा सभी शब्दों को परमात्मा का बोधक बतलाया गया है । ये सभी चीजें वहीं से जाननी चाहिए। रामानुज ने भी नाम और रूप का वर्णन करनेवाली कुतियों का विश्लेषण करते समय अपने वेदार्थ-संग्रह नामक ग्रन्थ में भी यही बात पुष्ट की है। विशेष-तत्त्वमुक्ताकलाप के उपर्युक्त संकेतों के पूरे श्लोक यों हैंसंस्थानक्याद्यभावे बहुषु निरुपधिहशब्दस्य रूढि
लॊकाम्नायप्रयोगानुगतमिह ततो लक्ष्म निष्कर्षणीयम् । अव्याप्तत्वादिदुःस्थं परमतपठितं लक्षणं तत्र तस्मात्
यद्धीतुल्याश्रयं तद्वपुरिदमपृथक् सिद्धिमद् द्रव्यमस्य ।। [ संसार के सभी जोवधारियों में ] शरीर की रचना की एकता नहीं देखी जाती, बहुत से पदार्थों में देह शब्द का प्रयोग ( रूढ़ि = Convention ) उपाधिहीन (.Unconditional ) ही है, यह लोक और वेद के प्रयोगों से सिद्ध है। इसलिए उसके अनुरूप ही एक लक्षण ( शरीर का ) निकालना चाहिए । दूसरे मतों के अनुसार दिये गये लक्षण अव्याप्ति आदि दोषों से दूषित हैं [ जैसे नैयायिक लोग 'चेष्टाश्रयत्वं शरीरत्वम्' कहते हैं, ईश्वर के शरीर के रूप में अभिमत काल आदि में चेष्टा नहीं है, अतः पूरे शरीर के अर्थ को यह लक्षण व्याप्त नहीं करता । ] इसलिए शरीर का लक्षण होगा-बुद्धि का आश्रय ही जिसका आश्रय है, जो द्रव्य जिससे पृथक् होकर नहीं रह सकता, वही उसका शरीर है। [ शरीर का आधार वही है जो बुद्धि का है, शरीर बुद्धि से पृथक् नहीं हो सकता, जो जिससे पृथक् नहीं हो वही उसका शरीर है । ]
शब्देस्तन्वंशरूपप्रभृतिभिरखिल: स्थाप्यते विश्वमूर्ते
रित्थंभावः प्रपञ्चस्तदनवगमतस्तत्पृथसिद्धमोहः । श्रोत्राद्यराश्रयेभ्यः स्फुरति खलु पृथक् शब्दगन्धादिधर्मो
जीवात्मन्यप्यदृश्ये वपुरपि हि दृशा गृह्यतेऽनन्यनिष्ठम् ॥