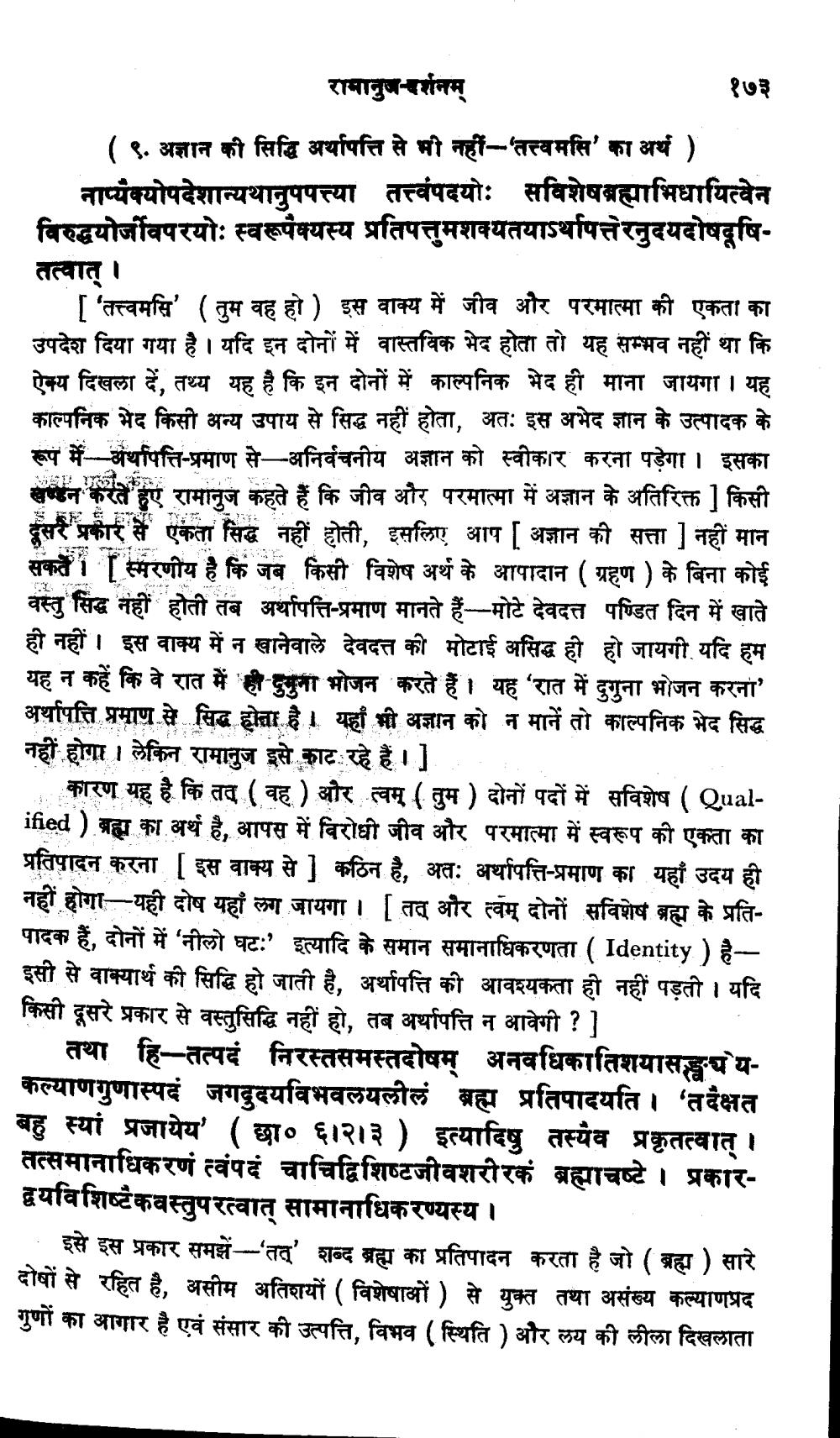________________
रामानुज-पर्शनम्
१७३ ( ९. अज्ञान की सिद्धि अर्थापत्ति से भी नहीं-'तत्त्वमसि' का अर्थ )
नाप्यक्योपदेशान्यथानुपपत्त्या तत्त्वंपदयोः सविशेषब्रह्माभिधायित्वेन विरुद्धयोर्जीवपरयोः स्वरूपैक्यस्य प्रतिपत्तुमशक्यतयाऽर्थापत्तेरनुदयदोषदूषि. तत्वात् ।
['तत्त्वमसि' (तुम वह हो ) इस वाक्य में जीव और परमात्मा की एकता का उपदेश दिया गया है। यदि इन दोनों में वास्तविक भेद होता तो यह सम्भव नहीं था कि ऐक्य दिखला दें, तथ्य यह है कि इन दोनों में काल्पनिक भेद ही माना जायगा । यह काल्पनिक भेद किसी अन्य उपाय से सिद्ध नहीं होता, अत: इस अभेद ज्ञान के उत्पादक के रूप में अपत्ति-प्रमाण से—अनिर्वचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका खण्डन करते हुए रामानुज कहते हैं कि जीव और परमात्मा में अज्ञान के अतिरिक्त ] किसी दूसरे प्रकार से एकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए आप [ अज्ञान की सत्ता ] नहीं मान सकते। [स्मरणीय है कि जब किसी विशेष अर्थ के आपादान ( ग्रहण ) के बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती तब अर्थापत्ति-प्रमाण मानते हैं-मोटे देवदत्त पण्डित दिन में खाते ही नहीं। इस वाक्य में न खानेवाले देवदत्त की मोटाई असिद्ध ही हो जायगी यदि हम
यह न कहें कि वे रात में ही दुमुना भोजन करते हैं। यह 'रात में दुगुना भोजन करना' __ अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है। यहाँ भी अज्ञान को न मानें तो काल्पनिक भेद सिद्ध नहीं होगा। लेकिन रामानुज इसे काट रहे हैं। ]
कारण यह है कि तत् ( वह ) और त्वम् ( तुम ) दोनों पदों में सविशेष ( Qualified ) ब्रह्म का अर्थ है, आपस में विरोधी जीव और परमात्मा में स्वरूप की एकता का प्रतिपादन करना [ इस वाक्य से ] कठिन है, अतः अर्थापत्ति-प्रमाण का यहाँ उदय ही नहीं होगा—यही दोष यहाँ लग जायगा। [ तत् और त्वम् दोनों सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, दोनों में 'नीलो घटः' इत्यादि के समान समानाधिकरणता ( Identity ) हैइसी से वाक्यार्थ की सिद्धि हो जाती है, अर्थापत्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि किसी दूसरे प्रकार से वस्तुसिद्धि नहीं हो, तब अर्थापत्ति न आवेगी ?]
तथा हि-तत्पदं निरस्तसमस्तदोषम् अनवधिकातिशयासङ्ख्यायकल्याणगुणास्पदं जगदुदयविभवलयलीलं ब्रह्म प्रतिपादयति । तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय' (छा० ६।२।३ ) इत्यादिषु तस्यैव प्रकृतत्वात् । तत्समानाधिकरणं त्वंपदं चाचिद्विशिष्टजीवशरीरकं ब्रह्माचष्टे । प्रकारद्वयविशिष्टैकवस्तुपरत्वात् सामानाधिकरण्यस्य। ___इसे इस प्रकार समझें-'तत्' शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करता है जो ( ब्रह्म ) सारे दोषों से रहित है, असीम अतिशयों ( विशेषाओं) से युक्त तथा असंख्य कल्याणप्रद गुणों का आगार है एवं संसार की उत्पत्ति, विभव ( स्थिति ) और लय की लीला दिखलाता
72